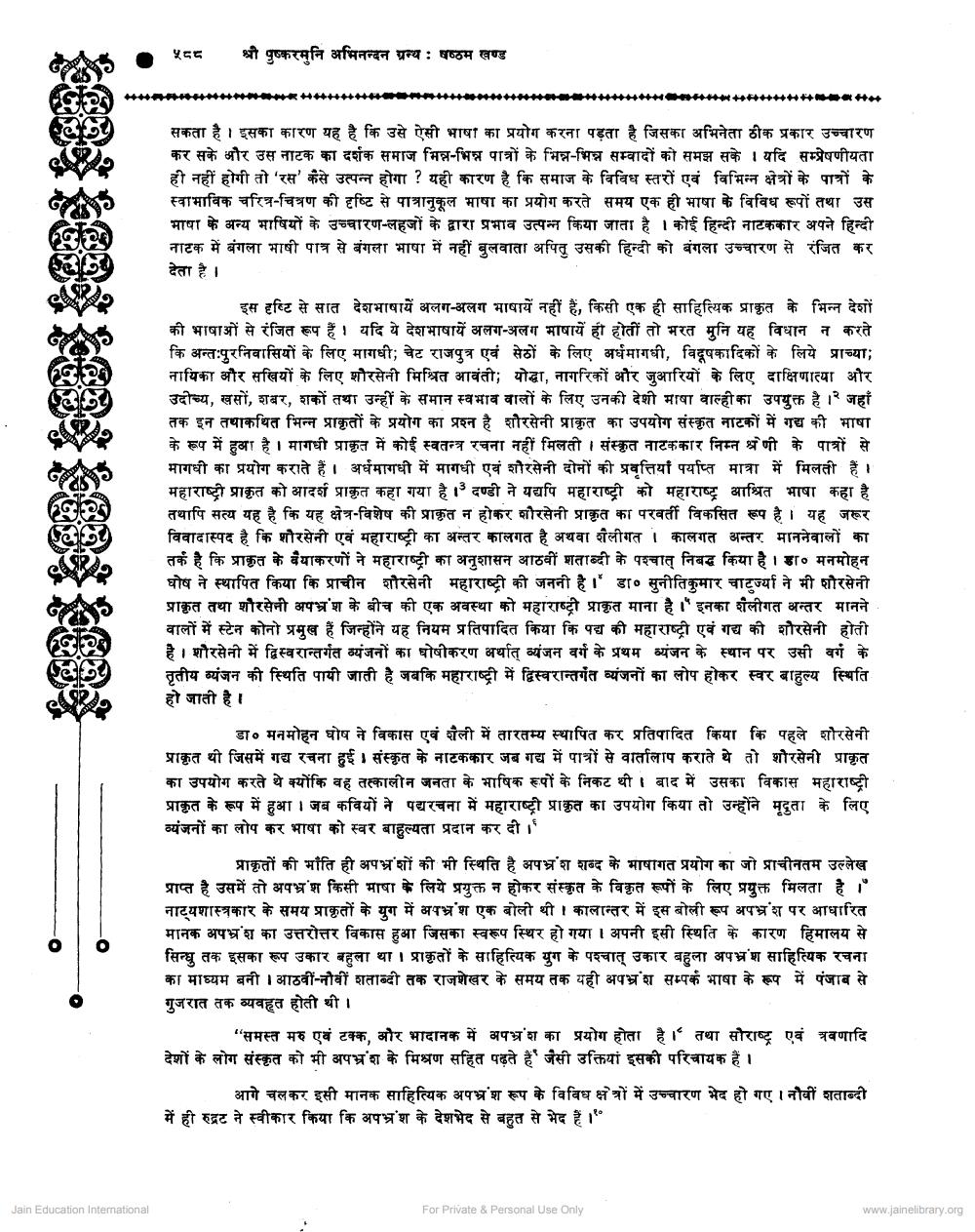________________
Jain Education International
५८८ श्री पुष्करमुनि अभिनन्दन ग्रन्थ : षष्ठम खण्ड
++++++
सकता है । इसका कारण यह है कि उसे ऐसी भाषा का प्रयोग करना पड़ता है जिसका अभिनेता ठीक प्रकार उच्चारण कर सके और उस नाटक का दर्शक समाज भिन्न-भिन्न पात्रों के भिन्न-भिन्न सम्वादों को समझ सके । यदि सम्प्रेषणीयता ही नहीं होगी तो 'रस' कैसे उत्पन्न होगा ? यही कारण है कि समाज के विविध स्तरों एवं विभिन्न क्षेत्रों के पात्रों के स्वाभाविक चरित्र-चित्रण की दृष्टि से पात्रानुकूल भाषा का प्रयोग करते समय एक ही भाषा के विविध रूपों तथा उस भाषा के अन्य भाषियों के उच्चारण-लहजों के द्वारा प्रभाव उत्पन्न किया जाता है । कोई हिन्दी नाटककार अपने हिन्दी नाटक में बंगला भाषी पात्र से बंगला भाषा में नहीं बुलवाता अपितु उसकी हिन्दी को बंगला उच्चारण से रंजित कर देता है ।
इस दृष्टि से सात देशभाषायें अलग-अलग भाषायें नहीं हैं, किसी एक ही साहित्यिक प्राकृत के भिन्न देशों की भाषाओं से रंजित रूप हैं। यदि ये देशभाषायें अलग-अलग भाषायें ही होतीं तो भरत मुनि यह विधान न करते कि अन्तःपुरनिवासियों के लिए मागधी; चेट राजपुत्र एवं सेठों के लिए अर्धमागधी, विदूषकादिकों के लिये प्राच्या; नायिका और सखियों के लिए शौरसेनी मिश्रित आवंती; योद्धा, नागरिकों और जुआरियों के लिए दाक्षिणात्या और उदीच्य, खसों, शबर, शकों तथा उन्हीं के समान स्वभाव वालों के लिए उनकी देशी भाषा वाल्हीका उपयुक्त है । जहाँ तक इन तथाकथित भिन्न प्राकृतों के प्रयोग का प्रश्न है शौरसेनी प्राकृत का उपयोग संस्कृत नाटकों में गद्य की भाषा के रूप में हुआ है । मागधी प्राकृत में कोई स्वतन्त्र रचना नहीं मिलती । संस्कृत नाटककार निम्न श्र ेणी के पात्रों से मागधी का प्रयोग कराते हैं । अर्धमागधी में मागधी एवं शौरसेनी दोनों की प्रवृत्तियां पर्याप्त मात्रा में मिलती हैं । महाराष्ट्री प्राकृत को आदर्श प्राकृत कहा गया है । दण्डी ने यद्यपि महाराष्ट्री को महाराष्ट्र आश्रित भाषा कहा है तथापि सत्य यह है कि यह क्षेत्र विशेष की प्राकृत न होकर शौरसेनी प्राकृत का परवर्ती विकसित रूप है। यह जरूर विवादास्पद है कि शौरसेनी एवं महाराष्ट्री का अन्तर कालगत है अथवा शैलीगत । कालगत अन्तर माननेवालों का तर्क है कि प्राकृत के वैयाकरणों ने महाराष्ट्री का अनुशासन आठवीं शताब्दी के पश्चात् निबद्ध किया है। डा० मनमोहन घोष ने स्थापित किया कि प्राचीन शौरसेनी महाराष्ट्री की जननी है। डा० सुनीतिकुमार चाटुयों ने भी शौरसेनी प्राकृत तथा शौरसेनी अपभ्रंश के बीच की एक अवस्था को महाराष्ट्री प्राकृत माना है ।" इनका शैलीगत अन्तर मानने वालों में स्टेन कोनो प्रमुख हैं जिन्होंने यह नियम प्रतिपादित किया कि पद्य की महाराष्ट्री एवं गद्य की शौरसेनी होती है । शौरसेनी में द्विस्वरान्तर्गत व्यंजनों का घोषीकरण अर्थात् व्यंजन वर्ग के प्रथम व्यंजन के स्थान पर उसी वर्ग के तृतीय व्यंजन की स्थिति पायी जाती है जबकि महाराष्ट्री में द्विस्वरान्तगंत व्यंजनों का लोप होकर स्वर बाहुल्य स्थिति हो जाती है।
डा० मनमोहन घोष ने विकास एवं शैली में तारतम्य स्थापित कर प्रतिपादित किया कि पहले शौरसेनी प्राकृत थी जिसमें गद्य रचना हुई। संस्कृत के नाटककार जब गद्य में पात्रों से वार्तालाप कराते थे तो शौरसेनी प्राकृत का उपयोग करते थे क्योंकि वह तत्कालीन जनता के भाषिक रूपों के निकट थी। बाद में उसका विकास महाराष्ट्री प्राकृत के रूप में हुआ । जब कवियों ने पद्यरचना में महाराष्ट्री प्राकृत का उपयोग किया तो उन्होंने मृदुता के लिए व्यंजनों का लोप कर भाषा को स्वर बाहुल्यता प्रदान कर दी।"
प्राकृतों की भाँति ही अपभ्रंशों की भी स्थिति है अपभ्रंश शब्द के भाषागत प्रयोग का जो प्राचीनतम उल्लेख प्राप्त है उसमें तो अपभ्रंश किसी भाषा के लिये प्रयुक्त न होकर संस्कृत के विकृत रूपों के लिए प्रयुक्त मिलता है ।" नाट्यशास्त्रकार के समय प्राकृतों के युग में अपभ्रंश एक बोली थी । कालान्तर में इस बोली रूप अपभ्रंश पर आधारित मानक अपभ्रंश का उत्तरोत्तर विकास हुआ जिसका स्वरूप स्थिर हो गया । अपनी इसी स्थिति के कारण हिमालय से सिन्धु तक इसका रूप उकार बहुला था । प्राकृतों के साहित्यिक युग के पश्चात् उकार बहुला अपभ्रंश साहित्यिक रचना का माध्यम बनी । आठवीं-नौवीं शताब्दी तक राजशेखर के समय तक यही अपभ्रंश सम्पर्क भाषा के रूप में पंजाब से गुजरात तक व्यवहृत होती थी।
" समस्त मरु एवं टक्क, और भादानक में अपभ्रंश का प्रयोग होता है ।" तथा सौराष्ट्र एवं त्रवणादि देशों के लोग संस्कृत को भी अपभ्रंश के मिश्रण सहित पढ़ते हैं' जैसी उक्तियां इसकी परिचायक हैं ।
आगे चलकर इसी मानक साहित्यिक अपभ्रंश रूप के विविध क्षेत्रों में उच्चारण भेद हो गए । नौवीं शताब्दी में ही रुद्रट ने स्वीकार किया कि अपभ्रंश के देशभेद से बहुत से भेद हैं ।"
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org