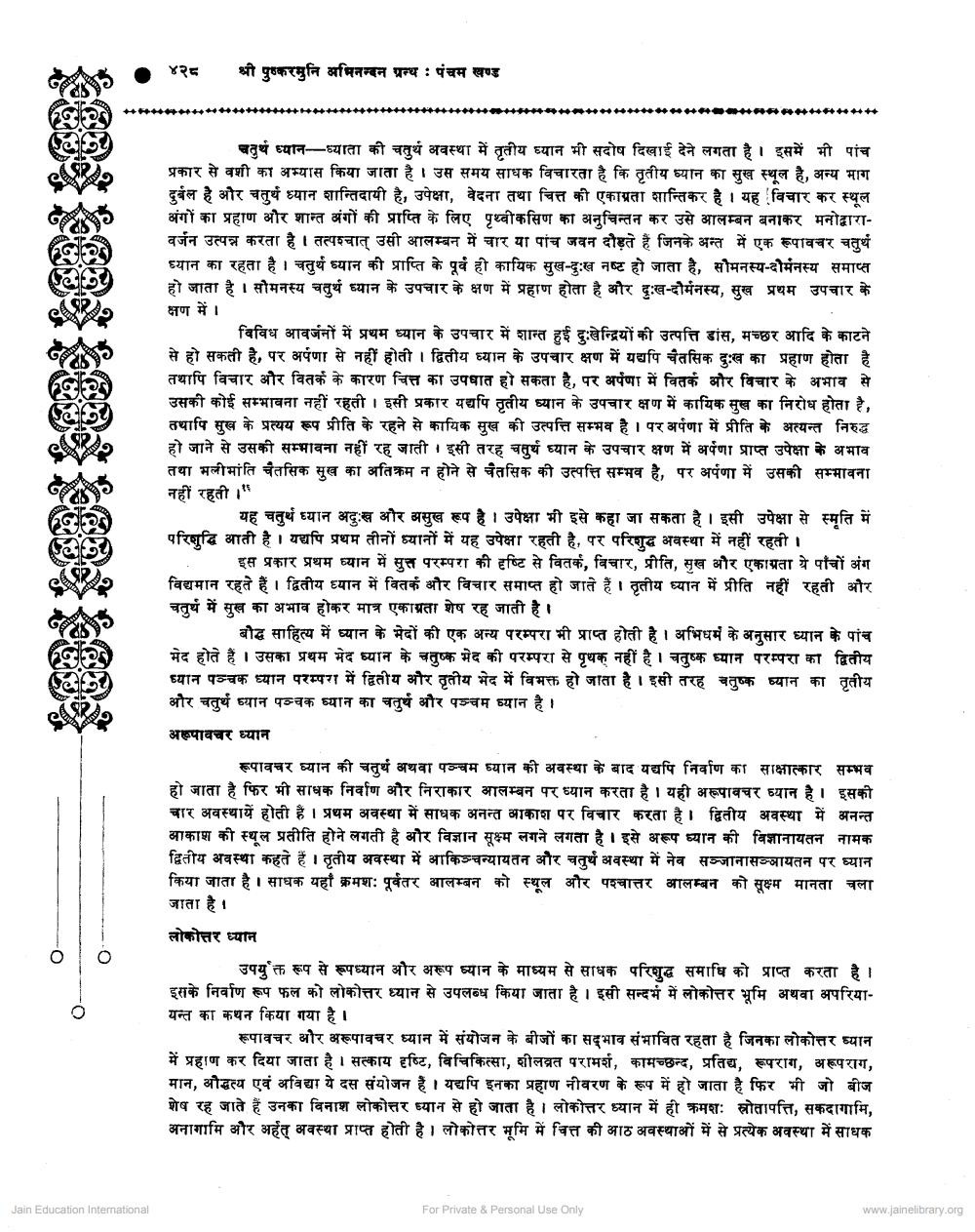________________
Jain Education International
४२८
श्री पुष्करमुनि अभिनन्दन ग्रन्थ : पंचम खण्ड
*****
चतुर्थ ध्यान - ध्याता की चतुर्थ अवस्था में तृतीय ध्यान भी सदोष दिखाई देने लगता है । इसमें भी पांच प्रकार से वशी का अभ्यास किया जाता है । उस समय साधक विचारता है कि तृतीय ध्यान का सुख स्थूल है, अन्य भाग दुर्बल है और चतुर्थ ध्यान शान्तिदायी है, उपेक्षा, वेदना तथा चित्त की एकाग्रता शान्तिकर है। यह विचार कर स्थूल अंगों का प्रहाण और शान्त अंगों की प्राप्ति के लिए पृथ्वीकसिण का अनुचिन्तन कर उसे आलम्बन बनाकर मनोद्वारावर्जन उत्पन्न करता है । तत्पश्चात् उसी आलम्बन में चार या पांच जवन दौड़ते हैं जिनके अन्त में एक रूपवचर चतुर्थ ध्यान का रहता है । चतुर्थ ध्यान की प्राप्ति के पूर्व ही कायिक सुख-दु:ख नष्ट हो जाता है, सौमनस्य- दौर्मनस्य समाप्त हो जाता है । सोमनस्य चतुर्थ ध्यान के उपचार के क्षण में प्रहाण होता है और दुःख दौर्मनस्य, सुख प्रथम उपचार के क्षण में ।
विविध आवजनों में प्रथम ध्यान के उपचार में शान्त हुई दुःखेन्द्रियों की उत्पत्ति डांस, मच्छर आदि के काटने से हो सकती है, पर अर्पणा से नहीं होती । द्वितीय ध्यान के उपचार क्षण में यद्यपि चैतसिक दुःख का प्रहाण होता है तथापि विचार और वितर्क के कारण चित्त का उपघात हो सकता है, पर अर्पणा में वितर्क और विचार के अभाव से उसकी कोई सम्भावना नहीं रहती। इसी प्रकार यद्यपि तृतीय ध्यान के उपचार क्षण में कायिक सुख का निरोध होता है, तथापि सुख के प्रत्यय रूप प्रीति के रहने से कायिक सुख की उत्पत्ति सम्भव है । पर अर्पणा में प्रीति के अत्यन्त निरुद्ध हो जाने से उसकी सम्भावना नहीं रह जाती। इसी तरह चतुर्थ ध्यान के उपचार क्षण में अर्पणा प्राप्त उपेक्षा के अभाव तथा भलीभांति चैतसिक सुख का अतिक्रम न होने से चेतसिक की उत्पत्ति सम्भव है, पर अर्पणा में उसकी सम्भावना नहीं रहती।
यह चतुर्थ ध्यान अदुःख और असुख रूप है । उपेक्षा भी इसे कहा जा सकता है । इसी उपेक्षा से स्मृति में परिशुद्धि आती है । यद्यपि प्रथम तीनों ध्यानों में यह उपेक्षा रहती है, पर परिशुद्ध अवस्था में नहीं रहती ।
इस प्रकार प्रथम ध्यान में सुख परम्परा की दृष्टि से वितर्क, विचार, प्रीति, सुख और एकाग्रता ये पाँचों अंग विद्यमान रहते हैं । द्वितीय ध्यान में वितर्क और विचार समाप्त हो जाते हैं। तृतीय ध्यान में प्रीति नहीं रहती और चतुर्थ में सुख का अभाव होकर मात्र एकाग्रता शेष रह जाती है ।
बौद्ध साहित्य में ध्यान के भेदों की एक अन्य परम्परा भी प्राप्त होती है। अभिधर्म के अनुसार ध्यान के पांच भेद होते हैं । उसका प्रथम भेद ध्यान के चतुष्क भेद की परम्परा से पृथक् नहीं है । चतुष्क ध्यान परम्परा का द्वितीय ध्यान पञ्चक ध्यान परम्परा में द्वितीय और तृतीय भेद में विभक्त हो जाता है। इसी तरह चतुष्क ध्यान का तृतीय और चतुर्थ ध्यान पञ्चक ध्यान का चतुर्थ और पञ्चम ध्यान है ।
अरूपावचर ध्यान
रूपावचर ध्यान की चतुर्थ अथवा पञ्चम ध्यान की अवस्था के बाद यद्यपि निर्वाण का साक्षात्कार सम्भव हो जाता है फिर भी साधक निर्वाण और निराकार आलम्बन पर ध्यान करता है । यही अरूपावचर ध्यान है। इसकी चार अवस्थायें होती हैं । प्रथम अवस्था में साधक अनन्त आकाश पर विचार करता है। द्वितीय अवस्था में अनन्त आकाश की स्थूल प्रतीति होने लगती है और विज्ञान सूक्ष्म लगने लगता है । इसे अरूप ध्यान की विज्ञानायतन नामक द्वितीय अवस्था कहते हैं। तृतीय अवस्था में आकिञ्चन्यायतन और चतुर्थ अवस्था में नेव सञ्जानासञ्जायतन पर ध्यान किया जाता है । साधक यहाँ क्रमशः पूर्वतर आलम्बन को स्थूल और पश्चात्तर आलम्बन को सूक्ष्म मानता चला जाता है ।
लोकोत्तर ध्यान
उपर्युक्त रूप से रूपध्यान और अरूप ध्यान के माध्यम से साधक परिशुद्ध समाधि को प्राप्त करता है । इसके निर्वाण रूप फल को लोकोत्तर ध्यान से उपलब्ध किया जाता है। इसी सन्दर्भ में लोकोत्तर भूमि अथवा अपरियायन्त का कथन किया गया है ।
रूपावचर और अरूपावचर ध्यान में संयोजन के बीजों का सद्भाव संभावित रहता है जिनका लोकोत्तर ध्यान में प्रहाण कर दिया जाता है। सत्काय दृष्टि, विचिकित्सा, शीलव्रत परामर्श, कामच्छन्द, प्रतिद्य, रूपराग, अरूपराग, मान, औद्धत्य एवं अविद्या ये दस संयोजन हैं । यद्यपि इनका प्रहाण नीवरण के रूप में हो जाता है फिर भी जो बीज शेष रह जाते हैं उनका विनाश लोकोत्तर ध्यान से हो जाता है। लोकोत्तर ध्यान में ही क्रमशः स्रोतापत्ति, सकदागामि, अनागामि और अर्हत् अवस्था प्राप्त होती है। लोकोत्तर भूमि में चित्त की आठ अवस्थाओं में से प्रत्येक अवस्था में साधक
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org