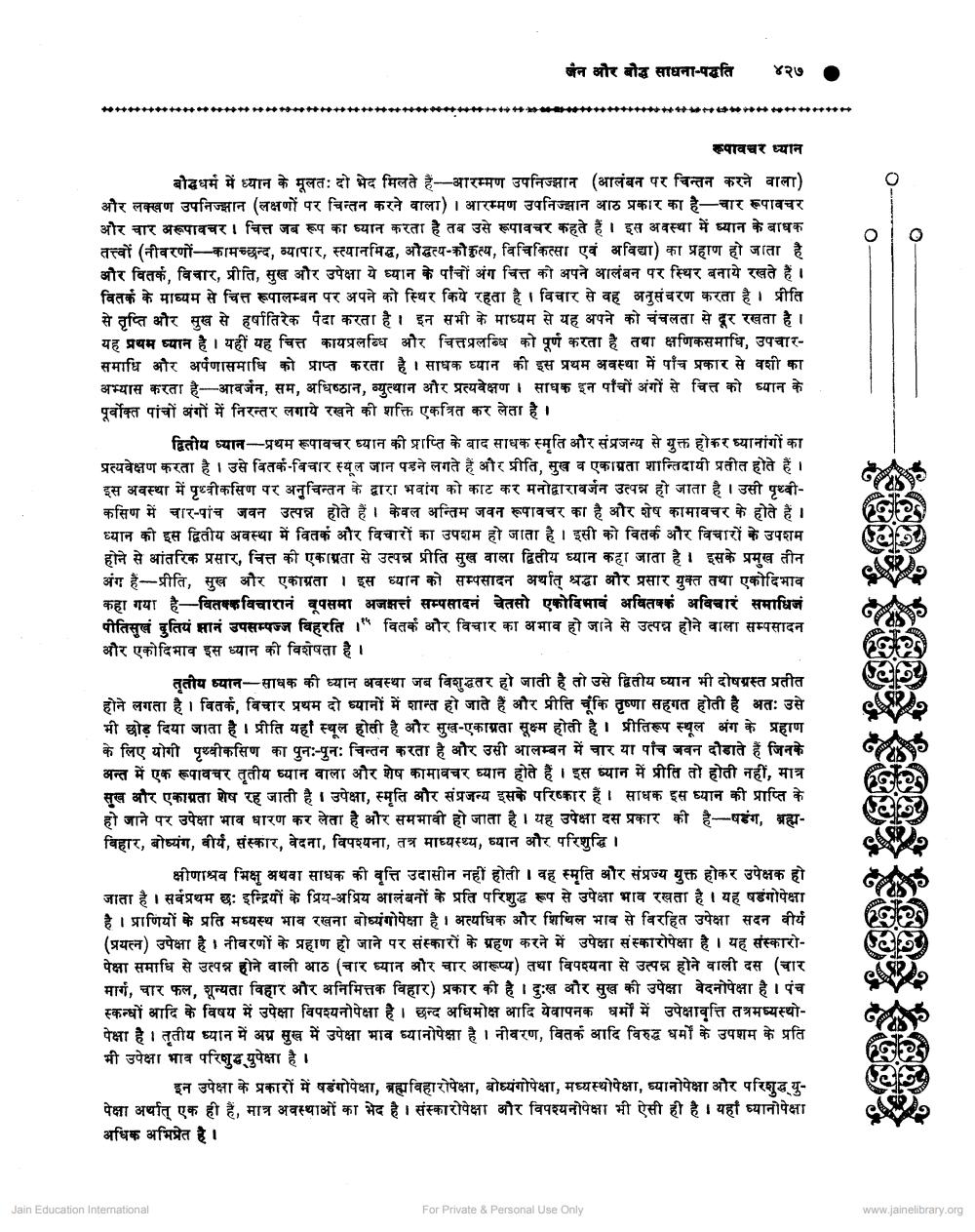________________
जैन और बौद्ध साधना-पद्धति
४२७
+++++
++++
++++
++
+++
++
+
+++
+
+
+++
++++
++
+
+++
++
+
+
+m
a ro +++++++++++
+
+
+++
+
+
+
+++
+
रूपावञ्चर ध्यान बौद्धधर्म में ध्यान के मूलत: दो भेद मिलते हैं-आरम्मण उपनिज्झान (आलंबन पर चिन्तन करने वाला) और लक्खण उपनिज्झान (लक्षणों पर चिन्तन करने वाला) । आरम्मण उपनिज्झान आठ प्रकार का है-चार रूपावचर और चार अरूपावचर । चित्त जब रूप का ध्यान करता है तब उसे रूपावचर कहते हैं । इस अवस्था में ध्यान के बाधक तत्त्वों (नीवरणों-कामच्छन्द, व्यापार, स्त्यानमिद्ध, औद्धत्य-कोकृत्य, विचिकित्सा एवं अविद्या) का प्रहाण हो जाता है और वितर्क, विचार, प्रीति, सुख और उपेक्षा ये ध्यान के पांचों अंग चित्त को अपने आलंबन पर स्थिर बनाये रखते हैं । वितर्क के माध्यम से चित्त रूपालम्बन पर अपने को स्थिर किये रहता है । विचार से वह अनुसंचरण करता है। प्रीति से तृप्ति और सुख से हर्षातिरेक पैदा करता है। इन सभी के माध्यम से यह अपने को चंचलता से दूर रखता है। यह प्रथम ध्यान है। यहीं यह चित्त कायप्रलब्धि और चित्तप्रलब्धि को पूर्ण करता है तथा क्षणिकसमाधि, उपचारसमाधि और अर्पणासमाधि को प्राप्त करता है। साधक ध्यान की इस प्रथम अवस्था में पाँच प्रकार से वशी का अभ्यास करता है-आवर्जन, सम, अधिष्ठान, व्युत्थान और प्रत्यवेक्षण । साधक इन पांचों अंगों से चित्त को ध्यान के पूर्वोक्त पांचों अंगों में निरन्तर लगाये रखने की शक्ति एकत्रित कर लेता है।
द्वितीय ध्यान-प्रथम रूपावचर ध्यान की प्राप्ति के बाद साधक स्मृति और संप्रजन्य से युक्त होकर ध्यानांगों का प्रत्यवेक्षण करता है। उसे वितर्क-विचार स्यूल जान पड़ने लगते हैं और प्रीति, सुख व एकाग्रता शान्तिदायी प्रतीत होते हैं। इस अवस्था में पृथ्वीकसिण पर अनुचिन्तन के द्वारा भवांग को काट कर मनोद्वारावर्जन उत्पन्न हो जाता है । उसी पृथ्वीकसिण में चार-पांच जवन उत्पन्न होते हैं। केवल अन्तिम जवन रूपावचर का है और शेष कामावचर के होते हैं। ध्यान को इस द्वितीय अवस्था में वितर्क और विचारों का उपशम हो जाता है। इसी को वितर्क और विचारों के उपशम होने से आंतरिक प्रसार, चित्त की एकाग्रता से उत्पन्न प्रीति सुख वाला द्वितीय ध्यान कहा जाता है। इसके प्रमुख तीन अंग हैं-प्रीति, सुख और एकाग्रता । इस ध्यान को सम्पसादन अर्थात् श्रद्धा और प्रसार युक्त तथा एकोदिभाव कहा गया है-वितक्कविचारानं खूपसमा अजझत्तं सम्पसादनं चेतसो एकोविभावं अवितकं अविचारं समाधिज पीतिसुखं दुतियं सानं उपसम्पज्ज विहरति ।५ वितर्क और विचार का अभाव हो जाने से उत्पन्न होने वाला सम्पसादन और एकोदिभाव इस ध्यान की विशेषता है ।।
तृतीय ध्यान-साधक की ध्यान अवस्था जब विशुद्धतर हो जाती है तो उसे द्वितीय ध्यान भी दोषग्रस्त प्रतीत होने लगता है। वितर्क, विचार प्रथम दो ध्यान में शान्त हो जाते हैं और प्रीति चूंकि तृष्णा सहगत होती है अतः उसे भी छोड़ दिया जाता है । प्रीति यहाँ स्थूल होती है और सुख-एकाग्रता सूक्ष्म होती है। प्रीतिरूप स्थूल अंग के प्रहाण के लिए योगी पृथ्वीकसिण का पुनः-पुनः चिन्तन करता है और उसी आलम्बन में चार या पांच जवन दौडाते हैं जिनके अन्त में एक रूपावचर तृतीय ध्यान वाला और शेष कामावचर ध्यान होते हैं । इस ध्यान में प्रीति तो होती नहीं, मात्र सुख और एकाग्रता शेष रह जाती है । उपेक्षा, स्मृति और संप्रजन्य इसके परिष्कार हैं। साधक इस ध्यान की प्राप्ति के हो जाने पर उपेक्षा भाव धारण कर लेता है और समभावी हो जाता है । यह उपेक्षा दस प्रकार की है-षडंग, ब्रह्मबिहार, बोध्यंग, वीर्य, संस्कार, वेदना, विपश्यना, तत्र माध्यस्थ्य, ध्यान और परिशुद्धि ।
क्षीणाश्रव भिक्षु अथवा साधक की वृत्ति उदासीन नहीं होती। वह स्मृति और संप्रज्य युक्त होकर उपेक्षक हो जाता है । सर्वप्रथम छ: इन्द्रियों के प्रिय-अप्रिय आलंबनों के प्रति परिशुद्ध रूप से उपेक्षा भाव रखता है । यह षडंगोपेक्षा है । प्राणियों के प्रति मध्यस्थ भाव रखना बोध्यंगोपेक्षा है। अत्यधिक और शिथिल भाव से विरहित उपेक्षा सदन वीर्य (प्रयत्न) उपेक्षा है। नीवरणों के प्रहाण हो जाने पर संस्कारों के ग्रहण करने में उपेक्षा संस्कारोपेक्षा है। यह संस्कारोपेक्षा समाधि से उत्पन्न होने वाली आठ (चार ध्यान और चार आरूप्य) तथा विपश्यना से उत्पन्न होने वाली दस (चार मार्ग, चार फल, शून्यता विहार और अनिमित्तक विहार) प्रकार की है। दु:ख और सुख की उपेक्षा वेदनोपेक्षा है। पंच स्कन्धों आदि के विषय में उपेक्षा विपश्यनोपेक्षा है। छन्द अधिमोक्ष आदि येवापनक धर्मों में उपेक्षावृत्ति तत्रमध्यस्थोपेक्षा है। तृतीय ध्यान में अग्र सुख में उपेक्षा भाव ध्यानोपेक्षा है। नीवरण, वितर्क आदि विरुद्ध धर्मों के उपशम के प्रति भी उपेक्षा भाव परिशुद्ध युपेक्षा है।
इन उपेक्षा के प्रकारों में षडंगोपेक्षा, ब्रह्मविहारोपेक्षा, बोध्यंगोपेक्षा, मध्यस्थोपेक्षा, ध्यानोपेक्षा और परिशुद्ध युपेक्षा अर्थात् एक ही हैं, मात्र अवस्थाओं का भेद है । संस्कारोपेक्षा और विपश्यनोपेक्षा भी ऐसी ही है । यहाँ ध्यानोपेक्षा अधिक अभिप्रेत है।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org