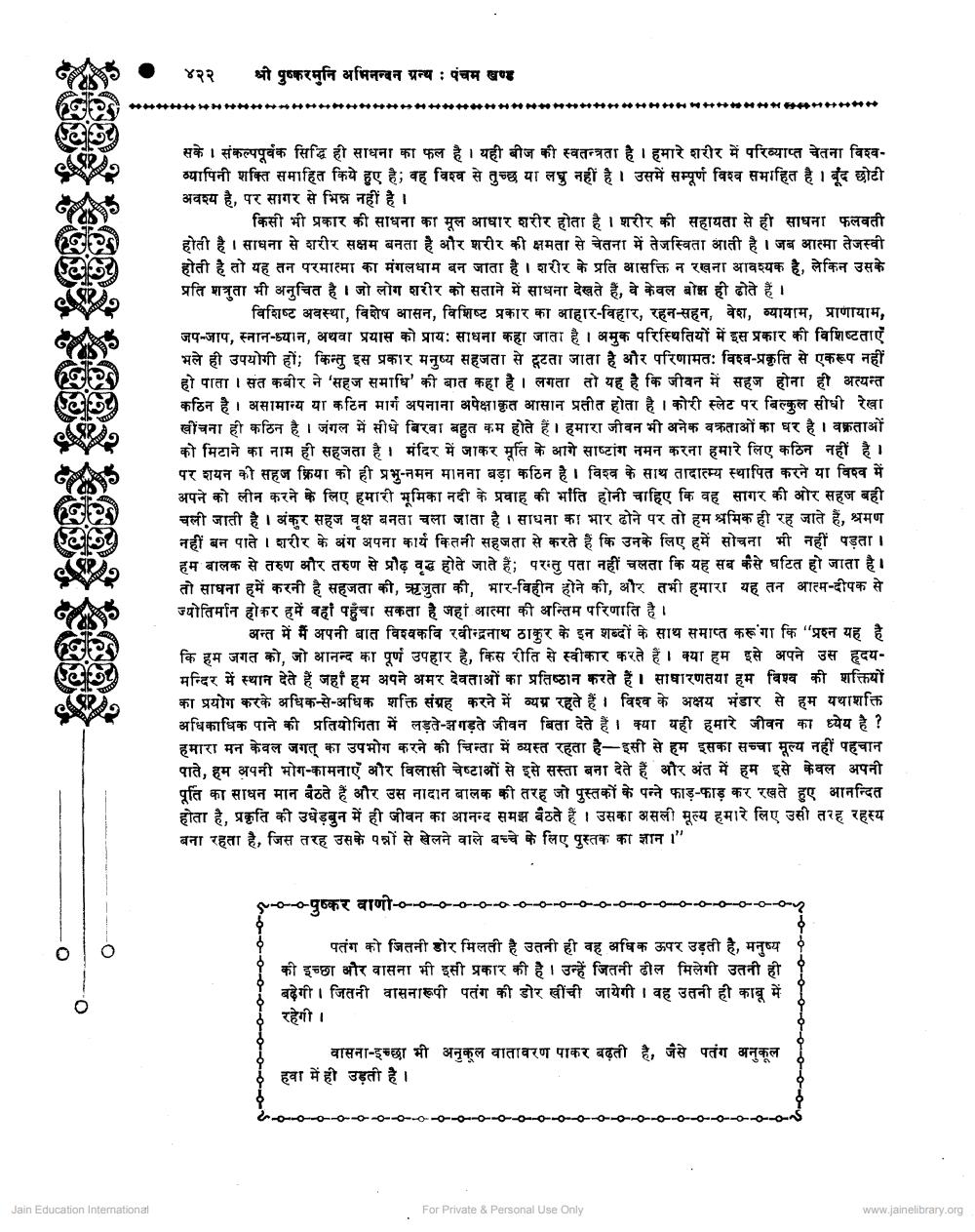________________
O
*
Jain Education International
४२२
श्री पुष्कर मुनि अभिनन्दन ग्रन्थ : पंचम खण्ड
सके । संकल्पपूर्वक सिद्धि ही साधना का फल है । यही बीज की स्वतन्त्रता है । हमारे शरीर में परिव्याप्त चेतना विश्वव्यापिनी शक्ति समाहित किये हुए है; वह विश्व से तुच्छ या लघु नहीं है । उसमें सम्पूर्ण विश्व समाहित है । बूंद छोटी अवश्य है, पर सागर से भिन्न नहीं है ।
किसी भी प्रकार की साधना का मूल आधार शरीर होता है । शरीर की सहायता से ही साधना फलवती होती है | साधना से शरीर सक्षम बनता है और शरीर की क्षमता से चेतना में तेजस्विता आती है । जब आत्मा तेजस्वी होती है तो यह तन परमात्मा का मंगलधाम बन जाता है । शरीर के प्रति आसक्ति न रखना आवश्यक है, लेकिन उसके प्रति शत्रुता भी अनुचित है । जो लोग शरीर को सताने में साधना देखते हैं, वे केवल बोझ ही ढोते हैं ।
विशिष्ट अवस्था, विशेष आसन, विशिष्ट प्रकार का आहार-विहार, रहन-सहन, वेश, व्यायाम, प्राणायाम, जप- जाप, स्नान-ध्यान, अथवा प्रयास को प्राय: साधना कहा जाता है । अमुक परिस्थितियों में इस प्रकार की विशिष्टताएँ भले ही उपयोगी हों; किन्तु इस प्रकार मनुष्य सहजता से टूटता जाता है और परिणामतः विश्व प्रकृति से एकरूप नहीं हो पाता । संत कबीर ने 'सहज समाधि' की बात कहा है। लगता तो यह है कि जीवन में सहज होना ही अत्यन्त कठिन है । असामान्य या कठिन मार्ग अपनाना अपेक्षाकृत आसान प्रतीत होता है। कोरी स्लेट पर बिल्कुल सीधी रेखा खींचना ही कठिन है । जंगल में सीधे बिरवा बहुत कम होते हैं। हमारा जीवन भी अनेक वक्रताओं का घर है । वक्रताओं को मिटाने का नाम ही सहजता है। मंदिर में जाकर मूर्ति के आगे साष्टांग नमन करना हमारे लिए कठिन नहीं है । पर शयन की सहज क्रिया को ही प्रभु-नमन मानना बड़ा कठिन है। विश्व के साथ तादात्म्य स्थापित करने या विश्व में अपने को लीन करने के लिए हमारी भूमिका नदी के प्रवाह की भांति होनी चाहिए कि वह सागर की ओर सहज बही चली जाती है । अंकुर सहज वृक्ष बनता चला जाता है। साधना का भार ढोने पर तो हम श्रमिक ही रह जाते हैं, श्रमण नहीं बन पाते । शरीर के अंग अपना कार्य कितनी सहजता से करते हैं कि उनके लिए हमें सोचना भी नहीं पड़ता । हम बालक से तरुण और तरुण से प्रौढ़ वृद्ध होते जाते हैं; परन्तु पता नहीं चलता कि यह सब कैसे घटित हो जाता है। तो साधना हमें करनी है सहजता की, ऋजुता की, भार-विहीन होने की, और तभी हमारा यह तन आत्म- दीपक से ज्योतिर्मान होकर हमें वहाँ पहुँचा सकता है जहां आत्मा की अन्तिम परिणाति है ।
अन्त में मैं अपनी बात विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर के इन शब्दों के साथ समाप्त करूंगा कि "प्रश्न यह है कि हम जगत को, जो आनन्द का पूर्ण उपहार है, किस रीति से स्वीकार करते हैं। क्या हम इसे अपने उस हृदयमन्दिर में स्थान देते हैं जहाँ हम अपने अमर देवताओं का प्रतिष्ठान करते हैं। साधारणतया हम विश्व की शक्तियों का प्रयोग करके अधिक-से-अधिक शक्ति संग्रह करने में व्यग्र रहते हैं । विश्व के अक्षय भंडार से हम यथाशक्ति अधिकाधिक पाने की प्रतियोगिता में लड़ते-झगड़ते जीवन बिता देते हैं। क्या यही हमारे जीवन का ध्येय है ? हमारा मन केवल जगत् का उपभोग करने की चिन्ता में व्यस्त रहता है— इसी से हम इसका सच्चा मूल्य नहीं पहचान पाते, हम अपनी भोग-कामनाएँ और विलासी चेष्टाओं से इसे सस्ता बना देते हैं और अंत में हम इसे केवल अपनी पूर्ति का साधन मान बैठते हैं और उस नादान बालक की तरह जो पुस्तकों के पन्ने फाड़-फाड़ कर रखते हुए आनन्दित होता है, प्रकृति की उधेड़बुन में ही जीवन का आनन्द समझ बैठते हैं । उसका असली मूल्य हमारे लिए उसी तरह रहस्य बना रहता है, जिस तरह उसके पन्नों से खेलने वाले बच्चे के लिए पुस्तक का ज्ञान ।"
5-०-०- पुष्कर वाणी-०-०
पतंग को जितनी डोर मिलती है उतनी ही वह अधिक ऊपर उड़ती है, मनुष्य की इच्छा और वासना भी इसी प्रकार की है। उन्हें जितनी ढील मिलेगी उतनी ही बढ़ेगी। जितनी वासनारूपी पतंग की डोर खींची जायेगी। वह उतनी ही काबू में रहेगी ।
वासना - इच्छा भी अनुकूल वातावरण पाकर बढ़ती है, जैसे पतंग अनुकूल हवा में ही उड़ती है ।
10--0
********
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org