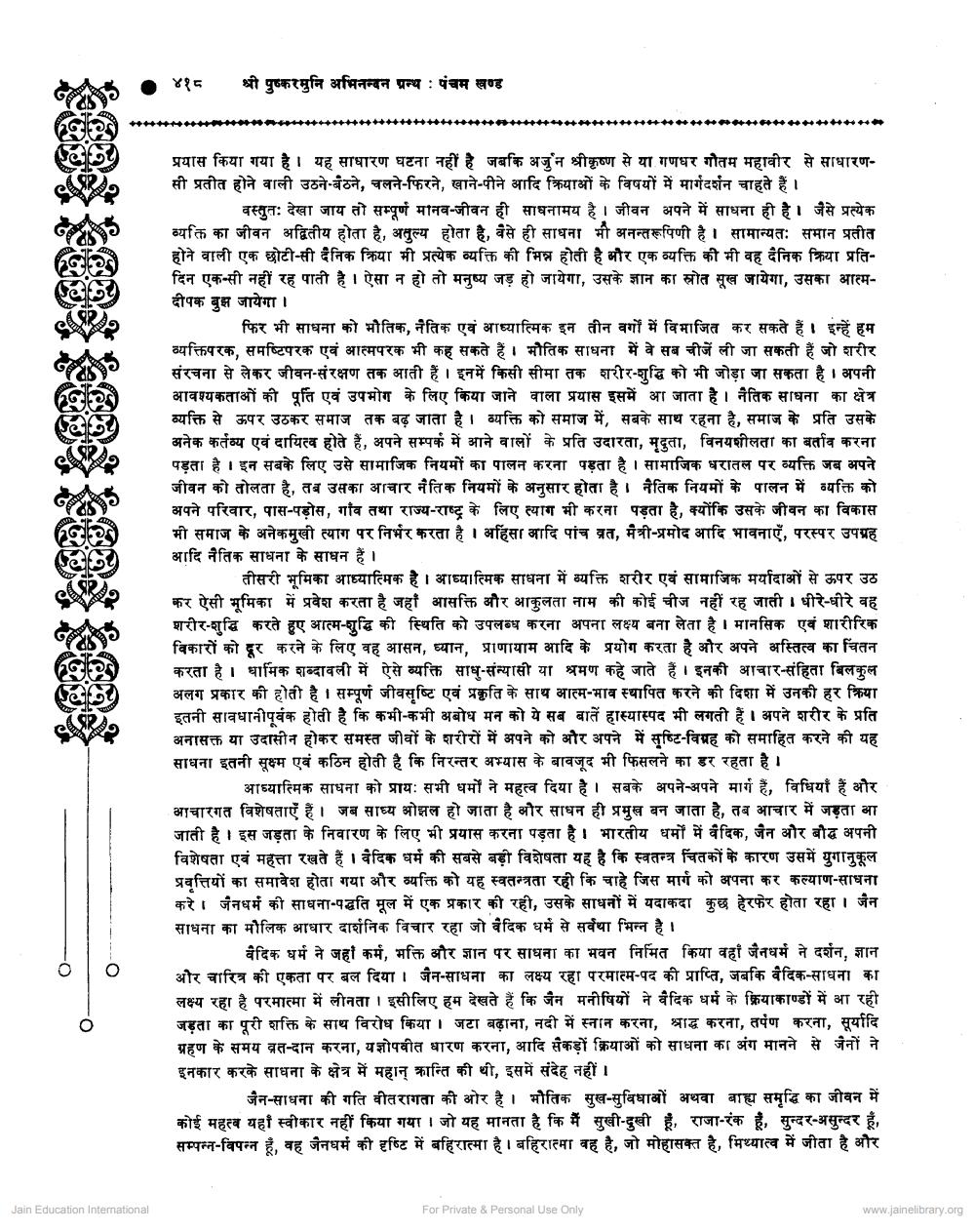________________
४१८
श्री पुष्करमुनि अभिनन्दन प्रन्थ : पंचम खण्ड
प्रयास किया गया है। यह साधारण घटना नहीं है जबकि अर्जुन श्रीकृष्ण से या गणधर गौतम महावीर से साधारणसी प्रतीत होने वाली उठने-बैठने, चलने-फिरने, खाने-पीने आदि क्रियाओं के विषयों में मार्गदर्शन चाहते हैं।
वस्तुतः देखा जाय तो सम्पूर्ण मानव-जीवन ही साधनामय है। जीवन अपने में साधना ही है। जैसे प्रत्येक व्यक्ति का जीवन अद्वितीय होता है, अतुल्य होता है, वैसे ही साधना भी अनन्तरूपिणी है। सामान्यतः समान प्रतीत होने वाली एक छोटी-सी दैनिक क्रिया भी प्रत्येक व्यक्ति की भिन्न होती है और एक व्यक्ति की भी वह दैनिक क्रिया प्रतिदिन एक-सी नहीं रह पाती है। ऐसा न हो तो मनुष्य जड़ हो जायेगा, उसके ज्ञान का स्रोत सूख जायेगा, उसका आत्मदीपक बुझ जायेगा।
फिर भी साधना को भौतिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक इन तीन वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। इन्हें हम व्यक्तिपरक, समष्टिपरक एवं आत्मपरक भी कह सकते हैं। भौतिक साधना में वे सब चीजें ली जा सकती हैं जो शरीर संरचना से लेकर जीवन-संरक्षण तक आती हैं। इनमें किसी सीमा तक शरीर-शुद्धि को भी जोड़ा जा सकता है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति एवं उपभोग के लिए किया जाने वाला प्रयास इसमें आ जाता है। नैतिक साधना का क्षेत्र व्यक्ति से ऊपर उठकर समाज तक बढ़ जाता है। व्यक्ति को समाज में, सबके साथ रहना है, समाज के प्रति उसके अनेक कर्तव्य एवं दायित्व होते हैं, अपने सम्पर्क में आने वालों के प्रति उदारता, मृदुता, विनयशीलता का बर्ताव करना पड़ता है । इन सबके लिए उसे सामाजिक नियमों का पालन करना पड़ता है । सामाजिक धरातल पर व्यक्ति जब अपने जीवन को तोलता है, तब उसका आचार नैतिक नियमों के अनुसार होता है। नैतिक नियमों के पालन में व्यक्ति को अपने परिवार, पास-पड़ोस, गाँव तथा राज्य-राष्ट्र के लिए त्याग भी करना पड़ता है, क्योंकि उसके जीवन का विकास भी समाज के अनेकमुखी त्याग पर निर्भर करता है । अहिंसा आदि पांच व्रत, मैत्री-प्रमोद आदि भावनाएँ, परस्पर उपग्रह आदि नैतिक साधना के साधन हैं।
तीसरी भूमिका आध्यात्मिक है । आध्यात्मिक साधना में व्यक्ति शरीर एवं सामाजिक मर्यादाओं से ऊपर उठ कर ऐसी भूमिका में प्रवेश करता है जहाँ आसक्ति और आकुलता नाम की कोई चीज नहीं रह जाती। धीरे-धीरे वह शरीर-शुद्धि करते हुए आत्म-शुद्धि की स्थिति को उपलब्ध करना अपना लक्ष्य बना लेता है । मानसिक एवं शारीरिक विकारों को दूर करने के लिए वह आसन, ध्यान, प्राणायाम आदि के प्रयोग करता है और अपने अस्तित्व का चिंतन करता है। धार्मिक शब्दावली में ऐसे व्यक्ति साधु-संन्यासी या श्रमण कहे जाते हैं । इनकी आचार-संहिता बिलकुल अलग प्रकार की होती है । सम्पूर्ण जीवसृष्टि एवं प्रकृति के साथ आत्म-भाव स्थापित करने की दिशा में उनकी हर क्रिया इतनी सावधानीपूर्वक होती है कि कभी-कभी अबोध मन को ये सब बातें हास्यास्पद भी लगती हैं। अपने शरीर के प्रति अनासक्त या उदासीन होकर समस्त जीवों के शरीरों में अपने को और अपने में सृष्टि-विग्रह को समाहित करने की यह साधना इतनी सूक्ष्म एवं कठिन होती है कि निरन्तर अभ्यास के बावजूद भी फिसलने का डर रहता है।
आध्यात्मिक साधना को प्रायः सभी धर्मों ने महत्व दिया है। सबके अपने-अपने मार्ग हैं, विधियाँ हैं और आचारगत विशेषताएँ हैं। जब साध्य ओझल हो जाता है और साधन ही प्रमुख बन जाता है, तब आचार में जड़ता आ जाती है। इस जड़ता के निवारण के लिए भी प्रयास करना पड़ता है। भारतीय धर्मों में वैदिक, जैन और बौद्ध अपनी विशेषता एवं महत्ता रखते हैं । वैदिक धर्म की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि स्वतन्त्र चिंतकों के कारण उसमें युगानुकूल प्रवृत्तियों का समावेश होता गया और व्यक्ति को यह स्वतन्त्रता रही कि चाहे जिस मार्ग को अपना कर कल्याण-साधना करे। जैनधर्म की साधना-पद्धति मूल में एक प्रकार की रही, उसके साधनों में यदाकदा कुछ हेरफेर होता रहा। जैन साधना का मौलिक आधार दार्शनिक विचार रहा जो वैदिक धर्म से सर्वथा भिन्न है।
वैदिक धर्म ने जहाँ कर्म, भक्ति और ज्ञान पर साधना का भवन निर्मित किया वहाँ जैनधर्म ने दर्शन, ज्ञान और चारित्र की एकता पर बल दिया। जैन-साधना का लक्ष्य रहा परमात्म-पद की प्राप्ति, जबकि वैदिक-साधना का लक्ष्य रहा है परमात्मा में लीनता । इसीलिए हम देखते हैं कि जैन मनीषियों ने वैदिक धर्म के क्रियाकाण्डों में आ रही जड़ता का पूरी शक्ति के साथ विरोध किया। जटा बढ़ाना, नदी में स्नान करना, श्राद्ध करना, तर्पण करना, सूर्यादि ग्रहण के समय व्रत-दान करना, यज्ञोपवीत धारण करना, आदि सैकड़ों क्रियाओं को साधना का अंग मानने से जैनों ने इनकार करके साधना के क्षेत्र में महान क्रान्ति की थी, इसमें संदेह नहीं।
जैन-साधना की गति वीतरागता की ओर है। भौतिक सुख-सुविधाओं अथवा बाह्य समृद्धि का जीवन में कोई महत्व यहाँ स्वीकार नहीं किया गया । जो यह मानता है कि मैं सुखी-दुखी हूँ, राजा-रंक हूँ, सुन्दर-असुन्दर हूँ, सम्पन्न-विपन्न हैं, वह जैनधर्म की दृष्टि में बहिरात्मा है । बहिरात्मा वह है, जो मोहासक्त है, मिथ्यात्व में जीता है और
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org