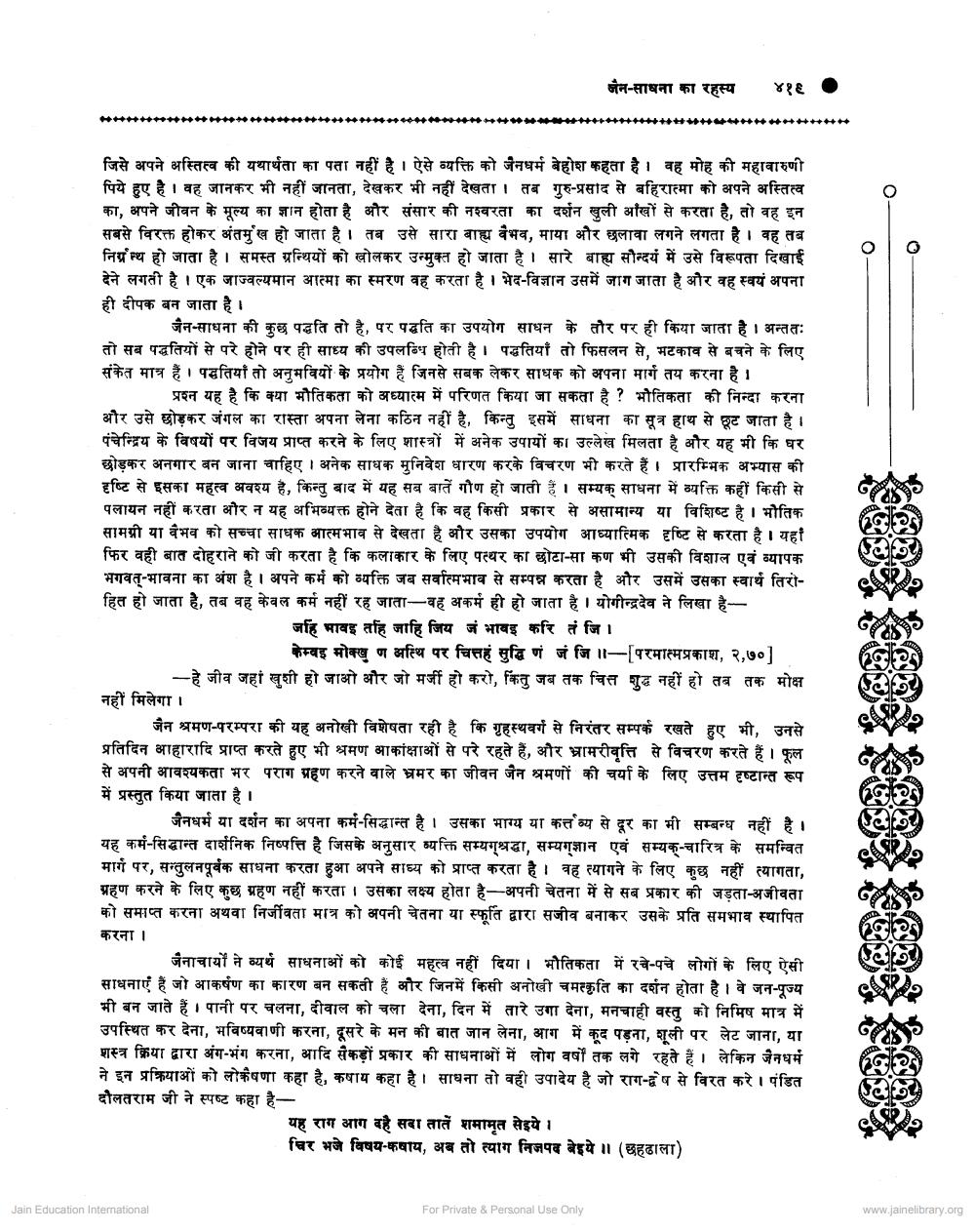________________
जैन-साधना का रहस्य
४१६
.
जिसे अपने अस्तित्व की यथार्थता का पता नहीं है । ऐसे व्यक्ति को जैनधर्म बेहोश कहता है। वह मोह की महावारुणी पिये हुए है । वह जानकर भी नहीं जानता, देखकर भी नहीं देखता। तब गुरु-प्रसाद से बहिरात्मा को अपने अस्तित्व का, अपने जीवन के मूल्य का ज्ञान होता है और संसार की नश्वरता का दर्शन खुली आँखों से करता है, तो वह इन सबसे विरक्त होकर अंतर्मुख हो जाता है। तब उसे सारा बाह्य वैभव, माया और छलावा लगने लगता है। वह तब निग्रंथ हो जाता है। समस्त ग्रन्थियों को खोलकर उन्मुक्त हो जाता है। सारे बाह्य सौन्दयं में उसे विरूपता दिखाई देने लगती है । एक जाज्वल्यमान आत्मा का स्मरण वह करता है । भेद-विज्ञान उसमें जाग जाता है और वह स्वयं अपना ही दीपक बन जाता है।
जैन-साधना की कुछ पद्धति तो है, पर पद्धति का उपयोग साधन के तौर पर ही किया जाता है । अन्ततः तो सब पद्धतियों से परे होने पर ही साध्य की उपलब्धि होती है। पद्धतियाँ तो फिसलन से, भटकाव से बचने के लिए संकेत मात्र हैं। पद्धतियाँ तो अनुमवियों के प्रयोग हैं जिनसे सबक लेकर साधक को अपना मार्ग तय करना है।
प्रश्न यह है कि क्या भौतिकता को अध्यात्म में परिणत किया जा सकता है ? भौतिकता की निन्दा करना और उसे छोड़कर जंगल का रास्ता अपना लेना कठिन नहीं है, किन्तु इसमें साधना का सूत्र हाथ से छूट जाता है। पंचेन्द्रिय के विषयों पर विजय प्राप्त करने के लिए शास्त्रों में अनेक उपायों का उल्लेख मिलता है और यह भी कि घर छोड़कर अनगार बन जाना चाहिए । अनेक साधक मुनिवेश धारण करके विचरण भी करते हैं। प्रारम्भिक अभ्यास की दृष्टि से इसका महत्व अवश्य है, किन्तु बाद में यह सब बातें गौण हो जाती हैं। सम्यक् साधना में व्यक्ति कहीं किसी से पलायन नहीं करता और न यह अभिव्यक्त होने देता है कि वह किसी प्रकार से असामान्य या विशिष्ट है । भौतिक सामग्री या वैभव को सच्चा साधक आत्मभाव से देखता है और उसका उपयोग आध्यात्मिक दृष्टि से करता है । यहाँ फिर वही बात दोहराने को जी करता है कि कलाकार के लिए पत्थर का छोटा-सा कण भी उसकी विशाल एवं व्यापक भगवत्-भावना का अंश है। अपने कर्म को व्यक्ति जब सर्वात्मभाव से सम्पन्न करता है और उसमें उसका स्वार्थ तिरोहित हो जाता है, तब वह केवल कर्म नहीं रह जाता-वह अकर्म ही हो जाता है । योगीन्द्रदेव ने लिखा है
जहि भावइ तहि जाहि जिय जं भावइ करि तं जि ।
केम्बइ मोक्खु ण अस्थि पर चित्तहं सुद्धि णं जं जि ॥-[परमात्मप्रकाश, २,७०] -हे जीव जहां खुशी हो जाओ और जो मर्जी हो करो, किंतु जब तक चित्त शुद्ध नहीं हो तब तक मोक्ष नहीं मिलेगा।
जैन श्रमण-परम्परा की यह अनोखी विशेषता रही है कि गृहस्थवर्ग से निरंतर सम्पर्क रखते हुए भी, उनसे प्रतिदिन आहारादि प्राप्त करते हुए भी श्रमण आकांक्षाओं से परे रहते हैं, और भ्रामरीवृत्ति से विचरण करते हैं। फूल से अपनी आवश्यकता भर पराग ग्रहण करने वाले भ्रमर का जीवन जैन श्रमणों की चर्या के लिए उत्तम दृष्टान्त रूप में प्रस्तुत किया जाता है।
जैनधर्म या दर्शन का अपना कर्म-सिद्धान्त है । उसका भाग्य या कर्तव्य से दूर का भी सम्बन्ध नहीं है। यह कर्म-सिद्धान्त दार्शनिक निष्पत्ति है जिसके अनुसार व्यक्ति सम्यग्श्रद्धा, सम्यग्ज्ञान एवं सम्यक्-चारित्र के समन्वित मार्ग पर, सन्तुलनपूर्वक साधना करता हुआ अपने साध्य को प्राप्त करता है। वह त्यागने के लिए कुछ नहीं त्यागता, ग्रहण करने के लिए कुछ ग्रहण नहीं करता। उसका लक्ष्य होता है-अपनी चेतना में से सब प्रकार की जड़ता-अजीवता को समाप्त करना अथवा निर्जीवता मात्र को अपनी चेतना या स्फूर्ति द्वारा सजीव बनाकर उसके प्रति समभाव स्थापित करना।
जैनाचार्यों ने व्यर्थ साधनाओं को कोई महत्व नहीं दिया। भौतिकता में रचे-पचे लोगों के लिए ऐसी साधनाएं हैं जो आकर्षण का कारण बन सकती हैं और जिनमें किसी अनोखी चमत्कृति का दर्शन होता है। वे जन-पूज्य भी बन जाते हैं । पानी पर चलना, दीवाल को चला देना, दिन में तारे उगा देना, मनचाही वस्तु को निमिष मात्र में उपस्थित कर देना, भविष्यवाणी करना, दूसरे के मन की बात जान लेना, आग में कूद पड़ना, शूली पर लेट जाना, या शस्त्र क्रिया द्वारा अंग-भंग करना, आदि सैकड़ों प्रकार की साधनाओं में लोग वर्षों तक लगे रहते हैं। लेकिन जैनधर्म ने इन प्रक्रियाओं को लोकैषणा कहा है, कषाय कहा है। साधना तो वही उपादेय है जो राग-द्वेष से विरत करे । पंडित दौलतराम जी ने स्पष्ट कहा है
यह राग आग बहै सदा तातें शमामृत सेइये । चिर भजे विषय-कवाय, अब तो त्याग निजपद बेइये ॥ (छहढाला)
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org