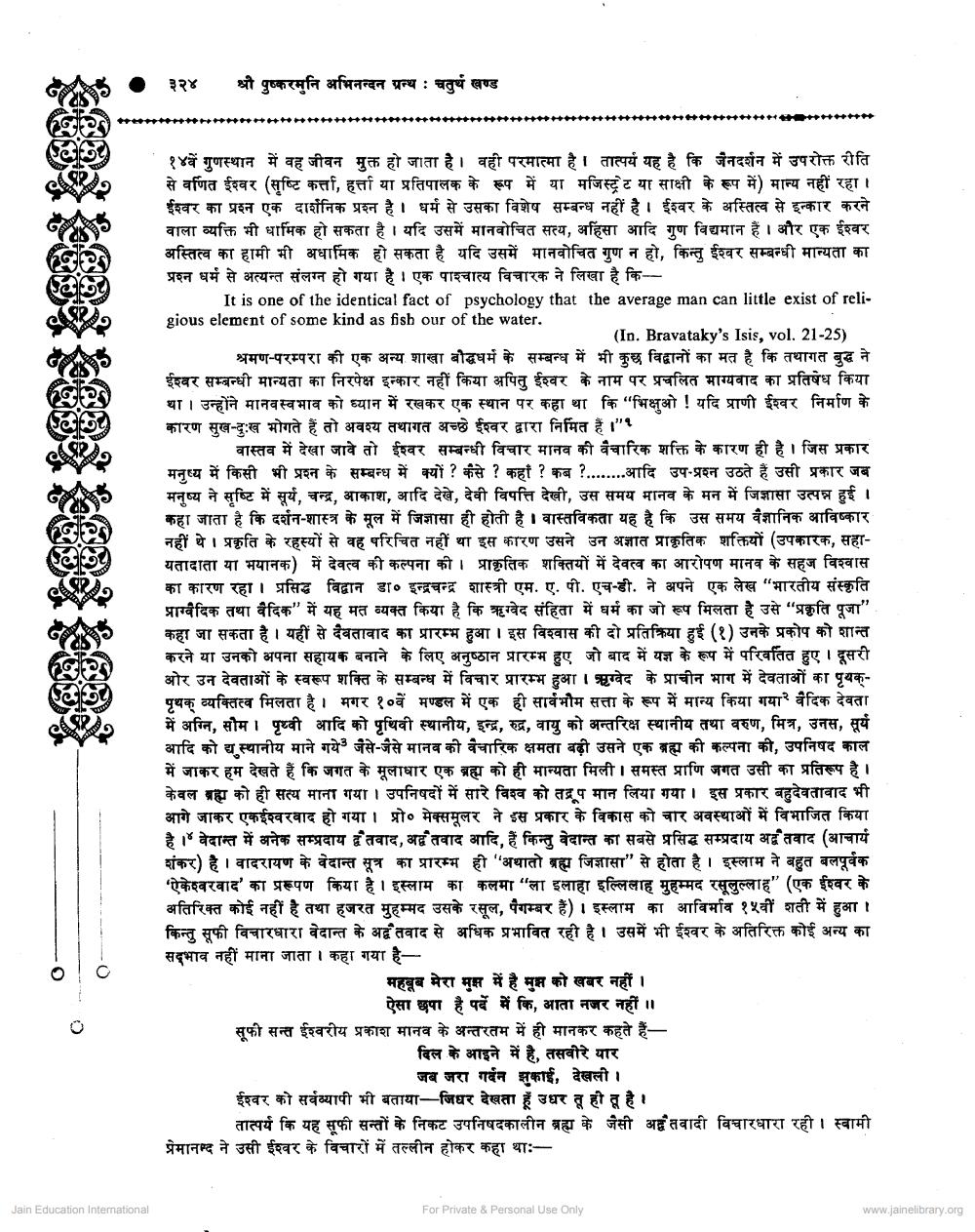________________
३२४
श्री पुष्करमुनि अभिनन्दन ग्रन्थ : चतुर्थ खण्ड
डा. इन्द्रचन्द्र प्राकृतिक शक्तिया उन अज्ञात प्राकृति
१४वें गुणस्थान में वह जीवन मुक्त हो जाता है। वही परमात्मा है । तात्पर्य यह है कि जैनदर्शन में उपरोक्त रीति से वर्णित ईश्वर (सृष्टि कर्ता, हर्ता या प्रतिपालक के रूप में या मजिस्ट्रेट या साक्षी के रूप में) मान्य नहीं रहा । ईश्वर का प्रश्न एक दार्शनिक प्रश्न है। धर्म से उसका विशेष सम्बन्ध नहीं है। ईश्वर के अस्तित्व से इन्कार करने वाला व्यक्ति भी धार्मिक हो सकता है । यदि उसमें मानवोचित सत्य, अहिंसा आदि गुण विद्यमान हैं । और एक ईश्वर अस्तित्व का हामी भी अधार्मिक हो सकता है यदि उसमें मानवोचित गुण न हो, किन्तु ईश्वर सम्बन्धी मान्यता का प्रश्न धर्म से अत्यन्त संलग्न हो गया है । एक पाश्चात्य विचारक ने लिखा है कि
It is one of the identical fact of psychology that the average man can little exist of religious element of some kind as fish our of the water.
(In. Bravataky's Isis, vol. 21-25) श्रमण-परम्परा की एक अन्य शाखा बौद्धधर्म के सम्बन्ध में भी कुछ विद्वानों का मत है कि तथागत बुद्ध ने ईश्वर सम्बन्धी मान्यता का निरपेक्ष इन्कार नहीं किया अपितु ईश्वर के नाम पर प्रचलित माग्यवाद का प्रतिषेध किया था। उन्होंने मानवस्वभाव को ध्यान में रखकर एक स्थान पर कहा था कि "भिक्षुओ! यदि प्राणी ईश्वर निर्माण के कारण सुख-दुःख भोगते हैं तो अवश्य तथागत अच्छे ईश्वर द्वारा निर्मित हैं।"
वास्तव में देखा जावे तो ईश्वर सम्बन्धी विचार मानव की वैचारिक शक्ति के कारण ही है। जिस प्रकार मनुष्य में किसी भी प्रश्न के सम्बन्ध में क्यों ? कैसे ? कहाँ ? कब ?........आदि उप-प्रश्न उठते हैं उसी प्रकार जब मनुष्य ने सृष्टि में सूर्य, चन्द्र, आकाश, आदि देखे, देवी विपत्ति देखी, उस समय मानव के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई । कहा जाता है कि दर्शन-शास्त्र के मूल में जिज्ञासा ही होती है । वास्तविकता यह है कि उस समय वैज्ञानिक आविष्कार नहीं थे। प्रकृति के रहस्यों से वह परिचित नहीं था इस कारण उसने उन अज्ञात प्राकृतिक शक्तियों (उपकारक, सहायतादाता या भयानक) में देवत्व की कल्पना की। प्राकृतिक शक्तियों में देवत्व का आरोपण मानव के सहज विश्वास का कारण रहा। प्रसिद्ध विद्वान डा० इन्द्रचन्द्र शास्त्री एम. ए. पी. एच-डी. ने अपने एक लेख "भारतीय संस्कृति प्राग्वैदिक तथा वैदिक" में यह मत व्यक्त किया है कि ऋग्वेद संहिता में धर्म का जो रूप मिलता है उसे "प्रकृति पूजा" कहा जा सकता है। यहीं से दैवतावाद का प्रारम्भ हुआ। इस विश्वास की दो प्रतिक्रिया हुई (१) उनके प्रकोप को शान्त करने या उनको अपना सहायक बनाने के लिए अनुष्ठान प्रारम्भ हुए जो बाद में यज्ञ के रूप में परिवर्तित हुए । दूसरी ओर उन देवताओं के स्वरूप शक्ति के सम्बन्ध में विचार प्रारम्भ हुआ । ऋग्वेद के प्राचीन भाग में देवताओं का पृथक्पृथक् व्यक्तित्व मिलता है। मगर १०वें मण्डल में एक ही सार्वभौम सत्ता के रूप में मान्य किया गया वैदिक देवता में अग्नि, सौम । पृथ्वी आदि को पृथिवी स्थानीय, इन्द्र, रुद्र, वायु को अन्तरिक्ष स्थानीय तथा वरुण, मित्र, उनस, सूर्य आदि को धु स्थानीय माने गये जैसे-जैसे मानव की वैचारिक क्षमता बढ़ी उसने एक ब्रह्म की कल्पना की, उपनिषद काल में जाकर हम देखते हैं कि जगत के मूलाधार एक ब्रह्म को ही मान्यता मिली। समस्त प्राणि जगत उसी का प्रतिरूप है। केवल ब्रह्म को ही सत्य माना गया। उपनिषदों में सारे विश्व को तद्रप मान लिया गया। इस प्रकार बहुदेवतावाद भी आगे जाकर एकईश्वरवाद हो गया। प्रो० मेक्समूलर ने इस प्रकार के विकास को चार अवस्थाओं में विभाजित किया है। वेदान्त में अनेक सम्प्रदाय द्वैतवाद, अद्वैतवाद आदि, हैं किन्तु वेदान्त का सबसे प्रसिद्ध सम्प्रदाय अद्वैतवाद (आचार्य शंकर) है । वादरायण के वेदान्त सूत्र का प्रारम्भ ही 'अथातो ब्रह्म जिज्ञासा" से होता है । इस्लाम ने बहुत बलपूर्वक 'ऐकेश्वरवाद' का प्ररूपण किया है । इस्लाम का कलमा "ला इलाहा इल्लिलाह मुहम्मद रसूलुल्लाह" (एक ईश्वर के अतिरिक्त कोई नहीं है तथा हजरत मुहम्मद उसके रसूल, पैगम्बर हैं) । इस्लाम का आविर्भाव १५वीं शती में हुआ। किन्तु सूफी विचारधारा वेदान्त के अद्वैतवाद से अधिक प्रभावित रही है। उसमें भी ईश्वर के अतिरिक्त कोई अन्य का सद्भाव नहीं माना जाता। कहा गया है
महबूब मेरा मुझ में है मुझ को खबर नहीं ।
ऐसा छपा है पर्दे में कि, आता नजर नहीं । सूफी सन्त ईश्वरीय प्रकाश मानव के अन्तरतम में ही मानकर कहते हैं
दिल के आइने में है, तसवीरे यार
जब जरा गर्दन झुकाई, देखली। ईश्वर को सर्वव्यापी भी बताया-जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है।
तात्पर्य कि यह सुफी सन्तों के निकट उपनिषदकालीन ब्रह्म के जैसी अद्वैतवादी विचारधारा रही। स्वामी प्रेमानन्द ने उसी ईश्वर के विचारों में तल्लीन होकर कहा थाः
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org