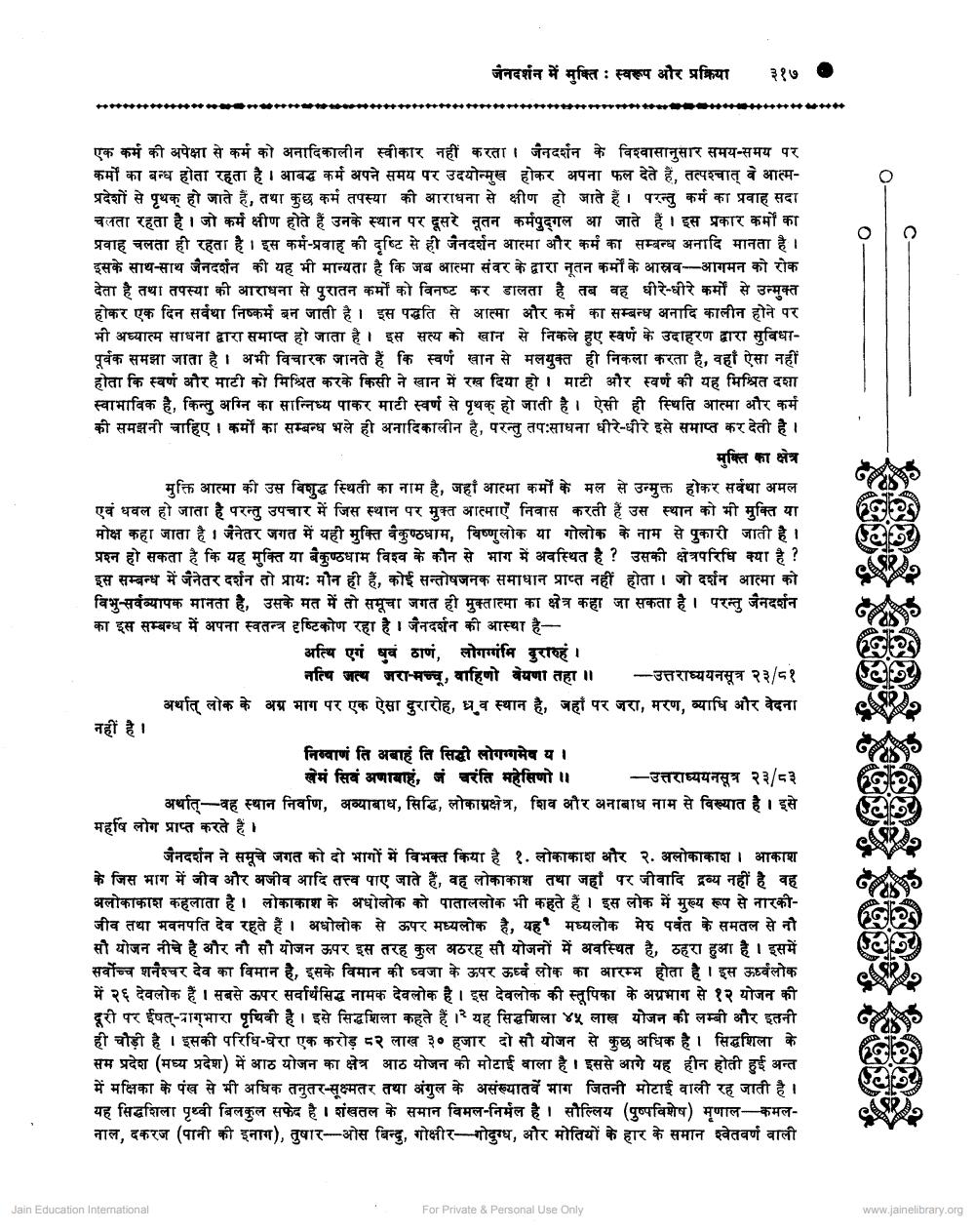________________
जनदर्शन में मुक्ति : स्वरूप और प्रक्रिया
३१७ .
एक कर्म की अपेक्षा से कर्म को अनादिकालीन स्वीकार नहीं करता। जनदर्शन के विश्वासानुसार समय-समय पर कर्मों का बन्ध होता रहता है । आबद्ध कर्म अपने समय पर उदयोन्मुख होकर अपना फल देते हैं, तत्पश्चात् वे आत्मप्रदेशों से पृथक् हो जाते हैं, तथा कुछ कर्म तपस्या की आराधना से क्षीण हो जाते हैं। परन्तु कर्म का प्रवाह सदा चलता रहता है। जो कर्म क्षीण होते हैं उनके स्थान पर दूसरे नूतन कर्मपुद्गल आ जाते हैं। इस प्रकार कर्मों का प्रवाह चलता ही रहता है। इस कर्म-प्रवाह की दृष्टि से ही जैनदर्शन आत्मा और कर्म का सम्बन्ध अनादि मानता है। इसके साथ-साथ जैनदर्शन की यह भी मान्यता है कि जब आत्मा संवर के द्वारा नूतन कर्मों के आस्रव-आगमन को रोक देता है तथा तपस्या की आराधना से पुरातन कर्मों को विनष्ट कर डालता है तब वह धीरे-धीरे कर्मों से उन्मुक्त होकर एक दिन सर्वथा निष्कर्म बन जाती है। इस पद्धति से आत्मा और कर्म का सम्बन्ध अनादि कालीन होने पर
पद्धति से आत्मा भी अध्यात्म साधना द्वारा समाप्त हो जाता है। इस सत्य को खान से निकले हुए स्वर्ण के उदाहरण द्वारा सुविधापूर्वक समझा जाता है। अभी विचारक जानते हैं कि स्वर्ण खान से मलयुक्त ही निकला करता है, वहाँ ऐसा नहीं होता कि स्वर्ण और माटी को मिश्रित करके किसी ने खान में रख दिया हो । माटी और स्वर्ण की यह मिश्रित दशा स्वाभाविक है, किन्तु अग्नि का सान्निध्य पाकर माटी स्वर्ण से पृथक् हो जाती है। ऐसी ही स्थिति आत्मा और कर्म की समझनी चाहिए । कर्मों का सम्बन्ध भले ही अनादिकालीन है, परन्तु तपःसाधना धीरे-धीरे इसे समाप्त कर देती है।
मुक्ति का क्षेत्र मुक्ति आत्मा की उस विशुद्ध स्थिती का नाम है, जहाँ आत्मा कर्मों के मल से उन्मुक्त होकर सर्वथा अमल एवं धवल हो जाता है परन्तु उपचार में जिस स्थान पर मुक्त आत्माएँ निवास करती हैं उस स्थान को भी मुक्ति या मोक्ष कहा जाता है । जैनेतर जगत में यही मुक्ति वैकुण्ठधाम, विष्णुलोक या गोलोक के नाम से पुकारी जाती है। प्रश्न हो सकता है कि यह मुक्ति या बैकुण्ठधाम विश्व के कौन से भाग में अवस्थित है ? उसकी क्षेत्रपरिधि क्या है ? इस सम्बन्ध में जैनेतर दर्शन तो प्रायः मौन ही हैं, कोई सन्तोषजनक समाधान प्राप्त नहीं होता। जो दर्शन आत्मा को विभु-सर्वव्यापक मानता है, उसके मत में तो समूचा जगत ही मुक्तात्मा का क्षेत्र कहा जा सकता है। परन्तु जैनदर्शन का इस सम्बन्ध में अपना स्वतन्त्र दृष्टिकोण रहा है । जैनदर्शन की आस्था है
अत्थि एग धुवं ठाणं, लोगग्गंमि दुरारुहं ।
नत्यि जत्य जरा-मच्चू, वाहिणो वेयणा तहा ॥ -उत्तराध्ययनसूत्र २३/८१ अर्थात् लोक के अग्र भाग पर एक ऐसा दुरारोह, ध्र व स्थान है, जहाँ पर जरा, मरण, व्याधि और वेदना नहीं है।
निग्वाणं ति अबाहं ति सिद्धी लोगग्गमेव य ।
खेमं सिवं अणाबाहं, जं चरंति महेसिणो॥ -उत्तराध्ययनसूत्र २३/८३ अर्थात्-वह स्थान निर्वाण, अव्याबाध, सिद्धि, लोकानक्षेत्र, शिव और अनाबाध नाम से विख्यात है। इसे महर्षि लोग प्राप्त करते हैं।
जैनदर्शन ने समूचे जगत को दो भागों में विभक्त किया है १. लोकाकाश और २. अलोकाकाश । आकाश के जिस भाग में जीव और अजीव आदि तत्त्व पाए जाते हैं, वह लोकाकाश तथा जहाँ पर जीवादि द्रव्य नहीं है वह अलोकाकाश कहलाता है। लोकाकाश के अधोलोक को पाताललोक भी कहते हैं। इस लोक में मुख्य रूप से नारकीजीव तथा भवनपति देव रहते हैं। अधोलोक से ऊपर मध्यलोक है, यह मध्यलोक मेरु पर्वत के समतल से नौ सौ योजन नीचे है और नौ सौ योजन ऊपर इस तरह कुल अठरह सौ योजनों में अवस्थित है, ठहरा हुआ है । इसमें सर्वोच्च शनैश्चर देव का विमान है, इसके विमान की ध्वजा के ऊपर ऊर्ध्व लोक का आरम्भ होता है । इस अवलोक में २६ देवलोक हैं । सबसे ऊपर सर्वार्थसिद्ध नामक देवलोक है । इस देवलोक की स्तूपिका के अग्रभाग से १२ योजन की दूरी पर ईषत्-वाग्भारा पृथिवी है । इसे सिद्धशिला कहते हैं। यह सिद्धशिला ४५ लाख योजन की लम्बी और इतनी ही चौड़ी है । इसकी परिधि-घेरा एक करोड़ ८२ लाख ३० हजार दो सौ योजन से कुछ अधिक है। सिद्धशिला के सम प्रदेश (मध्य प्रदेश) में आठ योजन का क्षेत्र आठ योजन की मोटाई वाला है। इससे आगे यह हीन होती हुई अन्त में मक्षिका के पंख से भी अधिक तनुतर-सूक्ष्मतर तथा अंगुल के असंख्यातवें भाग जितनी मोटाई वाली रह जाती है। यह सिद्धशिला पृथ्वी बिलकुल सफेद है । शंखतल के समान विमल-निर्मल है। सौल्लिय (पुष्पविशेष) मृणाल-कमलनाल, दकरज (पानी की इनाग), तुषार-ओस बिन्दु, गोक्षीर-गोदुग्ध, और मोतियों के हार के समान श्वेतवर्ण वाली
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org