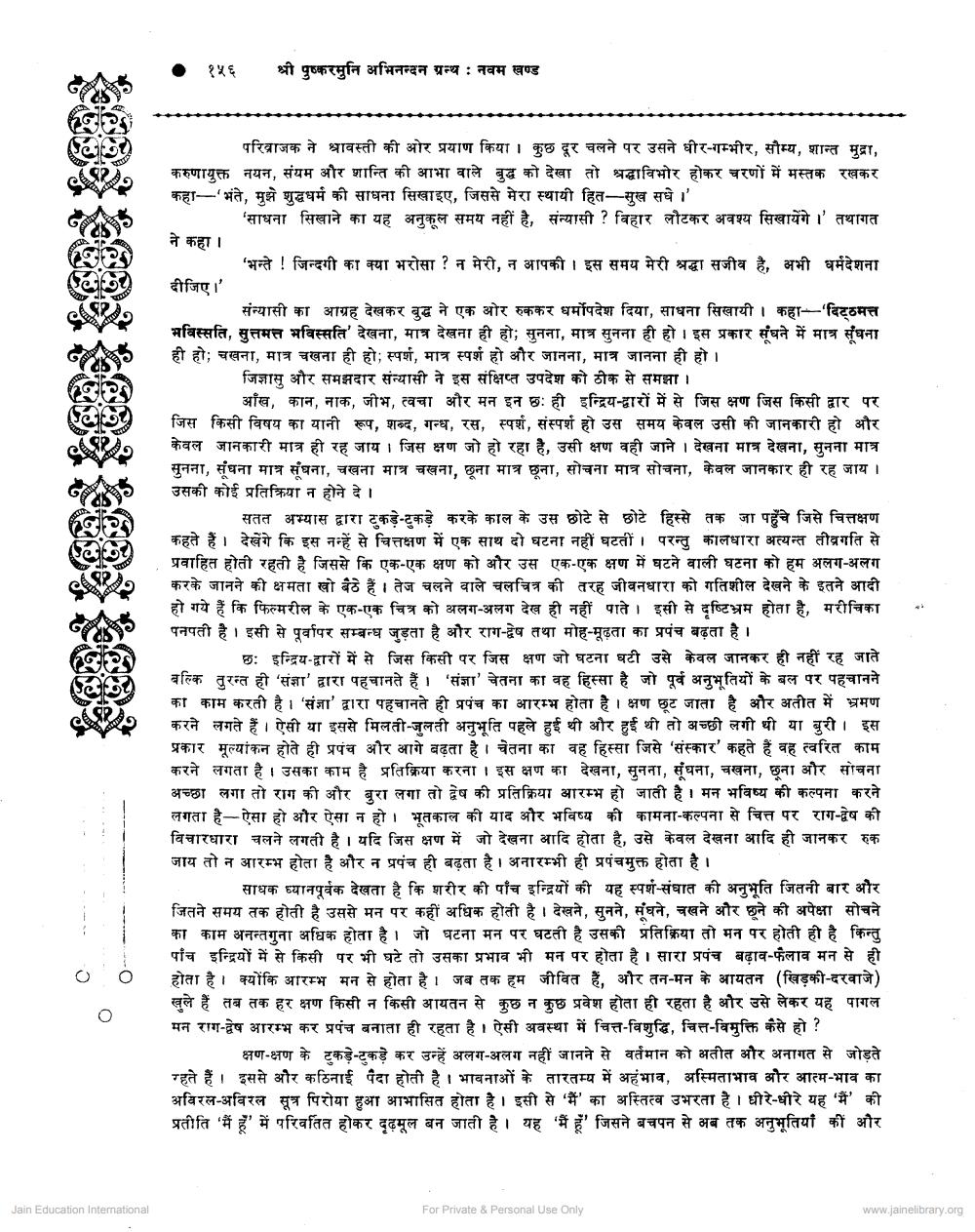________________
। १५६
श्री पुष्करमुनि अभिनन्दन ग्रन्थ : नवम खण्ड
परिव्राजक ने श्रावस्ती की ओर प्रयाण किया। कुछ दूर चलने पर उसने धीर-गम्भीर, सौम्य, शान्त मुद्रा, करुणायुक्त नयन, संयम और शान्ति की आभा वाले बुद्ध को देखा तो श्रद्धाविभोर होकर चरणों में मस्तक रखकर कहा- भंते, मुझे शुद्धधर्म की साधना सिखाइए, जिससे मेरा स्थायी हित-सूख सधे ।'
'साधना सिखाने का यह अनुकूल समय नहीं है, संन्यासी ? विहार लौटकर अवश्य सिखायेंगे।' तथागत ने कहा।
भन्ते ! जिन्दगी का क्या भरोसा ? न मेरी, न आपकी । इस समय मेरी श्रद्धा सजीव है, अभी धर्मदेशना दीजिए।'
संन्यासी का आग्रह देखकर बुद्ध ने एक ओर रुककर धर्मोपदेश दिया, साधना सिखायी। कहा-'विट्ठमत्त भविस्सति, सुत्तमत्त भविस्सति' देखना, मात्र देखना ही हो; सुनना, मात्र सुनना ही हो । इस प्रकार सूंघने में मात्र सूंघना ही हो; चखना, मात्र चखना ही हो; स्पर्श, मात्र स्पर्श हो और जानना, मात्र जानना ही हो।
जिज्ञासू और समझदार संन्यासी ने इस संक्षिप्त उपदेश को ठीक से समझा।
आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा और मन इन छः ही इन्द्रिय-द्वारों में से जिस क्षण जिस किसी द्वार पर जिस किसी विषय का यानी रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्पर्श, संस्पर्श हो उस समय केवल उसी की जानकारी हो और केवल जानकारी मात्र ही रह जाय । जिस क्षण जो हो रहा है, उसी क्षण वही जाने । देखना मात्र देखना, सुनना मात्र सुनना, सूंघना मात्र संघना, चखना मात्र चखना, छूना मात्र छूना, सोचना मात्र सोचना, केवल जानकार ही रह जाय । उसकी कोई प्रतिक्रिया न होने दे।
सतत अभ्यास द्वारा टुकड़े-टुकड़े करके काल के उस छोटे से छोटे हिस्से तक जा पहुँचे जिसे चित्तक्षण कहते हैं। देखेंगे कि इस नन्हें से चित्तक्षण में एक साथ दो घटना नहीं घटतीं। परन्तु कालधारा अत्यन्त तीव्रगति से प्रवाहित होती रहती है जिससे कि एक-एक क्षण को और उस एक-एक क्षण में घटने वाली घटना को हम अलग-अलग करके जानने की क्षमता खो बैठे हैं। तेज चलने वाले चलचित्र की तरह जीवनधारा को गतिशील देखने के इतने आदी हो गये हैं कि फिल्मरील के एक-एक चित्र को अलग-अलग देख ही नहीं पाते। इसी से दृष्टिभ्रम होता है, मरीचिका पनपती है । इसी से पूर्वापर सम्बन्ध जुड़ता है और राग-द्वेष तथा मोह-मूढ़ता का प्रपंच बढ़ता है।
छ: इन्द्रिय-द्वारों में से जिस किसी पर जिस क्षण जो घटना घटी उसे केवल जानकर ही नहीं रह जाते बल्कि तुरन्त ही 'संज्ञा' द्वारा पहचानते हैं। 'संज्ञा' चेतना का वह हिस्सा है जो पूर्व अनुभूतियों के बल पर पहचानने का काम करती है। 'संज्ञा' द्वारा पहचानते ही प्रपंच का आरम्भ होता है । क्षण छूट जाता है और अतीत में भ्रमण करने लगते हैं । ऐसी या इससे मिलती-जुलती अनुभूति पहले हुई थी और हुई थी तो अच्छी लगी थी या बुरी। इस प्रकार मूल्यांकन होते ही प्रपंच और आगे बढ़ता है। चेतना का वह हिस्सा जिसे 'संस्कार' कहते हैं वह त्वरित काम करने लगता है। उसका काम है प्रतिक्रिया करना । इस क्षण का देखना, सुनना, सूंघना, चखना, छूना और सोचना अच्छा लगा तो राग की और बुरा लगा तो द्वेष की प्रतिक्रिया आरम्भ हो जाती है। मन भविष्य की कल्पना करने लगता है-ऐसा हो और ऐसा न हो। भूतकाल की याद और भविष्य की कामना-कल्पना से चित्त पर राग-द्वेष की विचारधारा चलने लगती है। यदि जिस क्षण में जो देखना आदि होता है, उसे केवल देखना आदि ही जानकर रुक जाय तो न आरम्भ होता है और न प्रपंच ही बढ़ता है। अनारम्भी ही प्रपंचमुक्त होता है।
__साधक ध्यानपूर्वक देखता है कि शरीर की पाँच इन्द्रियों की यह स्पर्श-संघात की अनुभूति जितनी बार और जितने समय तक होती है उससे मन पर कहीं अधिक होती है। देखने, सुनने, संघने, चखने और छुने की अपेक्षा सोचने का काम अनन्तगुना अधिक होता है। जो घटना मन पर घटती है उसकी प्रतिक्रिया तो मन पर होती ही है किन्तु पाँच इन्द्रियों में से किसी पर भी घटे तो उसका प्रभाव भी मन पर होता है। सारा प्रपंच बढ़ाव-फैलाव मन से ही होता है। क्योंकि आरम्भ मन से होता है। जब तक हम जीवित हैं, और तन-मन के आयतन (खिड़की-दरवाजे) खुले हैं तब तक हर क्षण किसी न किसी आयतन से कुछ न कुछ प्रवेश होता ही रहता है और उसे लेकर यह पागल मन राग-द्वेष आरम्भ कर प्रपंच बनाता ही रहता है। ऐसी अवस्था में चित्त-विशुद्धि, चित्त-विमुक्ति कैसे हो?
क्षण-क्षण के टुकड़े-टुकड़े कर उन्हें अलग-अलग नहीं जानने से वर्तमान को अतीत और अनागत से जोड़ते रहते हैं। इससे और कठिनाई पैदा होती है। भावनाओं के तारतम्य में अहंभाव, अस्मिताभाव और आत्म-भाव का अविरल-अविरल सूत्र पिरोया हुआ आभासित होता है। इसी से 'मैं' का अस्तित्व उभरता है । धीरे-धीरे यह 'मैं' की प्रतीति 'मैं हूँ' में परिवर्तित होकर दृढमूल बन जाती है। यह 'मैं हूँ' जिसने बचपन से अब तक अनुभूतियां की और
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org