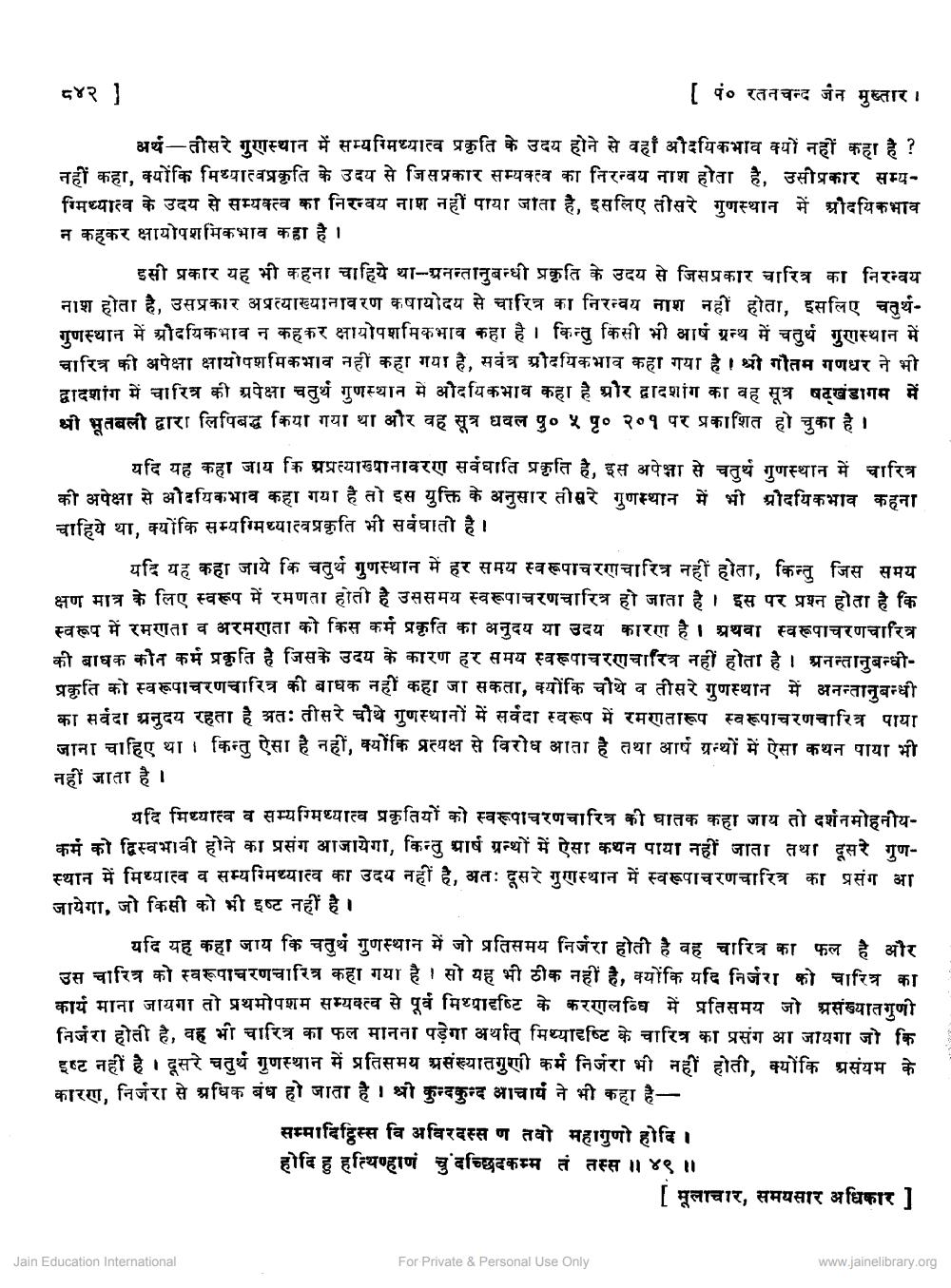________________
८४२ ]
[ पं० रतनचन्द जैन मुख्तार ।
अर्थ-तीसरे गुरणस्थान में सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृति के उदय होने से वहाँ औदयिकभाव क्यों नहीं कहा है ? नहीं कहा, क्योंकि मिथ्यात्वप्रकृति के उदय से जिस प्रकार सम्यक्त्व का निरन्वय नाश होता है, उसीप्रकार सम्यमिथ्यात्व के उदय से सम्यक्त्व का निरन्वय नाश नहीं पाया जाता है, इसलिए तीसरे गुणस्थान में प्रौदयिकभाव न कहकर क्षायोपशमिकभाव कहा है।
इसी प्रकार यह भी कहना चाहिये था-अनन्तानुबन्धी प्रकृति के उदय से जिसप्रकार चारित्र का निरन्वय नाश होता है. उसप्रकार अप्रत्याख्यानावरण कषायोदय से चारित्र का निरन्वय नाश नहीं होता. इसलिए चतुर्थगणस्थान में प्रौदयिकभाव न कहकर क्षायोपशमिकभाव कहा है। किन्तु किसी भी आर्ष ग्रन्थ में चतुर्थ गुणस्थान में चारित्र की अपेक्षा क्षायोपशमिकभाव नहीं कहा गया है, सर्वत्र प्रौदयिकभाव कहा गया है। श्री गौतम गणधर ने भी द्वादशांग में चारित्र की अपेक्षा चतुर्थ गुणस्थान में औदयिकभाव कहा है और द्वादशांग का वह सूत्र षट्खंडागम में श्री भूतबली द्वारा लिपिबद्ध किया गया था और वह सूत्र धवल पु०५ पृ० २०१ पर प्रकाशित हो चुका है।
यदि यह कहा जाय कि अप्रत्याख्यानावरण सर्वघाति प्रकृति है, इस अपेक्षा से चतुर्थ गुणस्थान में चारित्र की अपेक्षा से औदायकभाव कहा गया है तो इस युक्ति के अनुसार तीसरे गुणस्थान में भी प्रौदयिकभाव कहना चाहिये था, क्योंकि सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृति भी सर्वघाती है।
यदि यह कहा जाये कि चतुर्थ गुणस्थान में हर समय स्वरूपाचरणचारित्र नहीं होता, किन्तु जिस समय क्षण मात्र के लिए स्वरूप में रमणता होती है उससमय स्वरूपाचरणचारित्र हो जाता है। इस पर प्रश्न होता है कि स्वरूप में रमणता व अरमणता को किस कर्म प्रकृति का अनुदय या उदय कारण है। अथवा स्वरूपाचरणचारित्र को बाधक कौन कर्म प्रकृति है जिसके उदय के कारण हर समय स्वरूपाचरणचारित्र नहीं होता है। अनन्तानुबन्धीप्रकृति को स्वरूपाचरणचारित्र की बाधक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि चौथे व तीसरे गुणस्थान में अनन्तानुबन्धी कामवंदा अनदय रहता है अतः तीसरे चौथे गुणस्थानों में सर्वदा स्वरूप में रमणतारूप स्वरूपाचरणचारित्र पाया जाना चाहिए था। किन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष से विरोध आता है तथा आर्ष ग्रन्थों में ऐसा कथन पाया भी नहीं जाता है।
यदि मिथ्यात्व व सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृतियों को स्वरूपाचरणचारित्र की घातक कहा जाय तो दर्शनमोहनीयकर्म को द्विस्वभावी होने का प्रसंग आजायेगा, किन्तु प्रार्ष ग्रन्थों में ऐसा कथन पाया नहीं जाता तथा दूसरे गुणस्थान में मिथ्यात्व व सम्यग्मिथ्यात्व का उदय नहीं है, अतः दूसरे गुणस्थान में स्वरूपाचरणचारित्र का प्रसंग आ जायेगा, जो किसी को भी इष्ट नहीं है।
यदि यह कहा जाय कि चतुर्थ गुणस्थान में जो प्रतिसमय निर्जरा होती है वह चारित्र का फल है और उस चारित्र को स्वरूपाचरणचारित्र कहा गया है । सो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि यदि निर्जरा को चारित्र का का माना जायगा तो प्रथमोपशम सम्यक्त्व से पूर्व मिथ्यादृष्टि के करपलब्धि में प्रतिसमय जो असंख्यातगणी निर्जरा होती है, वह भी चारित्र का फल मानना पड़ेगा अर्थात् मिथ्यादृष्टि के चारित्र का प्रसंग आ जायगा जो कि इष्ट नहीं है । दूसरे चतुर्थ गुणस्थान में प्रतिसमय असंख्यातगुणी कर्म निर्जरा भी नहीं होती, क्योंकि प्रसंयम के कारण. निर्जरा से अधिक बंध हो जाता है। श्री कुन्दकुन्द आचार्य ने भी कहा है
सम्मादिद्धिस्स वि अविरदस्स ण तवो महागुणो होदि । होदि हु हत्थिण्हाणं चुदच्छिदकम्म तं तस्स ॥ ४९ ॥
[ मूलाचार, समयसार अधिकार ]
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org