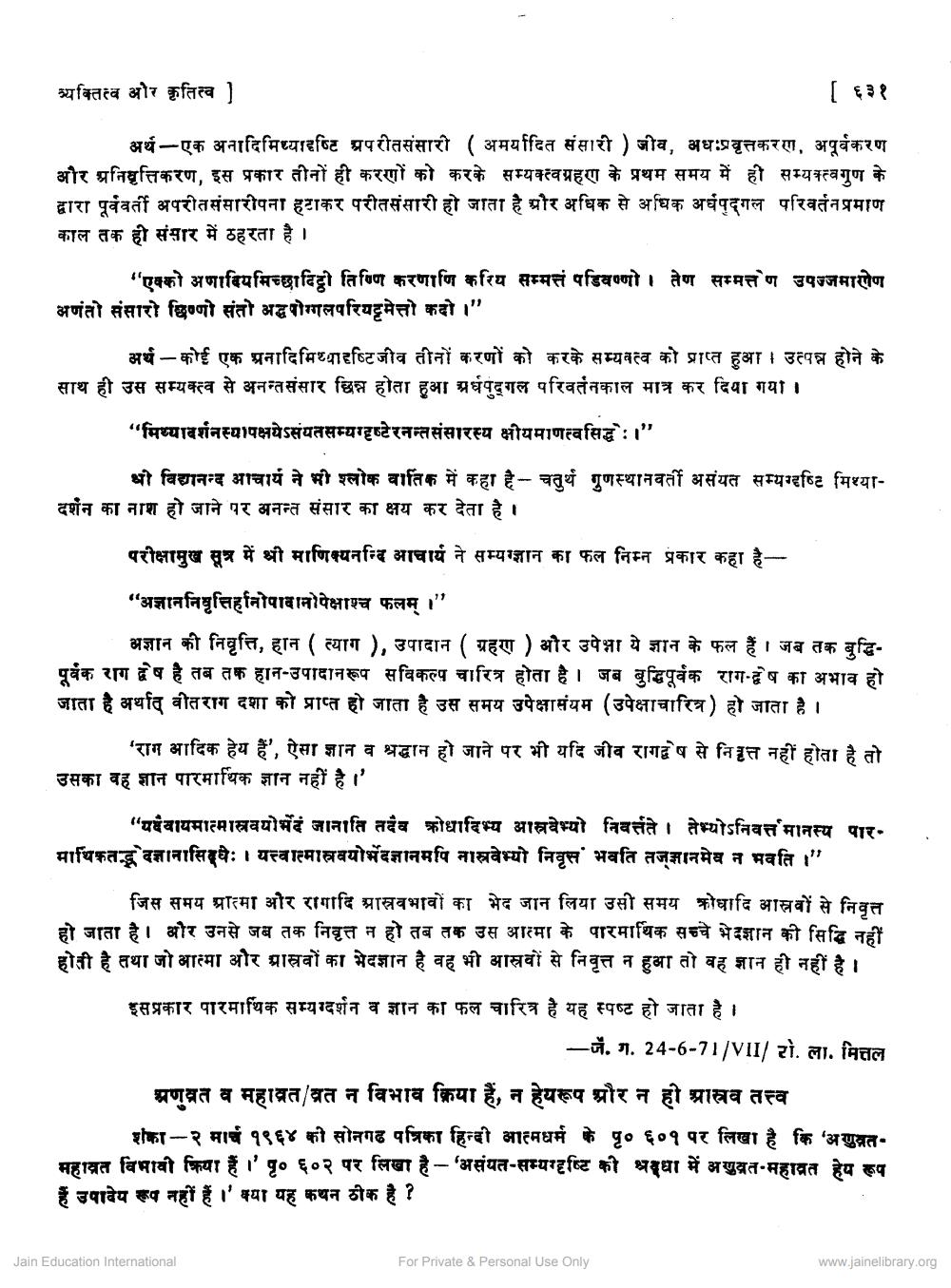________________
व्यक्तित्व और कृतित्व ]
[ ६३१
अर्थ-एक अनादिमिध्यादृष्टि अपरीतसंसारी ( अमर्यादित संसारी) जीव, अधःप्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, इस प्रकार तीनों ही कररणों को करके सम्यक्त्वग्रहरण के प्रथम समय में ही सम्यक्त्वगुण के द्वारा पूर्ववर्ती अपरीतसंसारीपना हटाकर परीतसंसारी हो जाता है और अधिक से अधिक अर्धपदगल परिवर्तन प्रमाण काल तक ही संसार में ठहरता है ।
"एक्को अणादियमिच्छादिट्ठी तिण्णि करणाणि करिय सम्मत्तं पडिवण्णो। तेण सम्मत्तण उपज्जमाणेण अणंतो संसारो छिण्णो संतो अद्धपोग्गलपरियट्टमेत्तो कदो।"
अर्थ-कोई एक अनादिमिथ्याष्टि जीव तीनों करणों को करके सम्यक्त्व को प्राप्त हुआ। उत्पन्न होने के साथ ही उस सम्यक्त्व से अनन्तसंसार छिन्न होता हुआ अर्धपुद्गल परिवर्तनकाल मात्र कर दिया गया।
"मिथ्यावर्शनस्यापक्षयेऽसंयतसम्यग्दृष्टेरनन्तसंसारस्य क्षीयमाणत्वसिद्ध।"
श्री विद्यानन्द आचार्य ने भी श्लोक वार्तिक में कहा है- चतुर्थ गुणस्थानवर्ती असंयत सम्यग्दृष्टि मिथ्यादर्शन का नाश हो जाने पर अनन्त संसार का क्षय कर देता है ।
परीक्षामुख सूत्र में श्री माणिक्यनन्दि आचार्य ने सम्यग्ज्ञान का फल निम्न प्रकार कहा है"अज्ञाननिवृत्तिानोपावानोपेक्षाश्च फलम् ।"
अज्ञान की निवृत्ति, हान ( त्याग ), उपादान ( ग्रहण ) और उपेक्षा ये ज्ञान के फल हैं । जब तक बुद्धिपूर्वक राग द्वेष है तब तक हान-उपादानरूप सविकल्प चारित्र होता है। जब बुद्धिपूर्वक राग-द्वेष का अभाव हो जाता है अर्थात वीतराग दशा को प्राप्त हो जाता है उस समय उपेक्षासंयम (उपेक्षाचारित्र) हो जाता है।
'राग आदिक हेय हैं', ऐसा ज्ञान व श्रद्धान हो जाने पर भी यदि जीव रागद्वेष से निवृत्त नहीं होता है तो उसका वह ज्ञान पारमार्थिक ज्ञान नहीं है।'
"यवायमात्मास्रवयोअंदं जानाति तदेव क्रोधादिभ्य आस्रवेभ्यो निवर्तते । तेभ्योऽनिवर्तमानस्य पार. माथिकतद्भवज्ञानासिधैः । यत्त्वात्मास्त्रवयोर्मेंदज्ञानमपि नास्रवेभ्यो निवृस भवति तज्ज्ञानमेव न भवति ।"
जिस समय प्रात्मा और रागादि प्रास्रवभावों का भेद जान लिया उसी समय क्रोधादि आस्रवों से निवृत्त हो जाता है। और उनसे जब तक निवृत्त न हो तब तक उस आत्मा के पारमार्थिक सच्चे भेदज्ञान की सिद्धि नहीं होती है तथा जो आत्मा और प्रास्रबों का भेदज्ञान है वह भी आस्रवों से निवृत्त न हआ तो वह ज्ञान ही नहीं है।
इसप्रकार पारमार्थिक सम्यग्दर्शन व ज्ञान का फल चारित्र है यह स्पष्ट हो जाता है ।
-जं. ग. 24-6-71/VII/ रो. ला. मित्तल अणुव्रत व महाव्रत/व्रत न विभाव क्रिया हैं, न हेयरूप और न ही प्रास्त्रव तत्त्व
शंका-२ मार्च १९६४ को सोनगढ पत्रिका हिन्दी आत्मधर्म के पृ० ६०१ पर लिखा है कि 'अणुव्रतमहावत विभावी क्रिया हैं ।' पृ०६०२ पर लिखा है - 'असंयत-सम्यग्दृष्टि की श्रद्धा में अणुव्रत-महावत हेय रूप हैं उपादेय रूप नहीं हैं। क्या यह कथन ठीक है?
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org