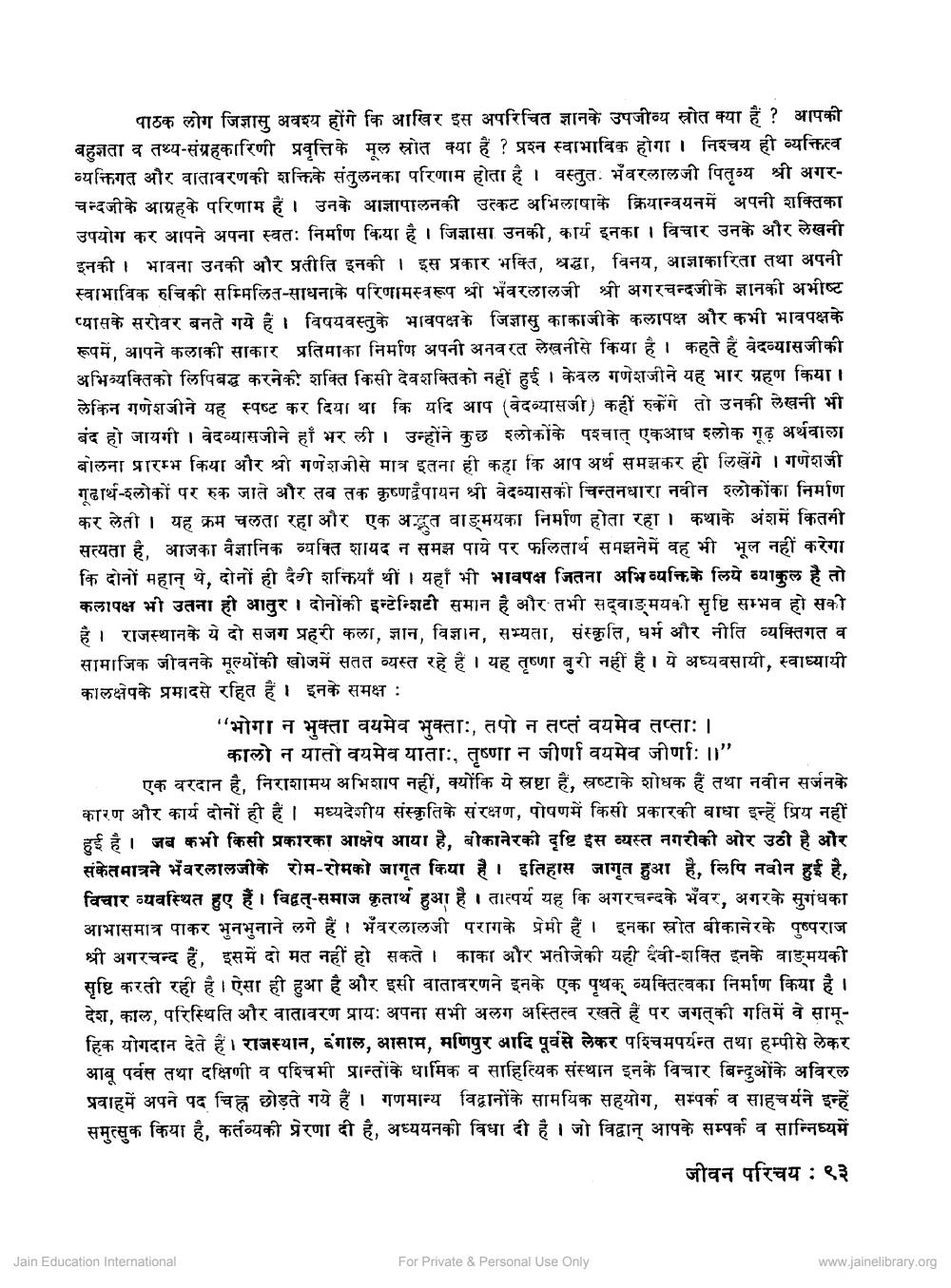________________
पाठक लोग जिज्ञासु अवश्य होंगे कि आखिर इस अपरिचित ज्ञानके उपजीव्य स्रोत क्या हैं ? आपकी बहुज्ञता व तथ्य-संग्रहकारिणी प्रवृत्ति के मूल स्रोत क्या हैं ? प्रश्न स्वाभाविक होगा। निश्चय ही व्यक्तित्व व्यक्तिगत और वातावरणकी शक्तिके संतुलनका परिणाम होता है । वस्तुत. भँवरलालजी पितृव्य श्री अगरचन्दजीके आग्रहके परिणाम है। उनके आज्ञापालनकी उत्कट अभिलाषाके क्रियान्वयनमें अपनी शक्तिका उपयोग कर आपने अपना स्वतः निर्माण किया है । जिज्ञासा उनकी, कार्य इनका । विचार उनके और लेखनी इनकी। भावना उनकी और प्रतीति इनकी । इस प्रकार भक्ति, श्रद्धा, विनय, आज्ञाकारिता तथा अपनी स्वाभाविक रुचिकी सम्मिलित-साधनाके परिणामस्वरूप श्री भंवरलालजी श्री अगरचन्दजीके ज्ञानकी अभीष्ट प्यासके सरोवर बनते गये हैं। विषयवस्तुके भावपक्षके जिज्ञासु काकाजीके कलापक्ष और कभी भावपक्षके रूपमें, आपने कलाकी साकार प्रतिमाका निर्माण अपनी अनवरत लेखनीसे किया है। कहते है वेदव्यासजीकी अभिव्यक्तिको लिपिबद्ध करने की शक्ति किसी देवशक्तिको नहीं हुई । केवल गणेशजीने यह भार ग्रहण किया। लेकिन गणेशजीने यह स्पष्ट कर दिया था कि यदि आप (वेदव्यासजी) कहीं रुकेंगे तो उनकी लेखनी भी बंद हो जायगी । वेदव्यासजीने हाँ भर ली। उन्होंने कुछ श्लोकोंके पश्चात् एकआध श्लोक गूढ़ अर्थवाला बोलना प्रारम्भ किया और श्री गणेशजोसे मात्र इतना ही कहा कि आप अर्थ समझकर ही लिखेंगे । गणेशजी गूढार्थ-श्लोकों पर रुक जाते और तब तक कृष्णद्वैपायन श्री वेदव्यासकी चिन्तनधारा नवीन श्लोकोंका निर्माण कर लेती। यह क्रम चलता रहा और एक अद्भत वाङ्मयका निर्माण होता रहा। कथाके अंशमें कितमी सत्यता है, आजका वैज्ञानिक व्यक्ति शायद न समझ पाये पर फलितार्थ समझने में वह भी भूल नहीं करेगा कि दोनों महान थे, दोनों ही दैवी शक्तियाँ थीं। यहाँ भी भावपक्ष जितना अभिव्यक्तिके लिये व्याकुल है तो कलापक्ष भी उतना ही आतुर । दोनोंकी इन्टेन्शिटी समान है और तभी सवाङ्मयकी सृष्टि सम्भव हो सकी है। राजस्थानके ये दो सजग प्रहरी कला, ज्ञान, विज्ञान, सभ्यता, संस्कृति, धर्म और नीति व्यक्तिगत व सामाजिक जीवनके मूल्योंकी खोजमें सतत व्यस्त रहे हैं । यह तृष्णा बुरी नहीं है। ये अध्यवसायी, स्वाध्यायी कालक्षेपके प्रमादसे रहित हैं। इनके समक्ष :
"भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ताः, तपो न तप्तं वयमेव तप्ताः ।
कालो न यातो वयमेव याताः तष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णाः " एक वरदान है, निराशामय अभिशाप नहीं, क्योंकि ये स्रष्टा है, स्रष्टाके शोधक हैं तथा नवीन सर्जनके कारण और कार्य दोनों ही हैं। मध्यदेशीय संस्कृतिके संरक्षण, पोषणमें किसी प्रकारकी बाधा इन्हें प्रिय नहीं हई है। जब कभी किसी प्रकारका आक्षेप आया है, बीकानेरको दृष्टि इस व्यस्त नगरीकी ओर उठी है और संकेतमात्रने भंवरलालजीके रोम-रोमको जागत किया है। इतिहास जागृत हुआ है, लिपि नवीन हुई है, विचार व्यवस्थित हुए हैं। विद्वत्-समाज कृतार्थ हुआ है । तात्पर्य यह कि अगरचन्दके भंवर, अगरके सुगंधका आभासमात्र पाकर भुनभुनाने लगे हैं। भवरलालजी परागके प्रेमी हैं। इनका स्रोत बीकानेरके पुष्पराज श्री अगरचन्द है, इसमें दो मत नहीं हो सकते। काका और भतीजेकी यही देवी-शक्ति इनके वाङ्मयकी सृष्टि करती रही है। ऐसा ही हुआ है और इसी वातावरणने इनके एक पृथक् व्यक्तित्वका निर्माण किया है। देश, काल, परिस्थिति और वातावरण प्रायः अपना सभी अलग अस्तित्व रखते हैं पर जगत्की गतिमें वे सामूहिक योगदान देते हैं। राजस्थान, बंगाल, आसाम, मणिपुर आदि पूर्व से लेकर पश्चिमपर्यन्त तथा हम्पीसे लेकर आबू पर्वत तथा दक्षिणी व पश्चिमी प्रान्तोंके धार्मिक व साहित्यिक संस्थान इनके विचार बिन्दुओंके अविरल प्रवाहमें अपने पद चिह्न छोड़ते गये हैं। गणमान्य विद्वानोंके सामयिक सहयोग, सम्पर्क व साहचर्यने इन्हें समत्सक किया है, कर्तव्यकी प्रेरणा दी है, अध्ययनको विधा दी है। जो विद्वान आपके सम्पर्क व सान्निध्यमें
जीवन परिचय : ९३
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org