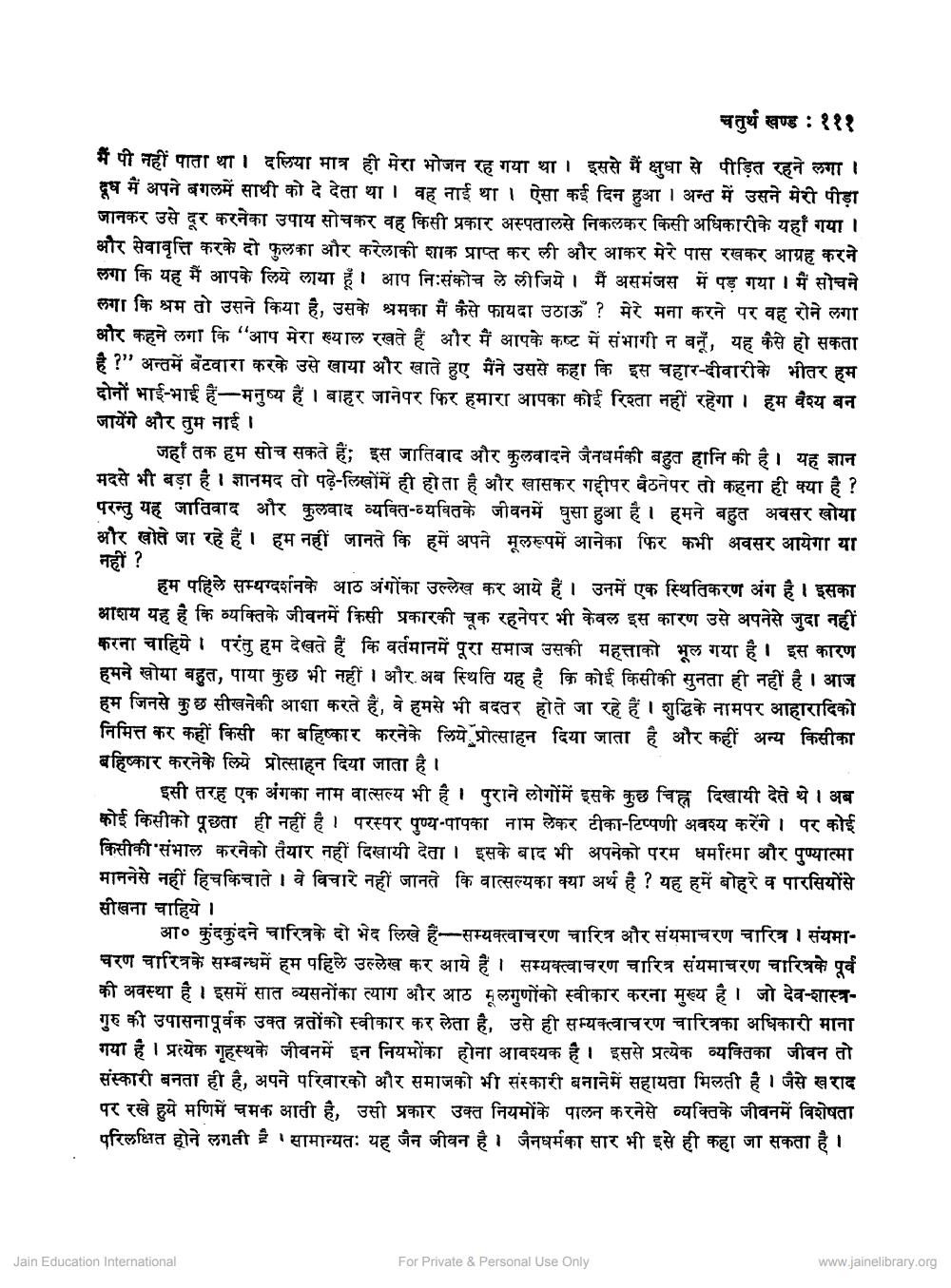________________
चतुर्थ खण्ड : १११
मैं पी नहीं पाता था। दलिया मात्र ही मेरा भोजन रह गया था। इससे मैं क्षुधा से पीड़ित रहने लगा। दूध मैं अपने बगलमें साथी को दे देता था। वह नाई था। ऐसा कई दिन हुआ । अन्त में उसने मेरी पीड़ा जानकर उसे दूर करनेका उपाय सोचकर वह किसी प्रकार अस्पतालसे निकलकर किसी अधिकारीके यहाँ गया। और सेवावत्ति करके दो फलका और करेलाको शाक प्राप्त कर ली और आकर मेरे पास रखकर आग्रह करने लगा कि यह मैं आपके लिये लाया हूँ। आप निःसंकोच ले लीजिये। मैं असमंजस में पड़ गया । मैं सोचने लगा कि श्रम तो उसने किया है, उसके श्रमका मैं कैसे फायदा उठाऊँ ? मेरे मना करने पर वह रोने लगा और कहने लगा कि "आप मेरा ख्याल रखते हैं और मैं आपके कष्ट में संभागी न बनें, यह कैसे हो सकता है ?" अन्तमें बँटवारा करके उसे खाया और खाते हुए मैंने उससे कहा कि इस चहार-दीवारीके भीतर हम दोनों भाई-भाई हैं-मनुष्य है । बाहर जानेपर फिर हमारा आपका कोई रिश्ता नहीं रहेगा। हम वैश्य बन जायेंगे और तुम नाई।
जहाँ तक हम सोच सकते हैं; इस जातिवाद और कुलवादने जैनधर्मकी बहुत हानि की है। यह ज्ञान मदसे भी बड़ा है। ज्ञानमद तो पढ़े-लिखोंमें ही होता है और खासकर गद्दीपर बैठनेपर तो कहना ही क्या है ? परन्तु यह जातिवाद और कुलवाद व्यक्ति-व्यक्तिके जीवन में घुसा हुआ है। हमने बहुत अवसर खोया और खोते जा रहे हैं। हम नहीं जानते कि हमें अपने मूलरूपमें आनेका फिर कभी अवसर आयेगा या नहीं?
हम पहिले सम्यग्दर्शनके आठ अंगोंका उल्लेख कर आये हैं। उनमें एक स्थितिकरण अंग है। इसका आशय यह है कि व्यक्तिके जीवनमें किसी प्रकारकी चूक रहनेपर भी केवल इस कारण उसे अपनेसे जुदा नहीं करना चाहिये। परंतु हम देखते हैं कि वर्तमानमें पूरा समाज उसकी महत्ताको भल गया है। इस कारण हमने खोया बहत, पाया कुछ भी नहीं। और अब स्थिति यह है कि कोई किसीकी सुनता ही न हम जिनसे कुछ सीखनेकी आशा करते है, वे हमसे भी बदतर होते जा रहे हैं । शुद्धिके नामपर आहारादिको निमित्त कर कहीं किसी का बहिष्कार करनेके लिये प्रोत्साहन दिया जाता है और कहीं अन्य किसीका बहिष्कार करनेके लिये प्रोत्साहन दिया जाता है।
इसी तरह एक अंगका नाम वात्सल्य भी है। पुराने लोगोंमें इसके कुछ चिह्न दिखायी देते थे। अब कोई किसीको पूछता ही नहीं है। परस्पर पुण्य-पापका नाम लेकर टीका-टिप्पणी अवश्य करेंगे। पर कोई किसीकी संभाल करनेको तैयार नहीं दिखायी देता। इसके बाद भी अपनेको परम धर्मात्मा और पुण्यात्मा माननेसे नहीं हिचकिचाते । वे विचारे नहीं जानते कि वात्सल्यका क्या अर्थ है ? यह हमें बोहरे व पारसियोंसे सीखना चाहिये।
आ० कुंदकूदने चारित्रके दो भेद लिखे हैं-सम्यक्त्वाचरण चारित्र और संयमाचरण चारित्र । संयमाचरण चारित्रके सम्बन्धमें हम पहिले उल्लेख कर आये हैं। सम्यक्त्वाचरण चारित्र संयमाचरण चारित्रके पूर्व की अवस्था है। इसमें सात व्यसनोंका त्याग और आठ मूलगुणोंको स्वीकार करना मुख्य है। जो देव-शास्त्रगुरु की उपासनापूर्वक उक्त व्रतोंको स्वीकार कर लेता है, उसे ही सम्यक्त्वाचरण चारित्रका अधिकारी माना गया है । प्रत्येक गृहस्थके जीवनमें इन नियमोंका होना आवश्यक है। इससे प्रत्येक व्यक्तिका जीवन तो संस्कारी बनता ही है, अपने परिवारको और समाजको भी संस्कारी बनाने में सहायता मिलती है । जैसे खराद पर रखे हुये मणिमें चमक आती है, उसी प्रकार उक्त नियमोंके पालन करनेसे व्यक्तिके जीवनमें विशेषता परिलक्षित होने लगती है । सामान्यतः यह जैन जीवन है। जैनधर्मका सार भी इसे ही कहा जा सकता है ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org |