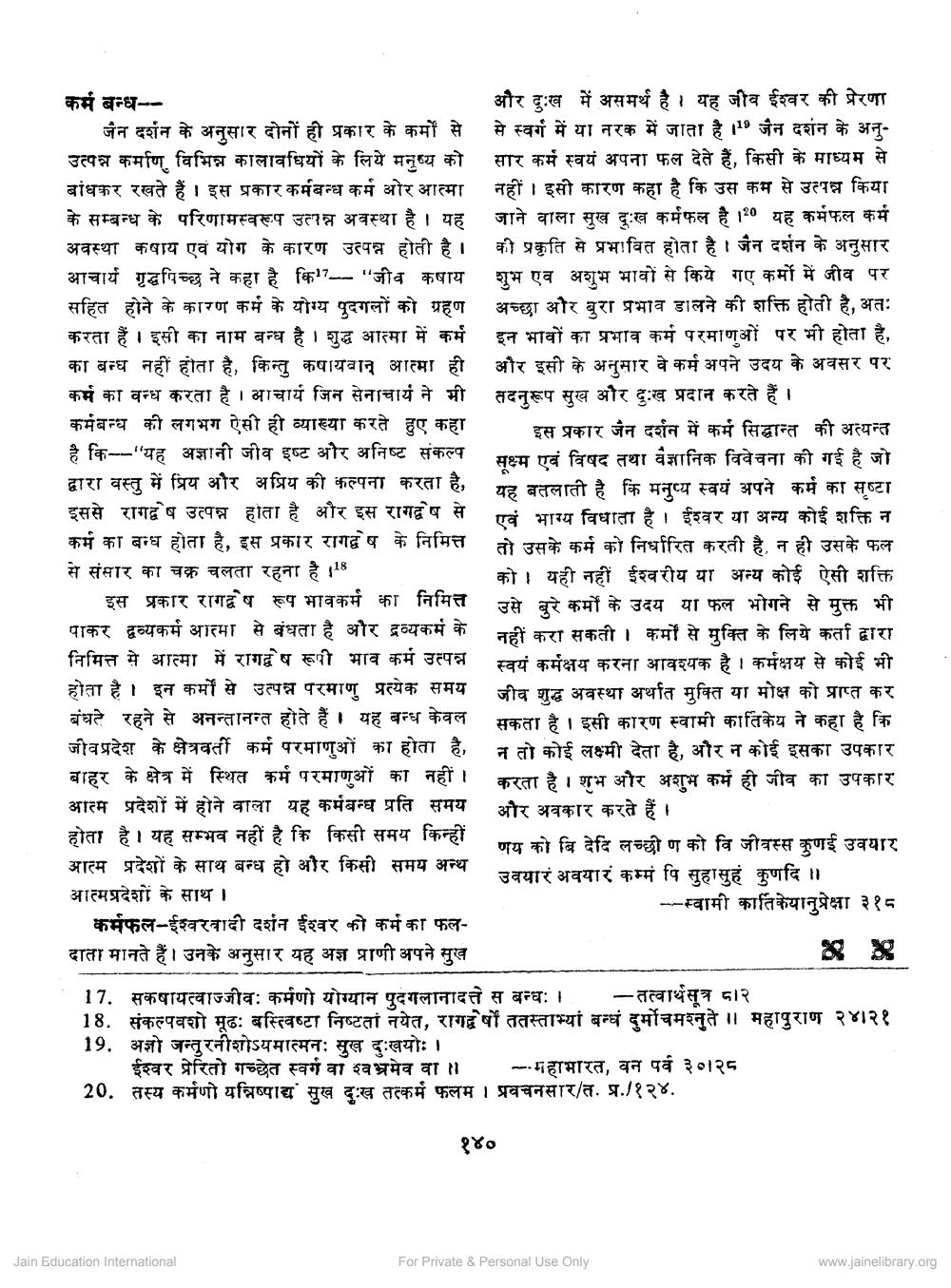________________
कर्म बन्ध-
जैन दर्शन के अनुसार दोनों ही प्रकार के कर्मों से उत्पन्न कर्माण विभिन्न कालावधियों के लिये मनुष्य को बांधकर रखते हैं। इस प्रकार कर्मबन्ध कर्म ओर आत्मा के सम्बन्ध के परिणामस्वरूप उत्पन्न अवस्था है। यह अवस्था कषाय एवं योग के कारण उत्पन्न होती है । आचार्य गृद्धपिच्छ ने कहा है कि "-- "जीव कषाय सहित होने के कारण कर्म के योग्य पुदगलों को ग्रहण करता हैं । इसी का नाम बन्ध है। शुद्ध आत्मा में कर्म का बन्ध नहीं होता है, किन्तु कषायवान् आत्मा ही कर्म का वन्ध करता है। आचार्य जिन सेनाचार्य ने भी कर्मबन्ध की लगभग ऐसी ही व्याख्या करते हुए कहा है कि- "यह अज्ञानी जीव इष्ट और अनिष्ट संकल्प द्वारा वस्तु में प्रिय और अप्रिय की कल्पना करता है, इससे रागद्वेष उत्पन्न होता है और इस रागद्वेष से कर्म का बन्ध होता है, इस प्रकार रागद्वेष के निमित्त से संसार का चक्र चलता रहना है।"
इस प्रकार रागद्व ेष रूप भावकर्म का निमित्त पाकर यकर्म आरमा से बंधता है और द्रव्यकर्म के निमित्त से आत्मा में रागद्वेष रूपी भाव कर्म उत्पन्न होता है । इन कर्मों से उत्पन्न परमाणु प्रत्येक समय बंचते रहने से अनन्तानन्त होते हैं। यह बन्ध केवल जीवप्रदेश के क्षेत्रवर्ती कर्म परमाणुओं का होता है, बाहर के क्षेत्र में स्थित कर्म परमाणुओं का नहीं । आत्म प्रदेशों में होने वाला यह कर्मबन्ध प्रति समय होता है। यह सम्भव नहीं है कि किसी समय किन्हीं आत्म प्रदेशों के साथ बन्ध हो और किसी समय अन्य आत्मप्रदेशों के साथ
कर्मफल- ईश्वरवादी दर्शन ईश्वर को कर्म का फलदाता मानते हैं। उनके अनुसार यह अज्ञ प्राणी अपने सुख
Jain Education International
और दुःख में असमर्थ है। यह जीव ईश्वर की प्रेरणा से स्वर्ग में या नरक में जाता है ।" जैन दर्शन के अनुसार कर्म स्वयं अपना फल देते हैं, किसी के माध्यम से नहीं । इसी कारण कहा है कि उस कम से उत्पन्न किया जाने वाला सुख दुःख कर्मफल है 120 यह कर्मफल कर्म की प्रकृति से प्रभावित होता है। जैन दर्शन के अनुसार शुभ एव अशुभ भावों से किये गए कर्मों में जीव पर अच्छा और बुरा प्रभाव डालने की शक्ति होती है, अतः इन भावों का प्रभाव कर्म परमाणुओं पर भी होता है, और इसी के अनुसार वे कर्म अपने उदय के अवसर पर तदनुरूप सुख और दुःख प्रदान करते हैं।
*
इस प्रकार जैन दर्शन में कर्म सिद्धान्त की अत्यन्त सूक्ष्म एवं विषद तथा वैज्ञानिक विवेचना की गई है जो यह बतलाती है कि मनुष्य स्वयं अपने कर्म का सुष्टा एवं भाग्य विधाता है। ईश्वर या अन्य कोई शक्ति न तो उसके कर्म को निर्धारित करती है, न ही उसके फल को। यही नहीं ईश्वरीय या अन्य कोई ऐसी शक्ति उसे बुरे कर्मों के उदय या फल भोगने से मुक्त भी नहीं करा सकती । कर्मों से मुक्ति के लिये कर्ता द्वारा स्वयं कर्मक्षय करना आवश्यक है । कर्मक्षय से कोई भी जीव शुद्ध अवस्था अर्थात मुक्ति या मोक्ष को प्राप्त कर सकता है । इसी कारण स्वामी कार्तिकेय ने कहा है कि न तो कोई लक्ष्मी देता है, और न कोई इसका उपकार करता है। शुभ और अशुभ कर्म ही जीव का उपकार और अवकार करते हैं ।
- तत्वार्थ सूत्र ८२
17. सकषायत्वाज्जीवः कर्मणो योग्यान पुदगलानादत्ते स बन्धः । 18. संकल्पयशो मूढः बस्त्विष्टा निष्टतां नयेत, रागद्वेष ततस्ताभ्यां बन्धं दुर्मोचमश्नुते । महापुराण २४।२१ 19. अज्ञो जन्तुरनीशोऽयमात्मनः सुख दुःखयोः ।
ईश्वर प्रेरितो गच्छेत स्वर्ग वा वमेव वा ॥ 20 तस्य कर्मणो यन्निष्याद्य सुख दुःख तत्कर्म फलम
णय को बि देदि लच्छी ण को वि जीवस्स कुणई उवयार उदयारं अववारं कम्म पि सुहासुहं कुणदि ॥ - स्वामी कार्तिकेयानुप्रेक्षा ३१८
x x
- महाभारत, वन पर्व ३०१२८ प्रवचनसार / स. प्र. / १२४.
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org