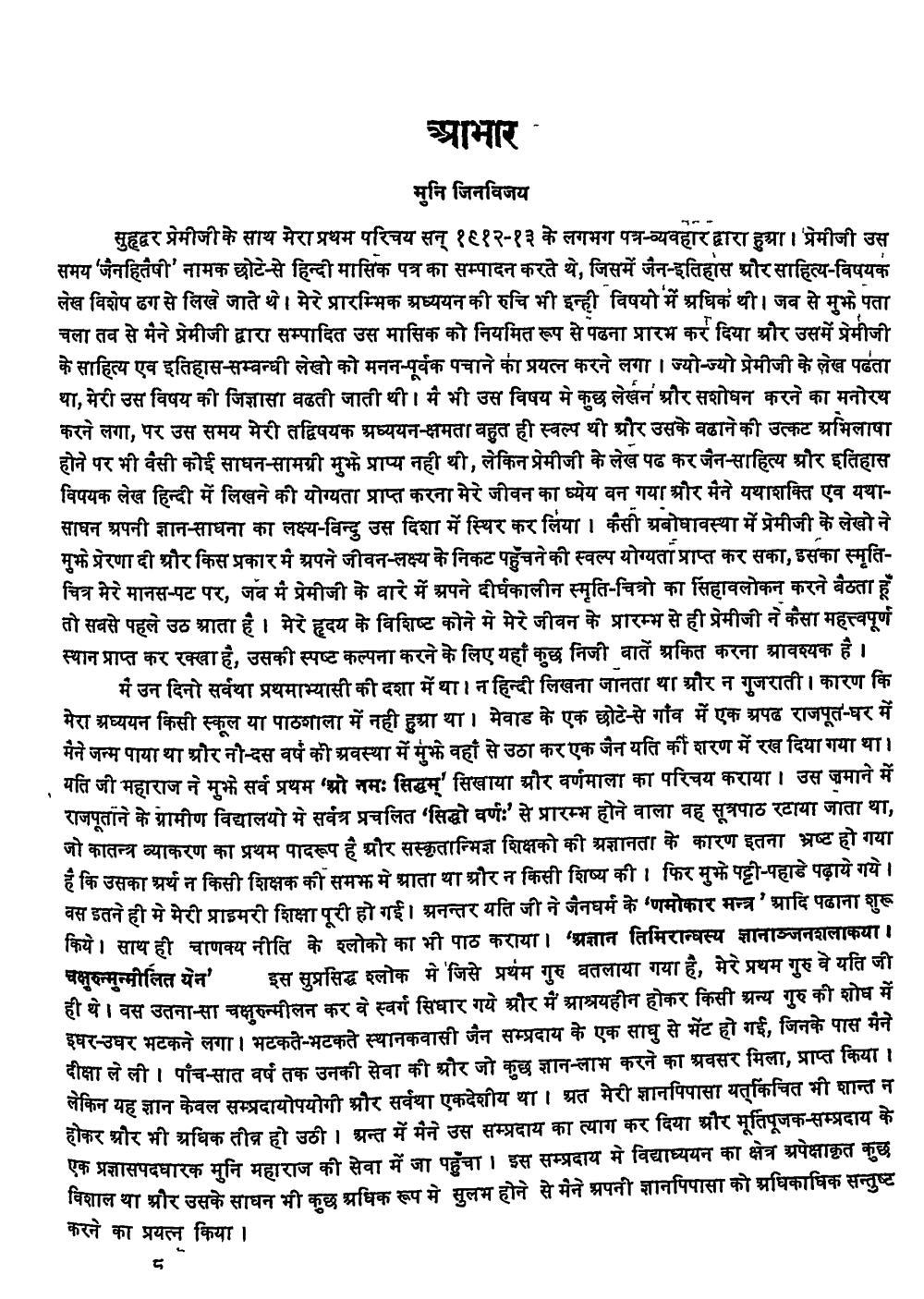________________
आभार
मुनि जिनविजय सुहृद्वर प्रेमीजी के साथ मेरा प्रथम परिचय सन् १९१२-१३ के लगभग पत्र-व्यवहार द्वारा हुआ। प्रेमीजी उस समय 'जनहितैषी' नामक छोटे-से हिन्दी मासिक पत्र का सम्पादन करते थे, जिसमें जैन-इतिहास और साहित्य-विषयक लेख विशेष ढग से लिखे जाते थे। मेरे प्रारम्भिक अध्ययन की रुचि भी इन्ही विषयो में अधिक थी। जव से मुझे पता चला तव से मैने प्रेमीजी द्वारा सम्पादित उस मासिक को नियमित रूप से पढना प्रारभ कर दिया और उसमें प्रेमीजी के साहित्य एव इतिहास-सम्बन्धी लेखो को मनन-पूर्वक पचाने का प्रयत्न करने लगा । ज्यो-ज्यो प्रेमीजी के लेख पढता था, मेरी उस विषय की जिज्ञासा वढती जाती थी। मै भी उस विषय मे कुछ लेखन और सशोधन करने का मनोरथ करने लगा, पर उस समय मेरी तद्विषयक अध्ययन-क्षमता बहुत ही स्वल्प थी और उसके बढाने की उत्कट अभिलाषा होने पर भी वैसी कोई साधन-सामग्री मुझे प्राप्य नही थी, लेकिन प्रेमीजी के लेख पढ कर जैन-साहित्य और इतिहास विषयक लेख हिन्दी में लिखने की योग्यता प्राप्त करना मेरे जीवन का ध्येय बन गया और मैने यथाशक्ति एव यथासाधन अपनी ज्ञान-साधना का लक्ष्य-विन्दु उस दिशा में स्थिर कर लिया। कसी अबोधावस्था में प्रेमीजी के लेखो ने मुझे प्रेरणा दी और किस प्रकार मै अपने जीवन-लक्ष्य के निकट पहुंचने की स्वल्प योग्यता प्राप्त कर सका, इसका स्मृतिचित्र मेरे मानस-पट पर, जब मै प्रेमीजी के बारे में अपने दीर्घकालीन स्मृति-चित्रो का सिंहावलोकन करने बैठता हूँ तो सबसे पहले उठ पाता है। मेरे हृदय के विशिष्ट कोने मे मेरे जीवन के प्रारम्भ से ही प्रेमीजी ने कैसा महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर रक्खा है, उसकी स्पष्ट कल्पना करने के लिए यहां कुछ निजी बातें अकित करना आवश्यक है।
मैं उन दिनो सर्वथा प्रथमाभ्यासी की दशा में था। न हिन्दी लिखना जानता था और न गुजराती। कारण कि मेरा अध्ययन किसी स्कूल या पाठशाला में नही हुआ था। मेवाड के एक छोटे से गांव में एक अपढ राजपूत-घर में मैने जन्म पाया था और नी-दस वर्ष की अवस्था में मुझे वहां से उठा कर एक जैन यति की शरण में रख दिया गया था। , यति जी महाराज ने मुझे सर्व प्रथम 'प्रो नमः सिद्धम् सिखाया और वर्णमाला का परिचय कराया। उस जमाने में
राजपूताने के ग्रामीण विद्यालयो मे सर्वत्र प्रचलित 'सिद्धो वर्णः' से प्रारम्भ होने वाला वह सूत्रपाठ रटाया जाता था, जो कातन्त्र व्याकरण का प्रथम पादरूप है और सस्कृतान्मिज्ञ शिक्षको की अज्ञानता के कारण इतना भ्रष्ट हो गया है कि उसका अर्थ न किसी शिक्षक की समझ मे आता था और न किसी शिष्य की। फिर मुझे पट्टी-पहाडे पढ़ाये गये। बस इतने ही मे मेरी प्राइमरी शिक्षा पूरी हो गई। अनन्तर यति जी ने जैनधर्म के 'णमोकार मन्त्र' आदि पढाना शुरू किये। साथ ही चाणक्य नीति के श्लोको का भी पाठ कराया। 'प्रज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया। चक्षुरुन्मुन्मीलित येन' इस सुप्रसिद्ध श्लोक मे 'जिसे प्रथम गुरु बतलाया गया है, मेरे प्रथम गुरु वे यति जी ही थे। वस उतना-सा चक्षुरुन्मीलन कर वे स्वर्ग सिधार गये और मैं आश्रयहीन होकर किसी अन्य गुरु की शोध में इधर-उधर भटकने लगा। भटकते-भटकते स्थानकवासी जैन सम्प्रदाय के एक साधु से भेंट हो गई, जिनके पास मैने दक्षिा ले ली। पांच-सात वर्ष तक उनकी सेवा की और जो कुछ ज्ञान-लाभ करने का अवसर मिला, प्राप्त किया। लेकिन यह ज्ञान केवल सम्प्रदायोपयोगी और सर्वथा एकदेशीय था। अत मेरी ज्ञानपिपासा यत्किंचित भी शान्त न होकर और भी अधिक तीव्र हो उठी। अन्त में मैने उस सम्प्रदाय का त्याग कर दिया और मूर्तिपूजक-सम्प्रदाय के एक प्रज्ञासपदधारक मुनि महाराज की सेवा में जा पहुंचा। इस सम्प्रदाय मे विद्याध्ययन का क्षेत्र अपेक्षाकृत कुछ विशाल था और उसके साधन भी कुछ अधिक रूप मे सुलभ होने से मैने अपनी ज्ञानपिपासा को अधिकाधिक सन्तुष्ट करने का प्रयत्न किया।