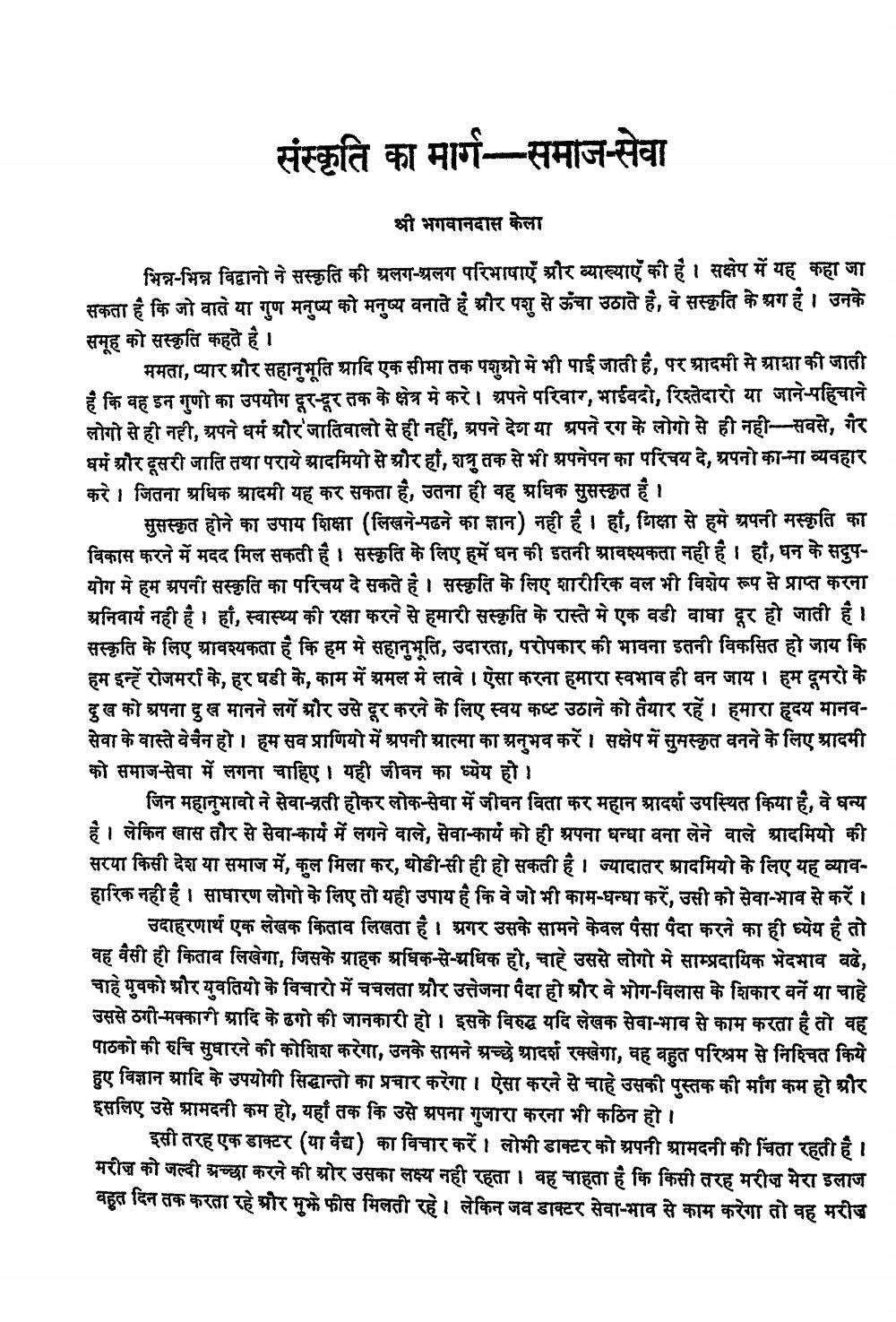________________
संस्कृति का मार्ग-समाज-सेवा
श्री भगवानदास केला भिन्न-भिन्न विद्वानो ने सस्कृति की अलग-अलग परिभाषाएँ और व्याख्याएँ की है। सक्षेप में यह कहा जा सकता है कि जो वाते या गुण मनुष्य को मनुष्य वनाते हैं और पशु से ऊंचा उठाते है, वे सस्कृति के अग है। उनके समूह को सस्कृति कहते है।
ममता, प्यार और सहानुभूति प्रादि एक सीमा तक पशुप्रो मे भी पाई जाती है, पर प्रादमी मे प्राशा की जाती है कि वह इन गुणो का उपयोग दूर-दूर तक के क्षेत्र में करे। अपने परिवार, भाईवदो, रिश्तेदारी या जाने पहिचाने लोगो से ही नहीं, अपने धर्म और जातिवालो से ही नहीं, अपने देश या अपने रग के लोगो से ही नही-सवसे, गैर धर्म और दूसरी जाति तथा पराये आदमियो से और हां, शत्रु तक से भी अपनेपन का परिचय दे, अपनो का-ना व्यवहार करे। जितना अधिक आदमी यह कर सकता है, उतना ही वह अधिक सुसस्कृत है।
सुसस्कृत होने का उपाय शिक्षा (लिखने-पढने का ज्ञान) नही है । हां, शिक्षा से हमे अपनी मस्कृति का विकास करने में मदद मिल सकती है। सस्कृति के लिए हमें धन की इतनी आवश्यकता नहीं है। हां, धन के सदुपयोग मे हम अपनी संस्कृति का परिचय दे सकते है । सस्कृति के लिए शारीरिक वल भी विशेप रूप से प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है। हां, स्वास्थ्य की रक्षा करने से हमारी सस्कृति के रास्ते मे एक वडी बाधा दूर हो जाती है। सस्कृति के लिए आवश्यकता है कि हम मे सहानुभूति, उदारता, परोपकार की भावना इतनी विकसित हो जाय कि हम इन्हें रोजमर्रा के, हर घडी के, काम में अमल में लावे । ऐसा करना हमारा स्वभाव ही वन जाय । हम दूसरो के दुख को अपना दुख मानने लगें और उसे दूर करने के लिए स्वय कष्ट उठाने को तैयार रहें। हमारा हृदय मानवसेवा के वास्ते वेचैन हो। हम सव प्राणियो में अपनी आत्मा का अनुभव करें। सक्षेप में सुमस्कृत बनने के लिए आदमी को समाज-सेवा में लगना चाहिए। यही जीवन का ध्येय हो।
जिन महानुभावो ने सेवा-वती होकर लोक सेवा में जीवन विता कर महान आदर्श उपस्थित किया है, वे धन्य है। लेकिन खास तौर से सेवा-कार्य में लगने वाले, सेवा-कार्य को ही अपना धन्धा बना लेने वाले आदमियो की सरया किसी देश या समाज में, कुल मिला कर, थोडी-सी ही हो सकती है। ज्यादातर आदमियो के लिए यह व्यावहारिक नही है । साधारण लोगो के लिए तो यही उपाय है कि वे जो भी काम-धन्धा करें, उसी को सेवा-भाव से करें।
___ उदाहरणार्थ एक लेखक किताब लिखता है। अगर उसके सामने केवल पैसा पैदा करने का ही ध्येय है तो वह वैसी ही किताव लिखेगा, जिसके ग्राहक अधिक-से-अधिक हो, चाहे उससे लोगो में साम्प्रदायिक भेदभाव बढे, चाहे युवको और युवतियो के विचारो में चचलता और उत्तेजना पैदा हो और वे भोग-विलास के शिकार बनें या चाहे उससे ठगी-मक्कारी आदि के ढगो की जानकारी हो। इसके विरुद्ध यदि लेखक सेवा-भाव से काम करता है तो वह पाठको की रुचि सुधारने की कोशिश करेगा, उनके सामने अच्छे आदर्श रक्खेगा, वह बहुत परिश्रम से निश्चित किये हुए विज्ञान आदि के उपयोगी सिद्धान्तो का प्रचार करेगा। ऐसा करने से चाहे उसकी पुस्तक की मांग कम हो और इसलिए उसे आमदनी कम हो, यहाँ तक कि उसे अपना गुजारा करना भी कठिन हो।
इसी तरह एक डाक्टर (या वैद्य) का विचार करें। लोभी डाक्टर को अपनी आमदनी की चिंता रहती है । मरीज़ को जल्दी अच्छा करने की और उसका लक्ष्य नही रहता। वह चाहता है कि किसी तरह मरीज़ मेरा इलाज बहुत दिन तक करता रहे और मुझे फीस मिलती रहे। लेकिन जब डाक्टर सेवा-भाव से काम करेगा तो वह मरीज