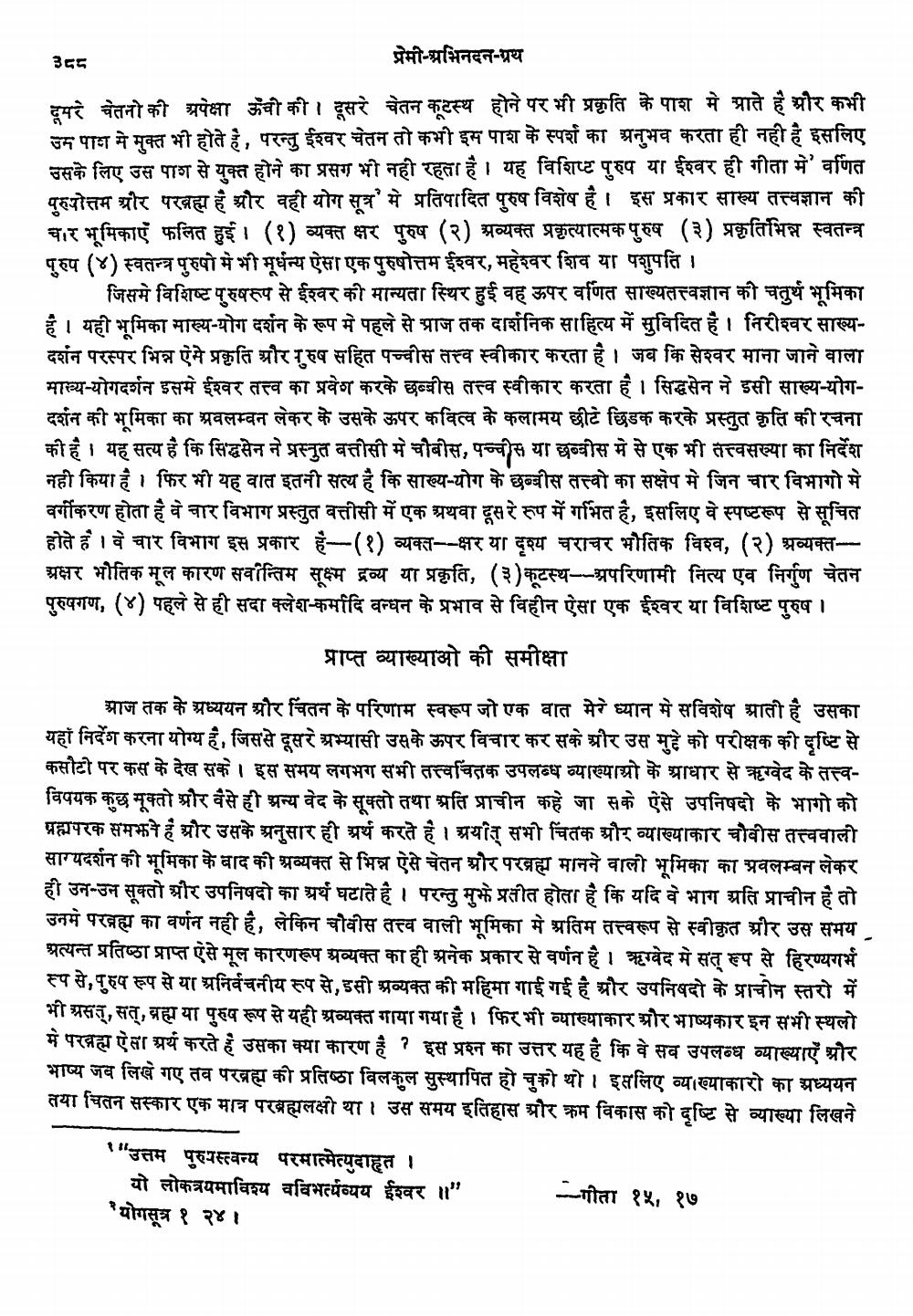________________
३८८
प्रेमी-अभिनदन-प्रथ
दूसरे चेतनो की अपेक्षा ऊंची की। दूसरे चेतन कूटस्थ होने पर भी प्रकृति के पाश मे आते है और कभी जम पाश मे मुक्त भी होते है, परन्तु ईश्वर चेतन तो कभी इस पाश के स्पर्श का अनुभव करता ही नहीं है इसलिए उसके लिए उस पाश से युक्त होने का प्रसग भी नही रहता है। यह विशिष्ट पुरुष या ईश्वर ही गीता में वर्णित पुरुषोत्तम और परब्रह्म है और वही योग सूत्र' मे प्रतिपादित पुरुष विशेष है। इस प्रकार साख्य तत्त्वज्ञान की चार भूमिकाएं फलित हुई। (१) व्यक्त क्षर पुरुष (२) अव्यक्त प्रकृत्यात्मक पुरुष (३) प्रकृतिभिन्न स्वतन्त्र पुरुष (४) स्वतन्त्र पुरुषो मे भी मूर्धन्य ऐसा एक पुरुषोत्तम ईश्वर, महेश्वर शिव या पशुपति ।
जिसमे विशिष्ट पुरुषरूप से ईश्वर की मान्यता स्थिर हुई वह ऊपर वर्णित साख्यतत्त्वज्ञान की चतुर्थ भूमिका है । यही भूमिका माख्य-योग दर्शन के रूप में पहले से आज तक दार्शनिक साहित्य में सुविदित है। निरीश्वर साख्यदर्शन परस्पर भिन्न ऐमे प्रकृति और पुरुष सहित पच्चीस तत्त्व स्वीकार करता है । जब कि सेश्वर माना जाने वाला मान्य-योगदर्शन इसमे ईश्वर तत्त्व का प्रवेश करके छब्बीस तत्त्व स्वीकार करता है । सिद्धसेन ने इसी साख्य-योगदर्शन की भूमिका का अवलम्बन लेकर के उसके ऊपर कवित्व के कलामय छीटे छिडक करके प्रस्तुत कृति की रचना की है। यह सत्य है कि सिद्धसेन ने प्रस्तुत बत्तीसी मे चौबीस, पच्चीस या छब्बीस मे से एक भी तत्त्वसख्या का निर्देश नही किया है। फिर भी यह वात इतनी सत्य है कि साख्य-योग के छब्बीस तत्त्वो का सक्षेप मे जिन चार विभागो में वर्गीकरण होता है वे चार विभाग प्रस्तुत बत्तीसी में एक अथवा दूसरे रूप में गर्भित है, इसलिए वे स्पष्टरूप से सूचित होते है । वे चार विभाग इस प्रकार है-(१) व्यक्त-क्षर या दृश्य चराचर भौतिक विश्व, (२) अव्यक्तअक्षर भौतिक मूल कारण सर्वान्तिम सूक्ष्म द्रव्य या प्रकृति, (३) कूटस्थ--अपरिणामी नित्य एव निर्गुण चेतन पुरुषगण, (४) पहले से ही सदा क्लेश-कर्मादि वन्धन के प्रभाव से विहीन ऐसा एक ईश्वर या विशिष्ट पुरुष ।
प्राप्त व्याख्याओ की समीक्षा
आज तक के अध्ययन और चिंतन के परिणाम स्वरूप जो एक बात मेरे ध्यान मे सविशेष आती है उसका यहाँ निर्देश करना योग्य है, जिससे दूसरे अभ्यासी उसके ऊपर विचार कर सके और उस मुद्दे को परीक्षक की दृष्टि से कसौटी पर कस के देख सके। इस समय लगभग सभी तत्त्वचिंतक उपलब्ध व्याख्यानो के आधार से ऋग्वेद के तत्त्वविषयक कुछ मूक्तो और वैसे ही अन्य वेद के सूक्तो तथा अति प्राचीन कहे जा सके ऐसे उपनिषदो के भागो को प्रह्मपरक समझते है और उसके अनुसार ही अर्थ करते है । अयात् सभी चिंतक और व्याख्याकार चौवीस तत्त्ववाली साग्यदर्शन की भूमिका के बाद की अव्यक्त से भिन्न ऐसे चेतन और परब्रह्म मानने वाली भूमिका का अवलम्बन लेकर ही उन-उन सूक्तो और उपनिषदो का अर्थ घटाते है । परन्तु मुझे प्रतीत होता है कि यदि वे भाग अति प्राचीन है तो उनमे परब्रह्म का वर्णन नही है, लेकिन चोवीस तत्त्व वाली भूमिका मे अतिम तत्त्वरूप से स्वीकृत और उस समय, अत्यन्त प्रतिष्ठा प्राप्त ऐसे मूल कारणरूप अव्यक्त का ही अनेक प्रकार से वर्णन है । ऋग्वेद में सत् रूप से हिरण्यगर्भ स्प से,पुरुष रूप से या अनिर्वचनीय रूप से, इसी अव्यक्त की महिमा गाई गई है और उपनिषदो के प्राचीन स्तरो में भी असत्, सत्, ब्रह्म या पुरुष रूप से यही अव्यक्त गाया गया है। फिर भी व्याख्याकार और भाष्यकार इन सभी स्थलो मे परब्रह्म ऐसा अर्थ करते है उसका क्या कारण है ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि वे सब उपलब्ध व्याख्याएँ और भाष्य जव लिखे गए तव परब्रह्म को प्रतिष्ठा विलकुल सुस्थापित हो चुकी थी। इसलिए व्याख्याकारो का अध्ययन तया चितन सस्कार एक मात्र परब्रह्मलक्षी था। उस समय इतिहास और क्रम विकास को दृष्टि से व्याख्या लिखने
""उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहृत । __ यो लोकत्रयमाविश्य वविभर्त्यव्यय ईश्वर ॥" 'योगसूत्र १ २४।
गीता १५, १७