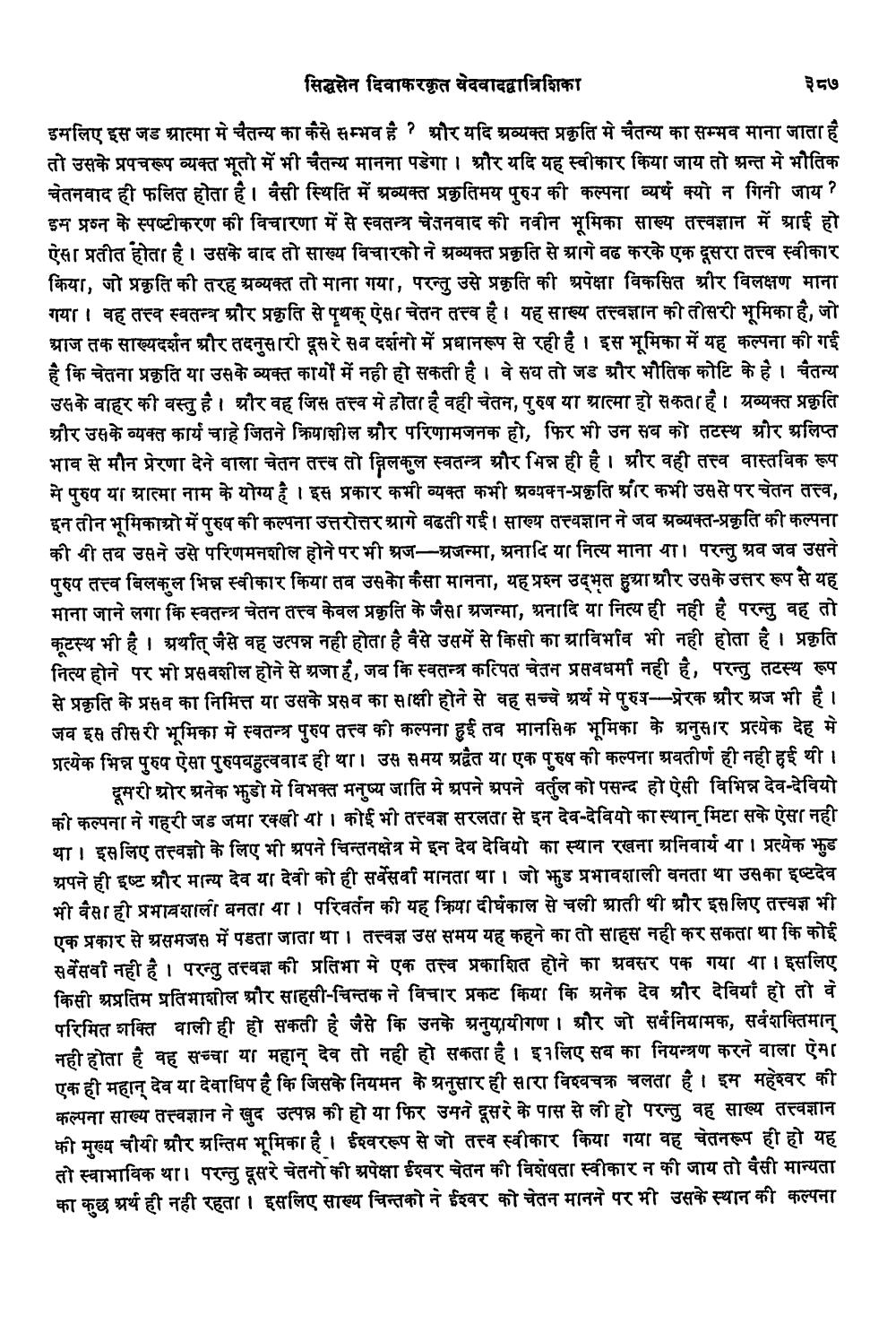________________
सिद्धसेन दिवाकरकृत वेववादद्वात्रिशिका
३८७
इमलिए इस जड प्रात्मा मे चैतन्य का कैसे सम्भव है ? और यदि अव्यक्त प्रकृति मे चैतन्य का सम्भव माना जाता है तो उसके प्रपचरूप व्यक्त भूतो में भी चैतन्य मानना पडेगा । और यदि यह स्वीकार किया जाय तो अन्त मे भौतिक चेतनवाद ही फलित होता है। वैसी स्थिति में अव्यक्त प्रकृतिमय पुरुष की कल्पना व्यर्थ क्यो न गिनी जाय? इम प्रश्न के स्पष्टीकरण की विचारणा में से स्वतन्त्र चेतनवाद को नवीन भूमिका साख्य तत्त्वज्ञान में आई हो ऐसा प्रतीत होता है। उसके बाद तो साख्य विचारको ने अव्यक्त प्रकृति से आगे बढ करके एक दूसरा तत्त्व स्वीकार किया, जो प्रकृति की तरह अव्यक्त तो माना गया, परन्तु उसे प्रकृति की अपेक्षा विकसित और विलक्षण माना गया। वह तत्त्व स्वतन्त्र और प्रकृति से पृथक् ऐसा चेतन तत्त्व है। यह साख्य तत्त्वज्ञान की तीसरी भूमिका है, जो आज तक साख्यदर्शन और तदनुसारो दूसरे सव दर्शनो में प्रधानरूप से रही है । इस भूमिका में यह कल्पना की गई है कि चेतना प्रकृति या उसके व्यक्त कार्यों में नही हो सकती है। वे सब तो जड और भौतिक कोटि के है। चैतन्य उसके बाहर की वस्तु है। और वह जिस तत्त्व मे होता है वही चेतन, पुरुष या प्रात्मा हो सकता है। अव्यक्त प्रकृति और उसके व्यक्त कार्य चाहे जितने क्रियाशील और परिणामजनक हो, फिर भी उन सब को तटस्थ और अलिप्त भाव से मौन प्रेरणा देने वाला चेतन तत्त्व तो विलकुल स्वतन्त्र और भिन्न ही है । और वही तत्त्व वास्तविक रूप मे पुरुप या आत्मा नाम के योग्य है । इस प्रकार कभी व्यक्त कभी अव्यक्त-प्रकृति और कभी उससे पर चेतन तत्व, इन तीन भूमिकामो में पुरुष की कल्पना उत्तरोत्तर आगे बढती गई। साख्य तत्त्वज्ञान ने जव अव्यक्त-प्रकृति की कल्पना की यो तब उसने उसे परिणमनशील होने पर भी अज-अजन्मा, अनादि या नित्य माना या। परन्तु अव जव उसने पुरुप तत्त्व बिलकुल भिन्न स्वीकार किया तब उसको कैसा मानना, यह प्रश्न उद्भत हया और उसके उत्तर रूप से यह माना जाने लगा कि स्वतन्त्र चेतन तत्त्व केवल प्रकृति के जैसा अजन्मा, अनादि या नित्य ही नही है परन्तु वह तो कूटस्थ भी है । अर्थात् जैसे वह उत्पन्न नहीं होता है वैसे उसमें से किसी का आविर्भाव भी नही होता है। प्रकृति नित्य होने पर भी प्रसवशील होने से अजा है, जब कि स्वतन्त्र कल्पित चेतन प्रसवधर्मा नही है, परन्तु तटस्थ रूप से प्रकृति के प्रसव का निमित्त या उसके प्रसव का साक्षी होने से वह सच्चे अर्थ मे पुरुष-प्रेरक और अज भी है। जव इस तीसरी भूमिका मे स्वतन्त्र पुरुप तत्त्व की कल्पना हुई तब मानसिक भूमिका के अनुसार प्रत्येक देह में प्रत्येक भिन्न पुरुष ऐसा पुरुपवहुत्ववाद ही था। उस समय अद्वैत या एक पुरुष की कल्पना अवतीर्ण ही नही हुई थी।
दूसरी ओर अनेक झुडो मे विभक्त मनुष्य जाति मे अपने अपने वर्तुल को पसन्द हो ऐसी विभिन्न देव-देवियो को कल्पना ने गहरी जड जमा रक्खी यो। कोई भी तत्त्वज्ञ सरलता से इन देव-देवियो का स्थान मिटा सके ऐसा नही था। इसलिए तत्त्वज्ञो के लिए भी अपने चिन्तनक्षेत्र में इन देव देवियो का स्थान रखना अनिवार्य या । प्रत्येक झुड अपने ही इष्ट और मान्य देव या देवी को ही सर्वेसर्वा मानता था। जो झुड प्रभावशाली वनता था उसका इष्टदेव भी वैसा ही प्रभावशाली बनता था। परिवर्तन की यह क्रिया दीर्घकाल से चली आती थी और इस लिए तत्त्वज्ञ भी एक प्रकार से असमजस में पडता जाता था। तत्त्वज्ञ उस समय यह कहने का तो साहस नही कर सकता था कि कोई सर्वेसर्वा नही है । परन्तु तत्त्वज्ञ की प्रतिभा मे एक तत्त्व प्रकाशित होने का अवसर पक गया था। इसलिए किसी अप्रतिम प्रतिभाशील और साहसी-चिन्तक ने विचार प्रकट किया कि अनेक देव और देवियाँ हो तो वे परिमित शक्ति वाली ही हो सकती है जैसे कि उनके अनुयायीगण । और जो सर्वनियामक, सर्वशक्तिमान् नही होता है वह सच्चा या महान् देव तो नही हो सकता है। इसलिए सब का नियन्त्रण करने वाला ऐमा एक ही महान् देव या देवाधिप है कि जिसके नियमन के अनुसार ही सारा विश्वचक्र चलता है। इम महेश्वर की कल्पना साख्य तत्त्वज्ञान ने खुद उत्पन्न की हो या फिर उमने दूसरे के पास से ली हो परन्तु वह साख्य तत्त्वज्ञान की मुख्य चीयो और अन्तिम भूमिका है । ईश्वररूप से जो तत्त्व स्वीकार किया गया वह चेतनरूप ही हो यह तो स्वाभाविक था। परन्तु दूसरे चेतनो की अपेक्षा ईश्वर चेतन की विशेषता स्वीकार न की जाय तो वैसी मान्यता का कछ अर्थ ही नही रहता। इसलिए साख्य चिन्तको ने ईश्वर को चेतन मानने पर भी उसके स्थान की कल्पना