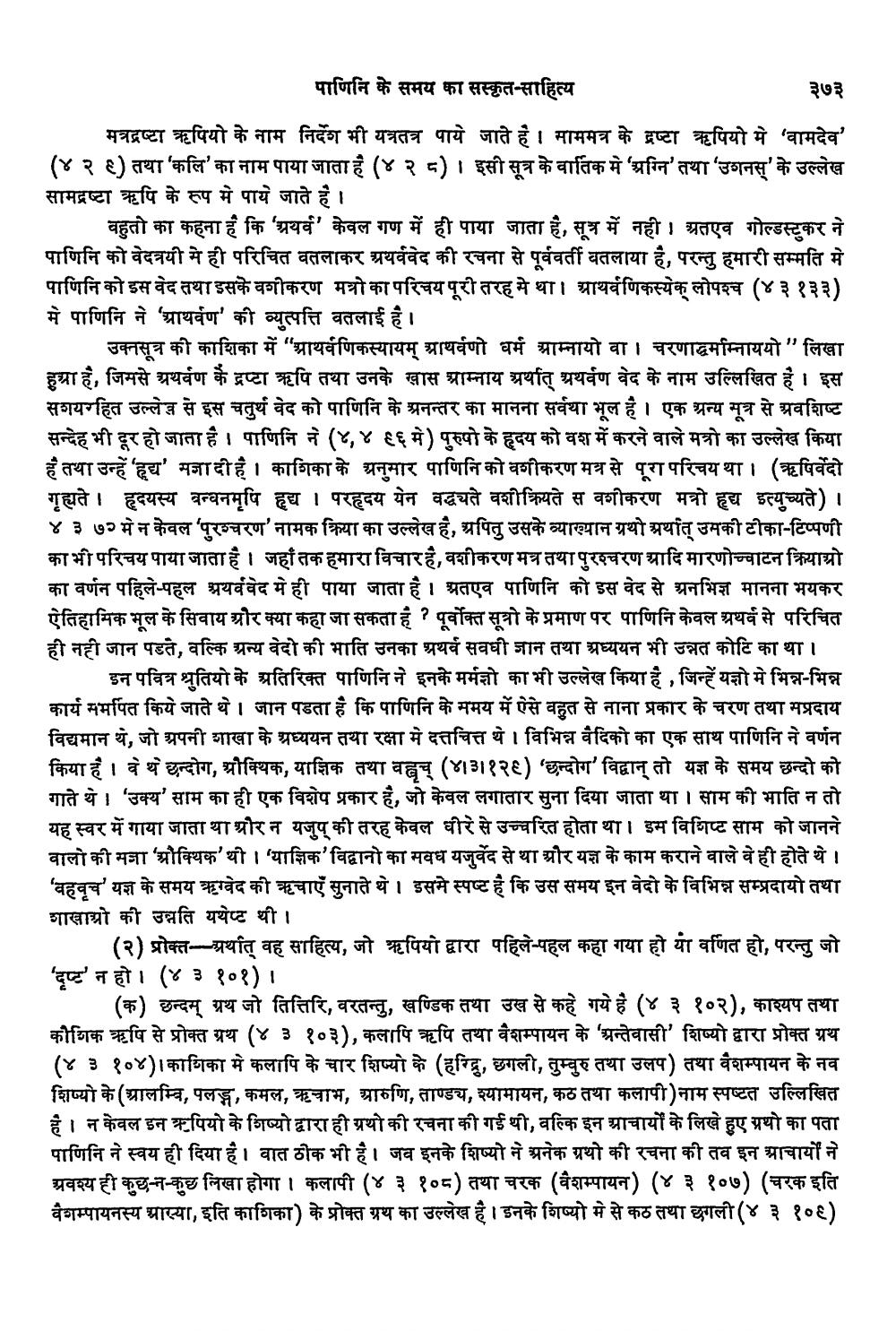________________
पाणिनि के समय का सस्कृत-साहित्य
३७३
मत्रद्रष्टा ऋषियो के नाम निर्देश भी यत्रतत्र पाये जाते है। माममत्र के द्रष्टा ऋषियो मे 'वामदेव' (४२ ६) तथा 'कलि' का नाम पाया जाता है (४ २८)। इसी सूत्र के वार्तिक मे 'अग्नि' तथा 'उगनस्' के उल्लेख सामद्रष्टा ऋपि के रूप में पाये जाते है।
वहुतो का कहना है कि 'अथर्व' केवल गण में ही पाया जाता है, सूत्र में नहीं। अतएव गोल्डस्टुकर ने पाणिनि को वेदत्रयी मे ही परिचित बतलाकर अथर्ववेद की रचना से पूर्ववर्ती बतलाया है, परन्तु हमारी सम्मति मे पाणिनि को इस वेद तथा इसके वशीकरण मत्रो का परिचय पूरी तरह मे था। आथर्वणिकस्येक् लोपश्च (४ ३ १३३) मे पाणिनि ने 'आथर्वण' की व्युत्पत्ति वतलाई है।
__ उक्तसूत्र की काशिका में "आथर्वणिकस्यायम् पाथर्वणो धर्म आम्नायो वा। चरणाद्धर्माम्नाययो" लिखा हुया है, जिससे अथर्वण के द्रप्टा ऋषि तथा उनके खास आम्नाय अर्थात् अथर्वण वेद के नाम उल्लिखित है। इस सगयरहित उल्लेज से इस चतुर्थ वेद को पाणिनि के अनन्तर का मानना सर्वथा भूल है। एक अन्य मूत्र से अवशिष्ट सन्देह भी दूर हो जाता है। पाणिनि ने (४,४ ६६ मे) पुरुषो के हृदय को वश में करने वाले मत्रो का उल्लेख किया है तथा उन्हें हृद्य' मजादी है । काशिका के अनुमार पाणिनि को वशीकरण मत्र से पूरा परिचय था। (ऋषिर्वेदो गृह्यते। हृदयस्य बन्वनमृषि हृद्य । परहृदय येन वद्धयते वशीक्रियते स वशीकरण मत्रो हृद्य इत्युच्यते) । ४ ३ ७२ मे न केवल पुरश्चरण' नामक क्रिया का उल्लेख है, अपितु उसके व्याख्यान ग्रथो अर्थात् उमको टीका-टिप्पणी का भी परिचय पाया जाता है । जहाँ तक हमारा विचार है, वशीकरण मत्र तथा पुरश्चरण आदि मारणोच्चाटन क्रियायो का वर्णन पहिले-पहल अथर्ववेद मे ही पाया जाता है । अतएव पाणिनि को इस वेद से अनभिज्ञ मानना भयकर ऐतिहासिक भूल के सिवाय और क्या कहा जा सकता है ? पूर्वोक्त सूत्रो के प्रमाण पर पाणिनि केवल अथर्व से परिचित ही नहीं जान पडते, बल्कि अन्य वेदो की भाति उनका अथर्व सवधी ज्ञान तथा अध्ययन भी उन्नत कोटि का था।
इन पवित्र श्रुतियो के अतिरिक्त पाणिनि ने इनके मर्मज्ञो का भी उल्लेख किया है , जिन्हें यज्ञो मे भिन्न-भिन्न कार्य ममर्पित किये जाते थे। जान पडता है कि पाणिनि के ममय में ऐसे बहुत से नाना प्रकार के चरण तथा मप्रदाय विद्यमान थे, जो अपनी शाखा के अध्ययन तथा रक्षा मे दत्तचित्त थे । विभिन्न वैदिको का एक साथ पाणिनि ने वर्णन किया है। वे थे छन्दोग, प्रोक्थिक, याज्ञिक तथा वह्वच (४।३।१२६) 'छन्दोग' विद्वान तो यज्ञ के समय छन्दो को गाते थे। 'उक्य' साम का ही एक विशेष प्रकार है, जो केवल लगातार सुना दिया जाता था। साम की भाति न तो यह स्वर में गाया जाता था और न यजुप की तरह केवल धीरे से उच्चरित होता था। इम विगिप्ट साम को जानने वालो की मना 'प्रोक्थिक' थी। 'याज्ञिक विद्वानो का मवध यजुर्वेद से था और यज्ञ के काम कराने वाले वे ही होते थे। 'वहवृच' यज्ञ के समय ऋग्वेद की ऋचाएँ सुनाते थे। इसमे स्पष्ट है कि उस समय इन वेदो के विभिन्न सम्प्रदायो तथा शाखायो की उन्नति यथेप्ट थी।
(२) प्रोक्त अर्थात् वह साहित्य, जो ऋपियो द्वारा पहिले-पहल कहा गया हो या वर्णित हो, परन्तु जो 'दृष्ट' न हो। (४ ३ १०१)।
(क) छन्दम् अथ जो तित्तिरि, वरतन्तु, खण्डिक तथा उख से कहे गये है (४ ३ १०२), काश्यप तथा कौगिक ऋषि से प्रोक्त अथ (४ ३ १०३), कलापि ऋपि तथा वैशम्पायन के 'अन्तेवासी' शिष्यो द्वारा प्रोक्त (४ ३ १०४)। काशिका मे कलापि के चार शिष्यो के (हरिद्रु, छगली, तुम्वुरु तथा उलप) तथा वैशम्पायन के नव शिष्यो के (प्रालम्बि, पलङ्ग, कमल, ऋत्राभ, आरुणि, ताण्ड्य, श्यामायन, कठ तथा कलापी)नाम स्पष्टत उल्लिखित है। न केवल इन ऋपियो के शिष्यो द्वारा ही ग्रथो की रचना की गई थी, बल्कि इन प्राचार्यों के लिखे हुए ग्रथो का पता पाणिनि ने स्वय ही दिया है। वात ठीक भी है। जव इनके शिष्यो ने अनेक ग्रथो की रचना की तव इन आचार्यों ने अवश्य ही कुछ-न-कुछ लिखा होगा। कलापी (४ ३ १०८) तथा चरक (वैशम्पायन) (४ ३ १०७) (चरक इति वैशम्पायनस्य प्रास्या, इति काशिका) के प्रोक्त ग्रथ का उल्लेख है। इनके शिष्यो मे से कठ तथा छगली (४ ३ १०६)