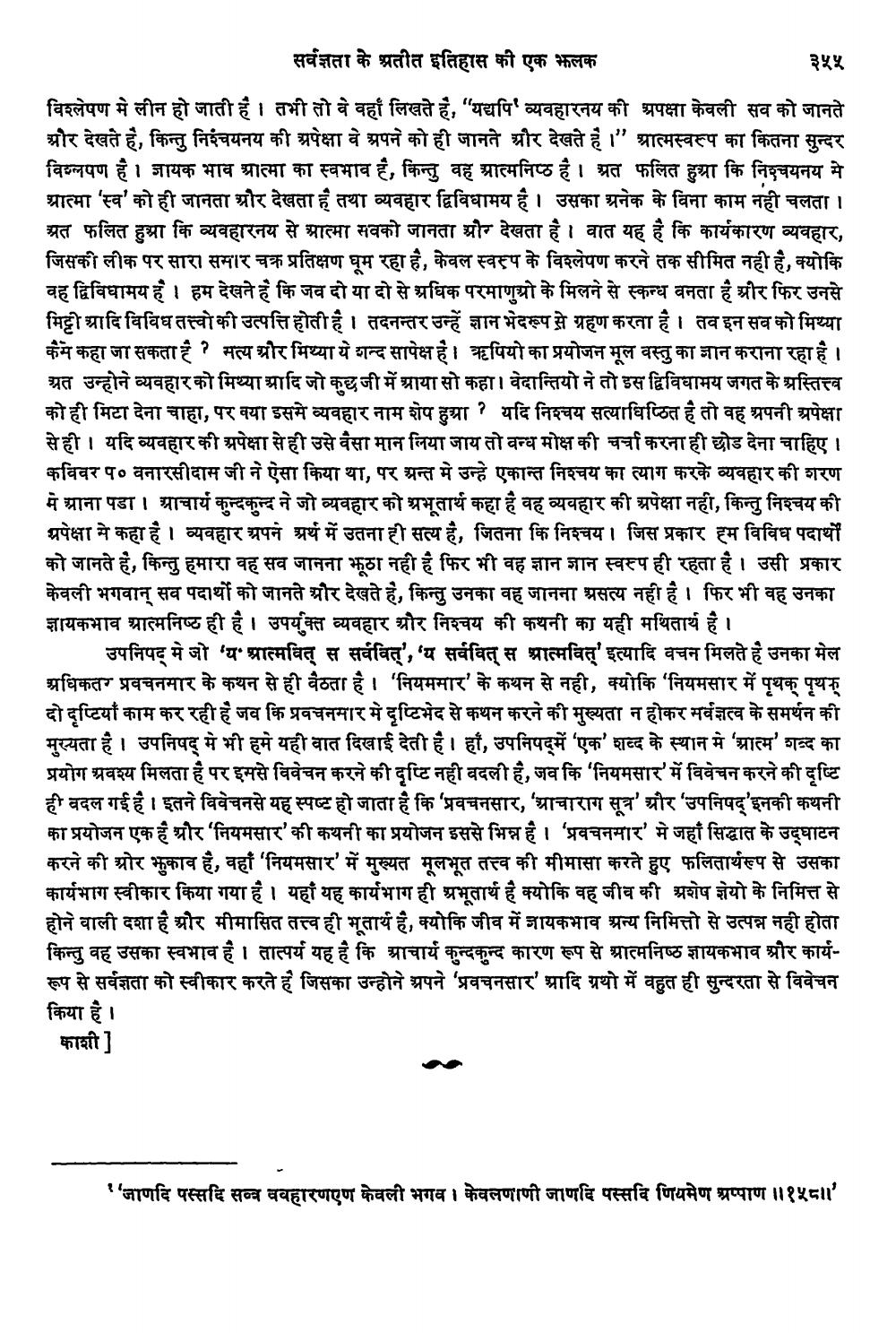________________
सर्वज्ञता के प्रतीत इतिहास की एक झलक
३५५ विश्लेषण मे लीन हो जाती है। तभी तो वे वहाँ लिखते है, "यद्यपि' व्यवहारनय की अपक्षा केवली सव को जानते
और देखते है, किन्तु निरंचयनय की अपेक्षा वे अपने को ही जानते और देखते है ।" अात्मस्वरूप का कितना सुन्दर विश्लपण है। जायक भाव आत्मा का स्वभाव है, किन्तु वह आत्मनिष्ठ है। अत फलित हुआ कि निश्चयनय मे प्रात्मा 'स्व' को ही जानता और देखता है तथा व्यवहार द्विविधामय है। उसका अनेक के विना काम नही चलता। अत फलित हुआ कि व्यवहारनय से आत्मा सवको जानता और देखता है। वात यह है कि कार्यकारण व्यवहार, जिसकी लीक पर सारा समार चक्र प्रतिक्षण घूम रहा है, केवल स्वस्प के विश्लेपण करने तक सीमित नहीं है, क्योकि वह द्विविधामय है। हम देखते हैं कि जब दो या दो से अधिक परमाणुमो के मिलने से स्कन्ध बनता है और फिर उनसे मिट्टी आदि विविध तत्त्वो की उत्पत्ति होती है। तदनन्तर उन्हें ज्ञान भेदरूप से ग्रहण करता है। तव इन सब को मिथ्या कैमे कहा जा सकता है ? मत्य और मिथ्या ये शन्द सापेक्ष है। ऋषियो का प्रयोजन मूल वस्तु का ज्ञान कराना रहा है। अत उन्होने व्यवहार को मिथ्या आदि जो कुछ जी में पाया सो कहा। वेदान्तियो ने तो इस द्विविधामय जगत के अस्तित्त्व को ही मिटा देना चाहा, पर क्या इसमे व्यवहार नाम शेप हुआ? यदि निश्चय सत्याधिष्ठित है तो वह अपनी अपेक्षा से ही। यदि व्यवहार की अपेक्षा से ही उसे वैसा मान लिया जाय तो वन्ध मोक्ष की चर्चा करना ही छोड देना चाहिए। कविवर प० वनारसीदास जी ने ऐसा किया था, पर अन्त मे उन्हे एकान्त निश्चय का त्याग करके व्यवहार की शरण मे आना पडा। प्राचार्य कुन्दकुन्द ने जो व्यवहार को अभूतार्थ कहा है वह व्यवहार की अपेक्षा नहीं, किन्तु निश्चय की अपेक्षा से कहा है। व्यवहार अपने अर्थ में उतना ही सत्य है, जितना कि निश्चय। जिस प्रकार हम विविध पदार्थों को जानते हैं, किन्तु हमारा वह सव जानना झूठा नहीं है फिर भी वह ज्ञान ज्ञान स्वरुप ही रहता है। उसी प्रकार केवली भगवान् सव पदार्थों को जानते और देखते है, किन्तु उनका वह जानना असत्य नहीं है। फिर भी वह उनका ज्ञायकभाव पात्मनिष्ठ ही है । उपर्युक्त व्यवहार और निश्चय की कथनी का यही मथितार्थ है।।
उपनिपद मे जो 'य प्रात्मवित् स सर्ववित्', 'य सर्ववित् स आत्मवित्' इत्यादि वचन मिलते है उनका मेल अधिकतर प्रवचनमार के कथन से ही बैठता है । 'नियममार' के कथन से नहीं, क्योकि 'नियमसार में पृथक् पृथक् दो दृष्टियाँ काम कर रही है जब कि प्रवचनमार मे दृष्टिभेद से कथन करने की मुख्यता न होकर सर्वज्ञत्व के समर्थन की मुस्यता है। उपनिषद् मे भी हमे यही वात दिखाई देती है। हाँ, उपनिषद्में 'एक' शब्द के स्थान में 'आत्म' शब्द का प्रयोग अवश्य मिलता है पर इमसे विवेचन करने की दृष्टि नहीं बदली है, जव कि 'नियमसार' में विवेचन करने की दृष्टि ही वदल गई है। इतने विवेचनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि 'प्रवचनसार, 'आचाराग सूत्र' और 'उपनिषद्'इनकी कथनी का प्रयोजन एक है और 'नियमसार' की कथनी का प्रयोजन इससे भिन्न है । 'प्रवचनमार' मे जहां सिद्धात के उद्घाटन करने की ओर झुकाव है, वहाँ 'नियमसार' में मुख्यत मूलभूत तत्त्व की मीमासा करते हुए फलितार्थरूप से उसका कार्यभाग स्वीकार किया गया है। यहां यह कार्यभाग ही अभूतार्थ है क्योकि वह जीव की अशेष ज्ञेयो के निमित्त से होने वाली दशा है और मीमासित तत्त्व ही भूतार्य है, क्योकि जीव में नायकभाव अन्य निमित्तो से उत्पन्न नही होता किन्तु वह उसका स्वभाव है । तात्पर्य यह है कि आचार्य कुन्दकुन्द कारण रूप से प्रात्मनिष्ठ ज्ञायकभाव और कार्यरूप से सर्वज्ञता को स्वीकार करते है जिसका उन्होने अपने 'प्रवचनसार' आदि ग्रथो में बहुत ही सुन्दरता से विवेचन किया है। काशी]
"जाणदि पस्सदि सन्न ववहारणएण केवली भगव । केवलणाणी जाणदि पस्सदि णियमेण अप्पाण ॥१५॥'