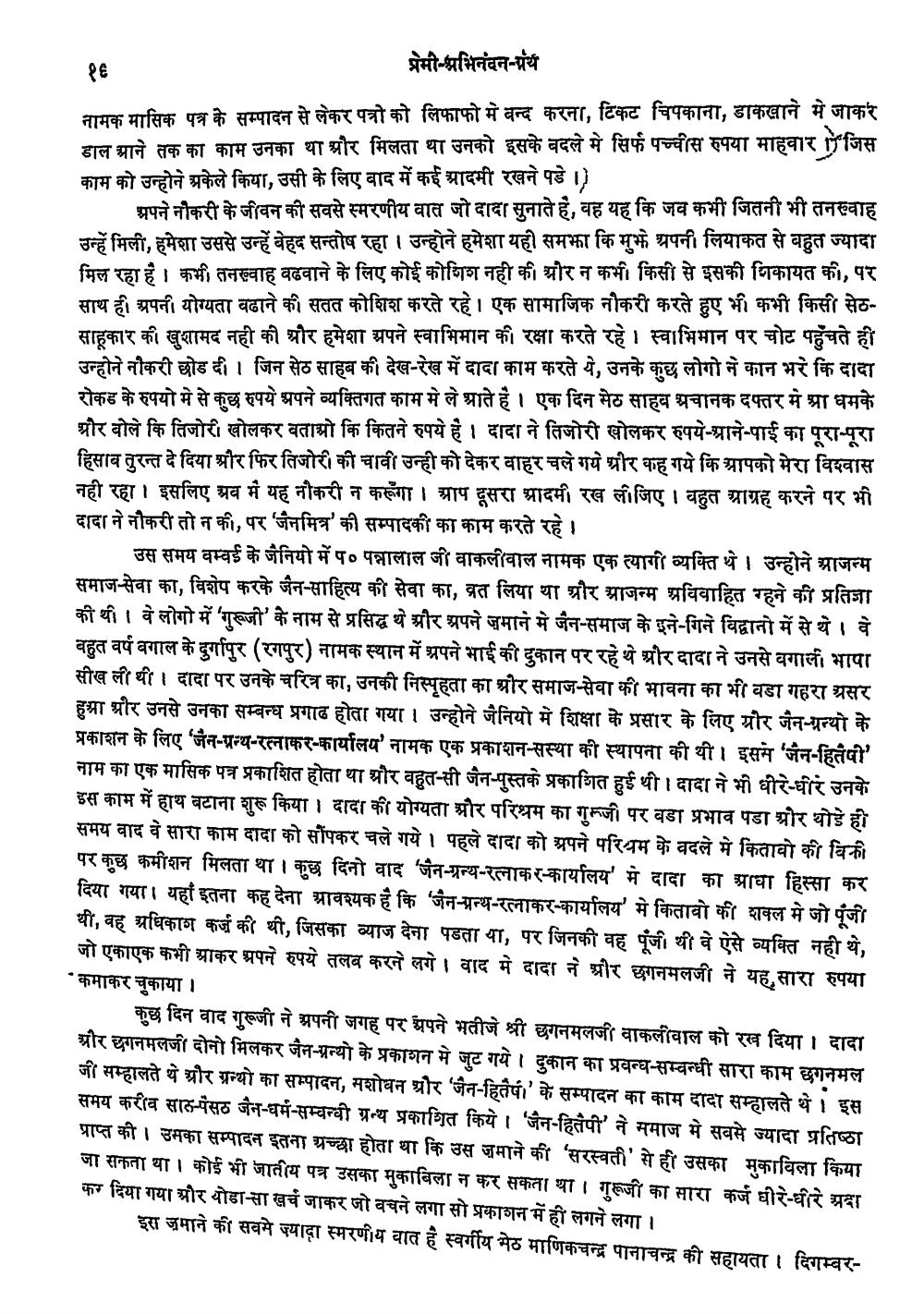________________
१६
प्रेमी-प्रभिनंदन-प्रय नामक मासिक पत्र के सम्पादन से लेकर पत्रो को लिफाफो मे बन्द करना, टिकट चिपकाना, डाकखाने मे जाकर डाल आने तक का काम उनका था और मिलता था उनको इसके बदले में सिर्फ पच्चीस रुपया माहवार जिस काम को उन्होने अकेले किया, उसी के लिए बाद में कई आदमी रखने पडे ।।
अपने नौकरी के जीवन की सबसे स्मरणीय वात जो दादा सुनाते है, वह यह कि जब कभी जितनी भी तनख्वाह उन्हें मिली, हमेशा उससे उन्हें बेहद सन्तोष रहा । उन्होने हमेशा यही समझा कि मुझे अपनी लियाकत से बहुत ज्यादा मिल रहा है। कभी तनख्वाह बढवाने के लिए कोई कोशिश नहीं की और न कभी किसी से इसकी शिकायत की, पर साथ ही अपनी योग्यता बढाने की सतत कोशिश करते रहे। एक सामाजिक नौकरी करते हुए भी कभी किसी सेठसाहूकार की खुशामद नही की और हमेशा अपने स्वाभिमान की रक्षा करते रहे। स्वाभिमान पर चोट पहुंचते ही उन्होने नौकरी छोड दी। जिन सेठ साहब की देख-रेख में दादा काम करते थे, उनके कुछ लोगो ने कान भरे कि दादा रोकड के रुपयो मे से कुछ रुपये अपने व्यक्तिगत काम मे ले आते है। एक दिन मेठ साहब अचानक दफ्तर में आ धमके और बोले कि तिजोरी खोलकर बताओ कि कितने रुपये है। दादा ने तिजोरी खोलकर रुपये-पाने-पाई का पूरा-पूरा हिसाब तुरन्त दे दिया और फिर तिजोरी की चावी उन्ही को देकर बाहर चले गये और कह गये कि आपको मेरा विश्वास नहीं रहा। इसलिए अब मैं यह नौकरी न करूंगा। आप दूसरा आदमी रख लीजिए । बहुत आग्रह करने पर भी दादा ने नौकरी तो न की, पर 'जनमित्र' की सम्पादकी का काम करते रहे।
उस समय वम्बई के जैनियो में प० पन्नालाल जी वाकलीवाल नामक एक त्यागी व्यक्ति थे। उन्होने आजन्म समाज-सेवा का, विशेप करके जैन-साहित्य की सेवा का, व्रत लिया था और आजन्म अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा की थी। वे लोगो में 'गुरुजी' के नाम से प्रसिद्ध थे और अपने जमाने मे जैन समाज के इने-गिने विद्वानो में से थे। वे बहुत वर्ष बगाल के दुर्गापुर (रंगपुर) नामक स्थान में अपने भाई की दुकान पर रहे थे और दादा ने उनसे बगाली भाषा सीख ली थी। दादा पर उनके चरित्र का, उनकी निस्पृहता का और समाज-सेवा की भावना का भी वडा गहरा असर हुआ और उनसे उनका सम्बन्ध प्रगाढ होता गया। उन्होने जैनियो मे शिक्षा के प्रसार के लिए और जैन-ग्रन्थो के प्रकाशन के लिए 'जन-ग्रन्थ-रत्नाकर-कार्यालय' नामक एक प्रकाशन-सस्था की स्थापना की थी। इसमे 'जैन-हितैषी' नाम का एक मासिक पत्र प्रकाशित होता था और बहुत-सी जैन-पुस्तके प्रकाशित हुई थी। दादा ने भी धीरे-धीरे उनके इस काम में हाथ बटाना शुरू किया। दादा की योग्यता और परिश्रम का गुरुजी पर बडा प्रभाव पडा और थोडे ही समय बाद वे सारा काम दादा को सौंपकर चले गये। पहले दादा को अपने परियम के बदले मे कितावो की विकी पर कुछ कमीशन मिलता था। कुछ दिनो वाद 'जैन-ग्रन्थ-रत्नाकर-कार्यालय में दादा का आधा हिस्सा कर दिया गया। यहां इतना कह देना आवश्यक है कि 'जैन-ग्रन्थ-रत्नाकर-कार्यालय मे कितावो की शक्ल मे जो पूंजी थी, वह अधिकाश कर्ज की थी, जिसका व्याज देना पड़ता था, पर जिनकी वह पूंजी थी वे ऐसे व्यक्ति नहीं थे, जो एकाएक कभी आकर अपने रुपये तलब करने लगे। वाद मे दादा ने और छगनमलजी ने यह सारा रुपया 'कमाकर चुकाया।
कुछ दिन बाद गुरूजी ने अपनी जगह पर अपने भतीजे श्री छगनमलजी वाकलीवाल को रख दिया। दादा और छगनमलजी दोनो मिलकर जैन-प्रन्यो के प्रकाशन मे जुट गये। दुकान का प्रवन्ध-सम्बन्धी सारा काम छगनमल जी सम्हालते थे और ग्रन्थो का सम्पादन, मशोधन और 'जैन-हितपी' के सम्पादन का काम दादा सम्हालते थे। इस समय करीव सास-पैसठ जैन-धर्म-सम्बन्धी ग्रन्थ प्रकाशित किये । 'जैन-हितैपी' ने ममाज में सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा प्राप्त की। उमका सम्पादन इतना अच्छा होता था कि उस जमाने की 'सरस्वती' से ही उसका मुकाविला किया जा सकता था। कोई भी जातीय पत्र उसका मुकाबिला न कर सकता था। गुरूजी का सारा कर्ज धीरे-धीरे अदा कर दिया गया और योडा-सा खर्च जाकर जो वचने लगा सो प्रकाशन में ही लगने लगा।
इरा ज़माने की सबसे ज्यादा स्मरणीय बात है स्वर्गीय भेठ माणिकचन्द्र पानाचन्द्र की सहायता । दिगम्बर