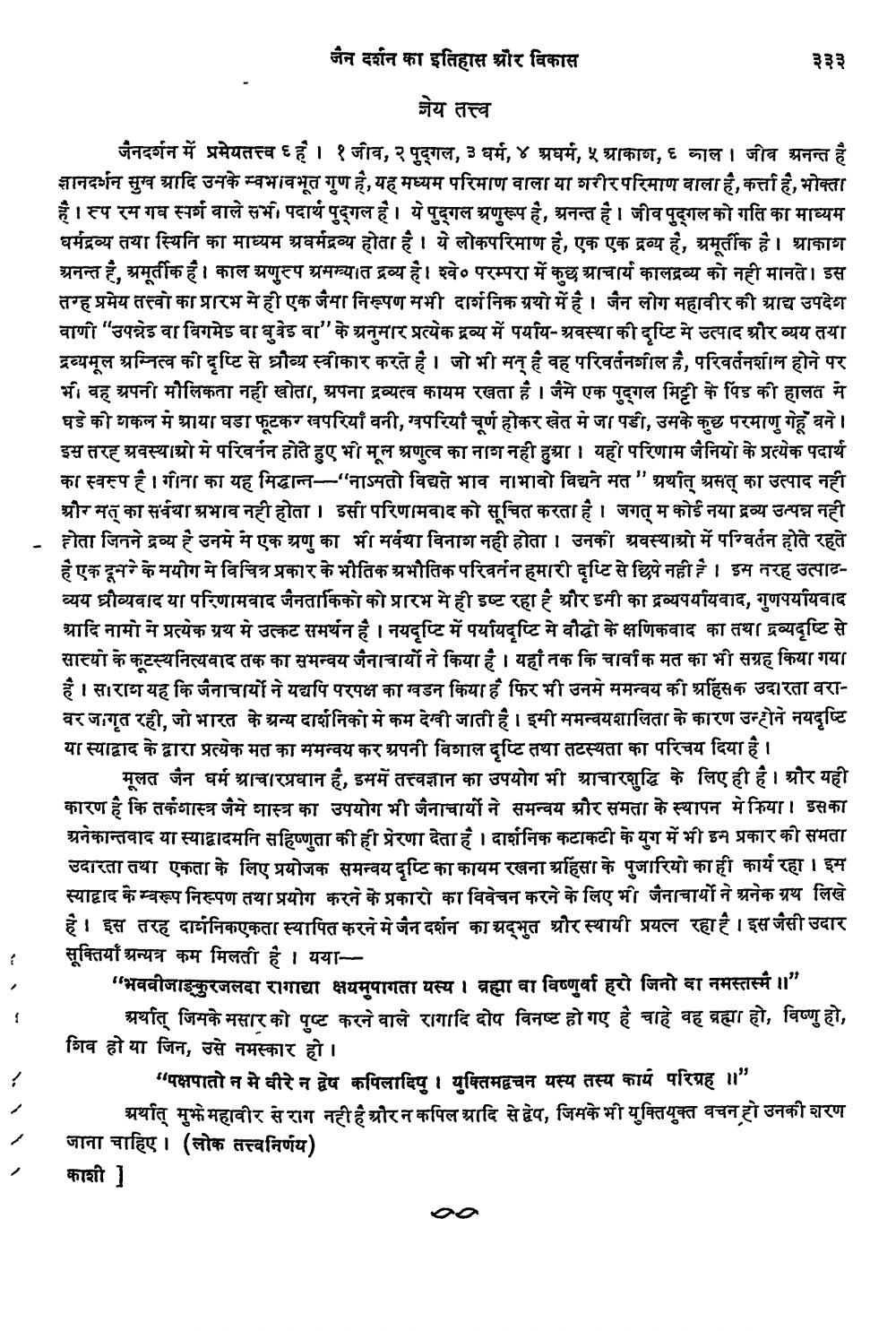________________
जैन दर्शन का इतिहास और विकास
जेय तत्त्व जनदर्शन में प्रमेयतत्त्व है। १ जीव, २ पुद्गल, ३ धर्म, ४ अधर्म, ५ अाकाग, ६ लाल । जीव अनन्त है ज्ञानदर्शन सुख प्रादि उनके स्वभावभूत गुण है, यह मध्यम परिमाण वाला या शरीर परिमाण वाला है, कर्ता है, भोक्ता है। स्प रस गव सर्ग वाले सभी पदार्थ पुद्गल है। ये पुद्गल अणुरूप है, अनन्त है । जीवपुद्गल को गति का माध्यम धर्मद्रव्य तथा स्थिति का माध्यम अधर्मद्रव्य होता है । ये लोकपरिमाण है, एक एक द्रव्य है, अमूर्तीक है। प्राकाश अनन्त है, अमूर्तीक है। काल अणुस्प अमन्यात द्रव्य है। श्वे० परम्परा में कुछ प्राचार्य कालद्रव्य को नहीं मानते। इस तरह प्रमेय तत्त्वो का प्रारभ से ही एक जैमा निरूपण मभी दार्शनिक ग्रयो में है । जैन लोग महावीर की पाद्य उपदेश वाणी "उपनेड वा विगमेड वा बेड वा" के अनुमार प्रत्येक द्रव्य में पर्याय-अवस्था की दृष्टि में उत्पाद और व्यय तया द्रव्यमूल अग्नित्व की दृष्टि से घोव्य स्वीकार करते है। जो भी मन् है वह परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील होने पर भी वह अपनी मौलिकता नहीं खोता, अपना द्रव्यत्व कायम रखता है । जैसे एक पुद्गल मिट्टी के पिंड की हालत में घडे को शकल में पाया घडा फूटकर खपरियां वनी, वपरियां चूर्ण होकर खेत मे जा पडी, उमके कुछ परमाणु गेहूं बने। इस तरह अवस्थाप्रो में परिवर्तन होते हुए भी मूल अणुत्व का नाश नही हुआ । यही परिणाम जैनियो के प्रत्येक पदार्थ का स्वस्प है। गीता का यह मिद्धान्त-"नाऽसतो विद्यते भाव नाभावो विद्यते मत" अर्थात् असत् का उत्पाद नहीं और मत् का सर्वथा अभाव नहीं होता। इसी परिणामवाद को सूचित करता है । जगत् म कोई नया द्रव्य उत्पन्न नहीं होता जिनने द्रव्य है उनमे में एक अणु का भी मर्वथा विनाश नहीं होता। उनकी अवस्थाओ में परिवर्तन होते रहते है एक दूसरे केमयोग मे विचित्र प्रकार के भौतिक अभौतिक परिवर्तन हमारी दृष्टि से छिपे नहीं है। इस तरह उत्पादव्यय प्रौव्यवाद या परिणामवाद जैनतार्किको को प्रारभ मे ही इष्ट रहा है और इमी का द्रव्यपर्यायवाद, गुणपर्यायवाद आदि नामो ने प्रत्येक ग्रय मे उत्कट समर्थन है । नयदृष्टि में पर्यायदृष्टि मे वौद्धो के क्षणिकवाद का तथा द्रव्यदृष्टि से सात्यो के कूटस्यनित्यवाद तक का समन्वय जैनाचार्यों ने किया है। यहां तक कि चार्वाक मत का भी सग्रह किया गया है। साराग यह कि जैनाचार्यों ने यद्यपि परपक्ष का वडन किया है फिर भी उनमे समन्वय की अहिंसक उदारता वरावर जागृत रही, जो भारत के अन्य दार्शनिको मे कम देखी जाती है । इसी ममन्वयशालिता के कारण उन्होने नयदृष्टि या स्याद्वाद के द्वारा प्रत्येक मत का समन्वय कर अपनी विशाल दृष्टि तथा तटस्थता का परिचय दिया है।
मूलत जैन धर्म प्राचारप्रधान है, इसमें तत्त्वज्ञान का उपयोग भी प्राचारशुद्धि के लिए ही है। और यही कारण है कि तर्कशास्त्र जमे शास्त्र का उपयोग भी जैनाचार्यों ने समन्वय और समता के स्थापन मे किया। इसका अनेकान्तवाद या स्याद्वादमति सहिष्णुता की ही प्रेरणा देता है । दार्शनिक कटाकटी के युग में भी इस प्रकार की समता उदारता तथा एकता के लिए प्रयोजक समन्वय दृष्टि का कायम रखना अहिंसा के पुजारियो का ही कार्य रहा । इस स्याबाद के स्वरूप निरूपण तथा प्रयोग करने के प्रकारो का विवेचन करने के लिए भी जैनाचार्यों ने अनेक ग्रथ लिखे है। इस तरह दार्गनिकएकता स्यापित करने मे जैन दर्शन का अद्भुत और स्थायी प्रयत्न रहा है । इस जैसी उदार सूक्तियाँ अन्यत्र कम मिलती है। यया
"भववीजाङ्कुरजलदा रागाद्या क्षयमुपागता यस्य । ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै ॥" ___ अर्थात् जिसके मसार को पुष्ट करने वाले रागादि दोष विनष्ट हो गए है चाहे वह ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शिव हो या जिन, उसे नमस्कार हो।
"पक्षपातो न मे वीरे न द्वेष कपिलादिषु । युक्तिमद्वचन यस्य तस्य कार्य परिग्रह ॥" अर्थात् मुझे महावीर से राग नहीं है और न कपिल आदि से द्वेप, जिमके भी युक्तियुक्त वचन हो उनकी शरण जाना चाहिए। (लोक तत्त्वनिर्णय) काशी ]
1
जाना