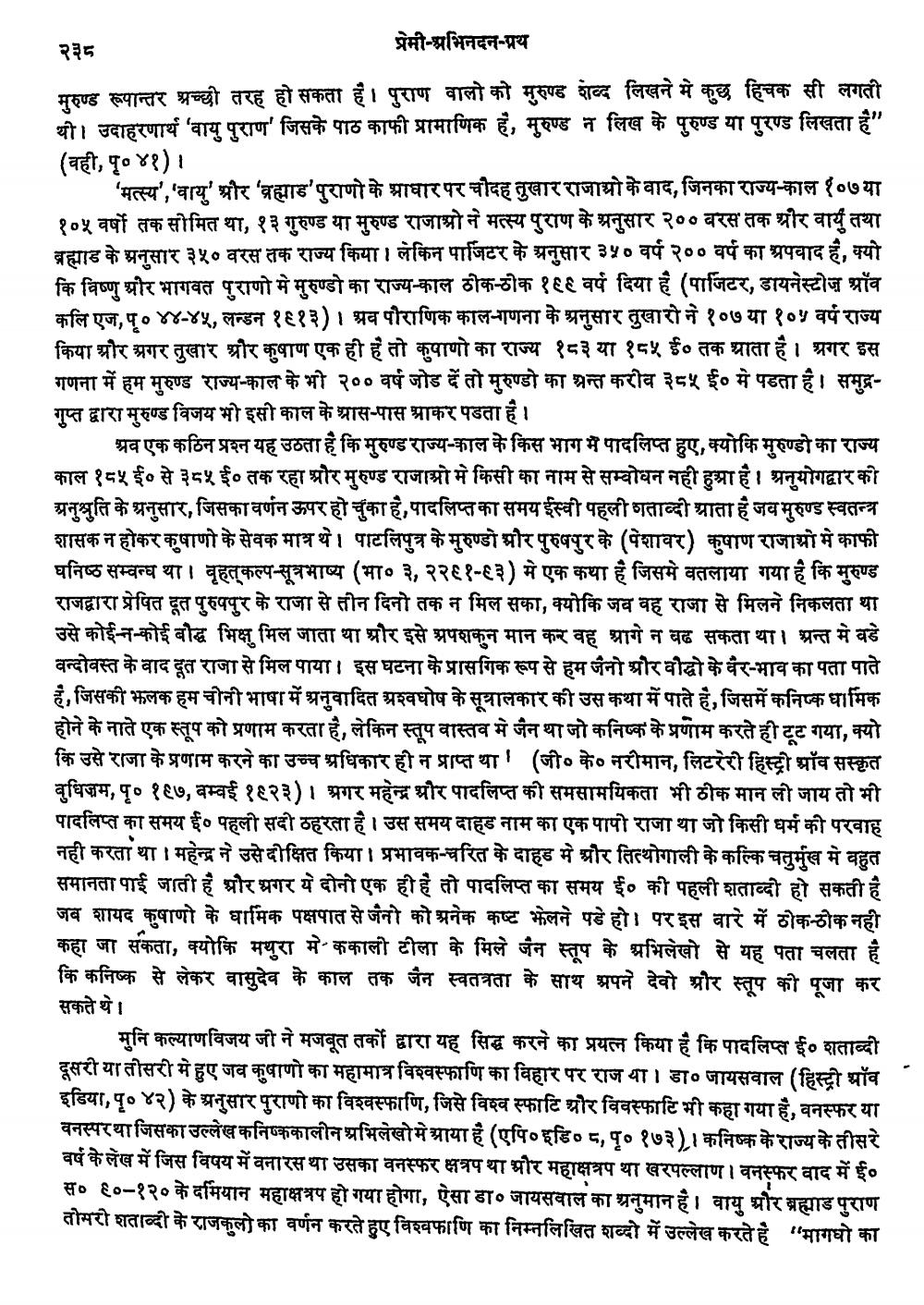________________
प्रेमी-अभिनदन-प्रय २३८ मुरुण्ड रूपान्तर अच्छी तरह हो सकता है। पुराण वालो को मुरुण्ड शब्द लिखने में कुछ हिचक सी लगती थी। उदाहरणार्थ 'वायु पुराण' जिसके पाठ काफी प्रामाणिक है, मुरुण्ड न लिख के पुरुण्ड या पुरण्ड लिखता है" (वही, पृ०४१)।
'मत्स्य','वायु' और 'ब्रह्माड' पुराणो के आधार पर चौदह तुखार राजामो के वाद, जिनका राज्य-काल १०७ या १०५ वर्षों तक सीमित था, १३ गुरुण्ड या मुरुण्ड राजाओ ने मत्स्य पुराण के अनुसार २०० बरस तक और वायु तथा ब्रह्माड के अनुसार ३५० वरस तक राज्य किया। लेकिन पाजिटर के अनुसार ३५० वर्प २०० वर्ष का अपवाद है, क्यो कि विष्णु और भागवत पुराणो मे मुरुण्डो का राज्य-काल ठीक-ठोक १९६ वर्ष दिया है (पाजिटर, डायनेस्टोज़ आँव कलि एज, पृ० ४४-४५, लन्डन १९१३) । अव पौराणिक काल-गणना के अनुसार तुखारोने १०७ या १०५ वर्ष राज्य किया और अगर तुखार और कुषाण एक ही है तो कुपाणो का राज्य १८३ या १८५ ई० तक पाता है। अगर इस गणना में हम मुरुण्ड राज्य-काल के भो २०० वर्ष जोड दें तो मुरुण्डो का अन्त करीव ३८५ ई० मे पडता है। समुद्रगुप्त द्वारा मुरुण्ड विजय भी इसी काल के पास-पास आकर पड़ता है।
अव एक कठिन प्रश्न यह उठता है कि मुरुण्डराज्य-काल के किस भाग में पादलिप्त हुए, क्योकि मुरुण्डो का राज्य काल १८५ ई० से ३८५ ई० तक रहा और मुरुण्ड राजाओ मे किसी का नाम से सम्बोधन नहीं हुआ है। अनुयोगद्वार को अनुश्रुति के अनुसार, जिसका वर्णन ऊपर हो चुका है, पादलिप्तका समय ईस्वी पहली शताब्दी पाता है जव मुरुण्ड स्वतन्त्र शासक न होकर कुषाणो के सेवक मात्र थे। पाटलिपुत्र के मुरुण्डो और पुरुषपुर के (पेशावर) कुषाण राजानो मे काफी घनिष्ठ सम्वन्ध था। बृहत्कल्प-सूत्रभाष्य (भा० ३, २२६१-६३) मे एक कथा है जिसमे वतलाया गया है कि मुरुण्ड राजद्वारा प्रेषित दूत पुरुषपुर के राजा से तीन दिनो तक न मिल सका, क्योकि जब वह राजा से मिलने निकलता था उसे कोई-न-कोई बौद्ध भिक्षु मिल जाता था और इसे अपशकुन मान कर वह आगे न बढ सकता था। अन्त मे वडे वन्दोवस्त के बाद दूत राजा से मिल पाया। इस घटना के प्रासगिक रूप से हम जैनो और वौद्धो के वर-भाव का पता पाते है, जिसकी झलक हम चीनी भाषा में अनुवादित अश्वघोष के सूत्रालकार की उस कथा में पाते है, जिसमें कनिष्क धार्मिक होने के नाते एक स्तूप को प्रणाम करता है, लेकिन स्तूप वास्तव मे जैन था जो कनिष्क के प्रणाम करते ही टूट गया, क्यो कि उसे राजा के प्रणाम करने का उच्च अधिकार ही न प्राप्त था। (जी० के० नरीमान, लिटरेरी हिस्ट्री प्रॉव सस्कृत बुधिजम, पृ० १६७, बम्बई १९२३)। अगर महेन्द्र और पादलिप्त की समसामयिकता भी ठीक मान ली जाय तो भी पादलिप्त का समय ई० पहली सदी ठहरता है। उस समय दाहड़ नाम का एक पापी राजा था जो किसी धर्म की परवाह नही करता था। महेन्द्र ने उसे दीक्षित किया। प्रभावक-चरित के दाहड मे और तित्थोगाली के कल्कि चतुर्मुख मे बहुत समानता पाई जाती है और अगर ये दोनो एक ही है तो पादलिप्त का समय ई० की पहली शताब्दी हो सकती है जब शायद कुषाणो के धार्मिक पक्षपात से जैनो को अनेक कष्ट झेलने पडे हो। पर इस बारे में ठीक-ठीक नही कहा जा सकता, क्योकि मथुरा मे ककाली टोला के मिले जैन स्तूप के अभिलेखो से यह पता चलता है कि कनिष्क से लेकर वासुदेव के काल तक जैन स्वतत्रता के साथ अपने देवो और स्तूप की पूजा कर सकते थे।
मुनि कल्याणविजय जी ने मजबूत तर्को द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि पादलिप्त ई० शताब्दी दूसरी या तीसरी मे हुए जव कुषाणो का महामात्र विश्वस्फाणि का विहार पर राज था। डा. जायसवाल (हिस्ट्री ऑव इडिया, पृ०४२) के अनुसार पुराणो का विश्वस्फाणि, जिसे विश्व स्फाटि और विवस्फाटि भी कहा गया है, वनस्फर या वनस्परथा जिसका उल्लेख कनिष्ककालीन अभिलेखोमेाया है (एपि० इडि०८, पृ० १७३) कनिष्क के राज्य के तीसरे वर्ष के लेख में जिस विषय में वनारस था उसका वनस्फर क्षत्रप था और महाक्षत्रप था खरपल्लाण । वनस्फर वाद में ई० स० ६०-१२० के दमियान महाक्षत्रप हो गया होगा, ऐसा डा० जायसवाल का अनुमान है। वायु और ब्रह्माड पुराण तोमरो शताब्दी के राजकुलो का वर्णन करते हुए विश्वफाणि का निम्नलिखित शब्दो में उल्लेख करते है "मागधो का