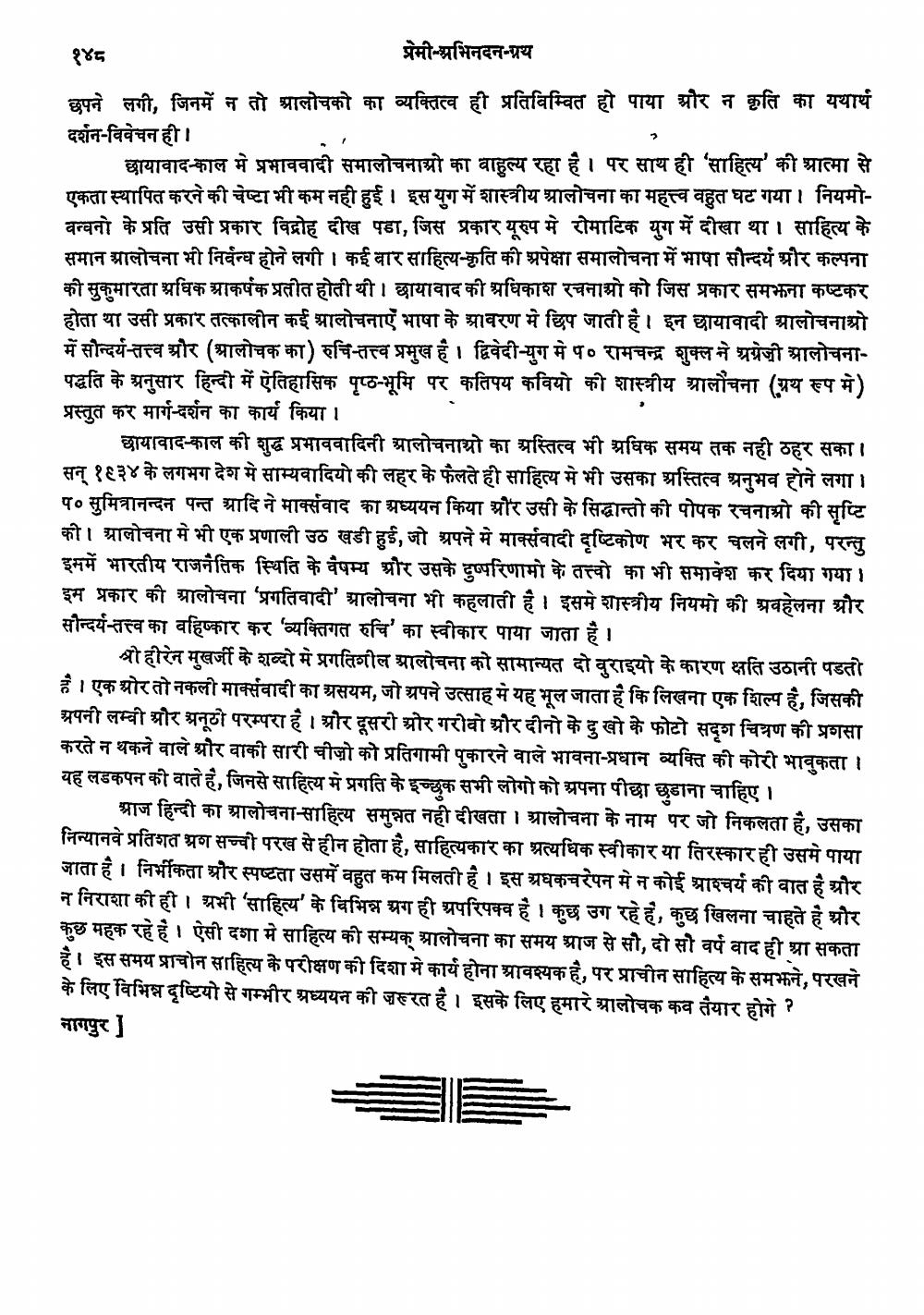________________
१४८
प्रेमी-अभिनदन-प्रथ छपने लगी, जिनमें न तो आलोचको का व्यक्तित्व ही प्रतिविम्वित हो पाया और न कृति का यथार्थ दर्शन-विवेचनही।
छायावाद काल मे प्रभाववादी समालोचनाओ का बाहुल्य रहा है । पर साथ ही 'साहित्य' की आत्मा से एकता स्थापित करने की चेष्टा भी कम नही हुई। इस युग में शास्त्रीय आलोचना का महत्त्व बहुत घट गया। नियमोवन्वनो के प्रति उसी प्रकार विद्रोह दीख पडा, जिस प्रकार यूरुप मे रोमाटिक युग में दोखा था। साहित्य के समान आलोचना भी निर्वन्ध होने लगी। कई बार साहित्य-कृति की अपेक्षा समालोचना में भाषा सौन्दर्य और कल्पना को सुकुमारता अधिक आकर्षक प्रतीत होती थी। छायावाद की अधिकाश रचनाओ को जिस प्रकार समझना कष्टकर होता था उसी प्रकार तत्कालीन कई आलोचनाएँ भाषा के आवरण मे छिप जाती है। इन छायावादी आलोचनाओ में सौन्दर्य-तत्त्व और (आलोचक का) रुचि-तत्त्व प्रमुख है। द्विवेदी-युग मे प० रामचन्द्र शुक्ल ने अग्रेज़ी आलोचनापद्धति के अनुसार हिन्दी में ऐतिहासिक पृष्ठ-भूमि पर कतिपय कवियो को शास्त्रीय आलोचना (अथ रूप में) प्रस्तुत कर मार्ग-दर्शन का कार्य किया।
छायावाद-काल की शुद्ध प्रभाववादिनी आलोचनायो का अस्तित्व भी अधिक समय तक नही ठहर सका। सन् १९३४ के लगभग देश मे साम्यवादियो की लहर के फैलते ही साहित्य मे भी उसका अस्तित्व अनुभव होने लगा। प० सुमित्रानन्दन पन्त आदि ने मार्क्सवाद का अध्ययन किया और उसी के सिद्धान्तो की पोपक रचनाओ की सृष्टि की। आलोचना में भी एक प्रणाली उठ खडी हुई, जो अपने मे मार्क्सवादी दृष्टिकोण भर कर चलने लगी, परन्तु इममें भारतीय राजनैतिक स्थिति के वैषम्य और उसके दुष्परिणामो के तत्त्वो का भी समावेश कर दिया गया। इस प्रकार की आलोचना 'प्रगतिवादी' आलोचना भी कहलाती है। इसमे शास्त्रीय नियमो की अवहेलना और सौन्दर्य-तत्त्व का बहिष्कार कर 'व्यक्तिगत रुचि' का स्वीकार पाया जाता है।
श्री हीरेन मुखर्जी के शब्दो मे प्रगतिशील पालोचना को सामान्यत दो वुराइयो के कारण क्षति उठानी पडतो है । एक ओर तो नकली मार्क्सवादी का असयम, जो अपने उत्साह में यह भूल जाता है कि लिखना एक शिल्प है, जिसकी अपनी लम्बी और अनूठो परम्परा है । और दूसरी ओर गरोवो और दीनो के दुखो के फोटो सदृश चित्रण की प्रशसा करते न थकने वाले और वाकी सारी चीज़ो को प्रतिगामी पुकारने वाले भावना-प्रधान व्यक्ति की कोरी भावुकता। यह लडकपन की वाते है, जिनसे साहित्य में प्रगति के इच्छुक सभी लोगो को अपना पीछा छुडाना चाहिए।
आज हिन्दी का आलोचना-साहित्य समुन्नत नहीं दीखता। आलोचना के नाम पर जो निकलता है, उसका निन्यानवे प्रतिशत अग सच्ची परख से हीन होता है, साहित्यकार का अत्यधिक स्वीकार या तिरस्कार ही उसमे पाया जाता है। निर्भीकता और स्पष्टता उसमें बहुत कम मिलती है । इस अधकचरेपन मे न कोई आश्चर्य की बात है और न निराशा की ही। अभी 'साहित्य' के विभिन्न अंग ही अपरिपक्व है । कुछ उग रहे है, कुछ खिलना चाहते है और कुछ महक रहे है । ऐसी दशा मे साहित्य की सम्यक् आलोचना का समय आज से सौ, दो सौ वर्ष वाद ही आ सकता है। इस समय प्राचीन साहित्य के परीक्षण की दिशा मे कार्य होना आवश्यक है, पर प्राचीन साहित्य के समझने, परखने के लिए विभिन्न दृष्टियो से गम्भीर अध्ययन की ज़रूरत है। इसके लिए हमारे आलोचक कव तैयार होगे? नागपुर
-