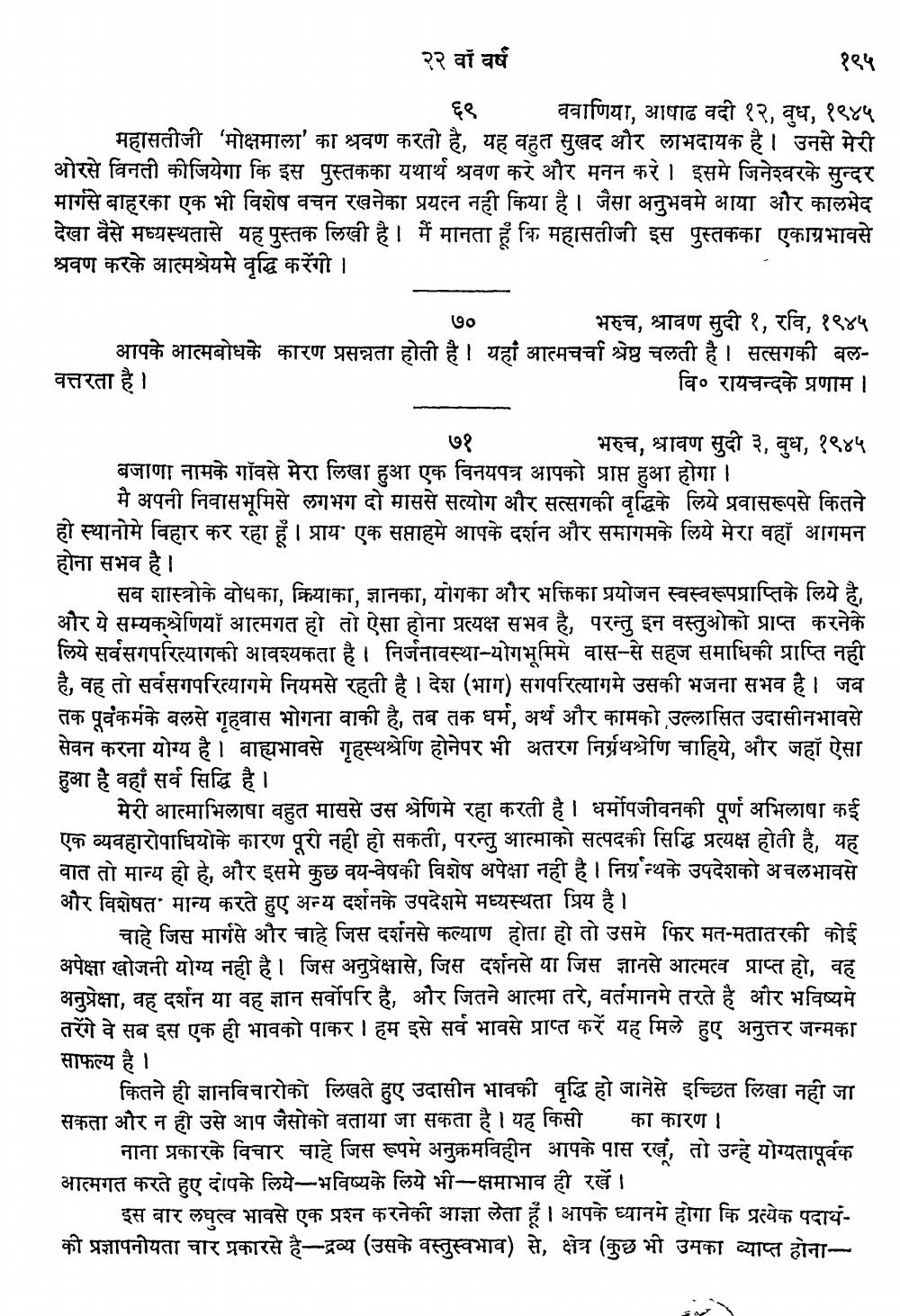________________
२२ वॉ वर्ष
१९५
६९
वाणिया, आषाढ वदी १२, बुध, १९४५ महासतीजी 'मोक्षमाला' का श्रवण करती है, यह बहुत सुखद और लाभदायक है । उनसे मेरी ओरसे विनती कीजियेगा कि इस पुस्तकका यथार्थ श्रवण करे और मनन करे । इसमे जिनेश्वरके सुन्दर मार्गसे बाहरका एक भी विशेष वचन रखनेका प्रयत्न नही किया है । जैसा अनुभवमे आया और कालभेद देखा वैसे मध्यस्थतासे यह पुस्तक लिखी है । में मानता हूँ कि महासतीजी इस पुस्तकका एकाग्र भावसे श्रवण करके आत्मश्रेयमे वृद्धि करेंगी ।
७०
भरुच, श्रावण सुदी १, रवि, १९४५ आपके आत्मबोधके कारण प्रसन्नता होती है । यहाँ आत्मचर्चा श्रेष्ठ चलती है । सत्सगकी बलवत्तरता है । वि० रायचन्दके प्रणाम ।
७१
भरुच, श्रावण सुदी ३, बुध, १९४५
बजाणा नामके गाँवसे मेरा लिखा हुआ एक विनयपत्र आपको प्राप्त हुआ होगा । मै अपनी निवासभूमिसे लगभग दो माससे सत्योग और सत्सगकी वृद्धिके लिये प्रवासरूपसे कितने हो स्थानोमे विहार कर रहा हूँ । प्राय एक सप्ताहमे आपके दर्शन और समागमके लिये मेरा वहाँ आगमन होना संभव है ।
सब शास्त्रोके बोधका क्रियाका, ज्ञानका, योगका और भक्तिका प्रयोजन स्वस्वरूपप्राप्तिके लिये है, और ये सम्यकश्रेणियाँ आत्मगत हो तो ऐसा होना प्रत्यक्ष संभव है, परन्तु इन वस्तुओको प्राप्त करनेके लिये सर्वसंगपरित्यागको आवश्यकता है । निर्जनावस्था - योगभूमिमे वास - से सहज समाधिकी प्राप्ति नही है, वह तो सर्वसंगपरित्यागमे नियमसे रहती है । देश (भाग) सगपरित्यागमे उसकी भजना सभव है । जब तक पूर्वकर्मके बलसे गृहवास भोगना बाकी है, तब तक धर्म, अर्थ और कामको उल्लासित उदासीनभावसे सेवन करना योग्य है । बाह्यभावसे गृहस्थश्रेणि होनेपर भी अतरग निर्ग्रथश्रेणि चाहिये, और जहाँ ऐसा हुआ है वहाँ सर्वसिद्धि है ।
मेरी आत्माभिलाषा बहुत माससे उस श्रेणिमे रहा करती है। धर्मोपजीवनकी पूर्ण अभिलाषा कई एक व्यवहारोपाधियोके कारण पूरी नही हो सकती, परन्तु आत्माको सत्पदकी सिद्धि प्रत्यक्ष होती है, यह तो मान्य हो है, और इसमे कुछ वय - वेषकी विशेष अपेक्षा नही है । निर्ग्रन्थके उपदेशको अचलभावसे और विशेषत' मान्य करते हुए अन्य दर्शनके उपदेशमे मध्यस्थता प्रिय है ।
चाहे जिस मार्ग से और चाहे जिस दर्शनसे कल्याण होता हो तो उसमे फिर मत-मतातरकी कोई अपेक्षा खोजनी योग्य नही है । जिस अनुप्रेक्षासे, जिस दर्शनसे या जिस ज्ञानसे आत्मत्व प्राप्त हो, वह अनुप्रेक्षा, वह दर्शन या वह ज्ञान सर्वोपरि है, और जितने आत्मा तरे, वर्तमानमे तरते है और भविष्य मे तरेंगे वे सब इस एक ही भावको पाकर । हम इसे सर्व भावसे प्राप्त करें यह मिले हुए अनुत्तर जन्मका साफल्य है
कितने ही ज्ञानविचारोको लिखते हुए उदासीन भावकी वृद्धि हो जानेसे इच्छित लिखा नही जा सकता और न ही उसे आप जैसोको बताया जा सकता है । यह किसी का कारण ।
नाना प्रकारके विचार चाहे जिस रूपमे अनुक्रमविहीन आपके पास रखूं, तो उन्हे योग्यतापूर्वक आत्मगत करते हुए दोपके लिये - भविष्य के लिये भी- क्षमाभाव ही रखें ।
इस बार लघुत्व भावसे एक प्रश्न करनेकी आज्ञा लेता हूँ । आपके ध्यानमे होगा कि प्रत्येक पदार्थप्रज्ञापनीयता चार प्रकारसे है- द्रव्य (उसके वस्तुस्वभाव) से, क्षेत्र (कुछ भी उसका व्याप्त होना