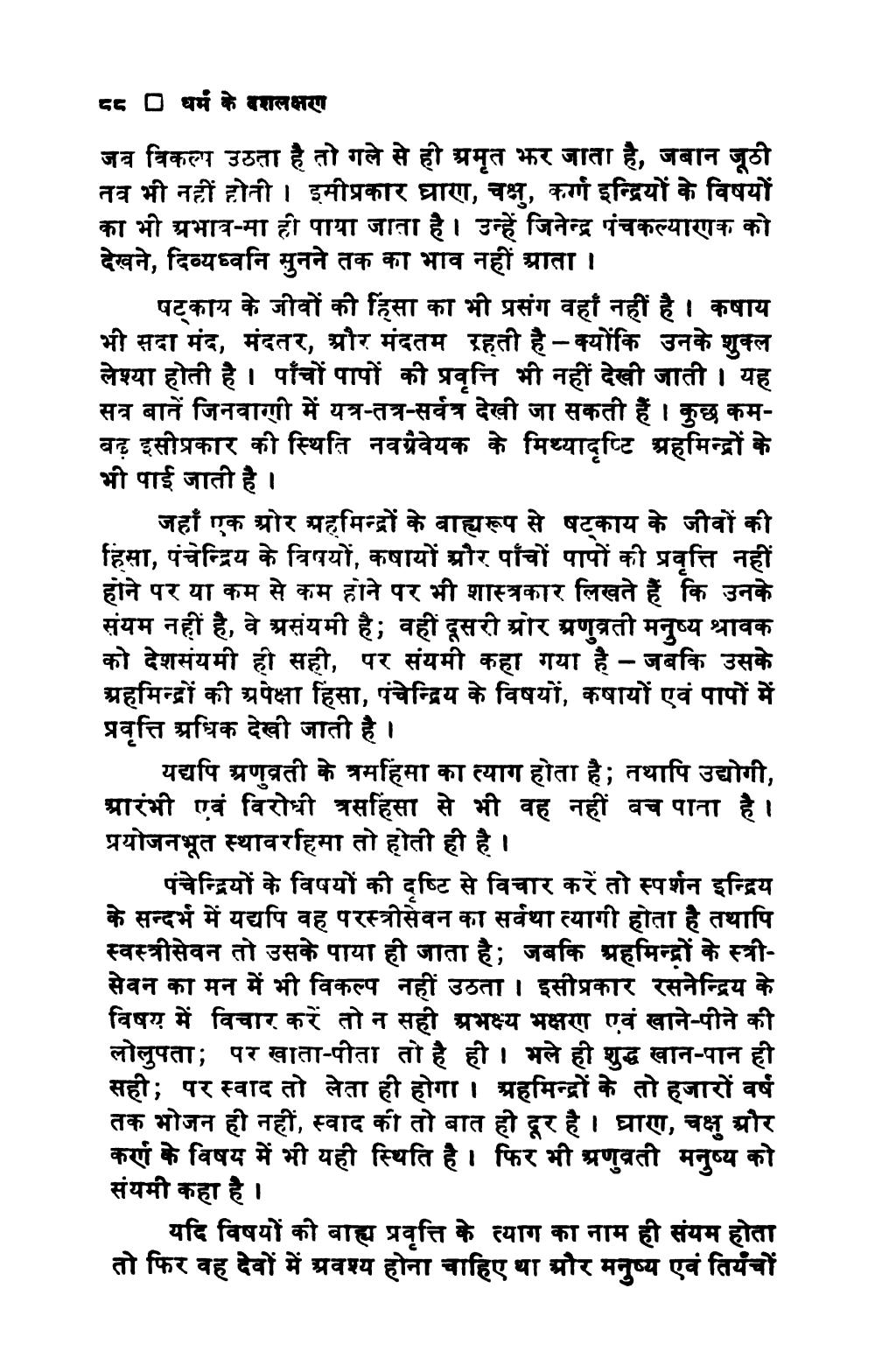________________
८८ धर्म के बरालक्षण जब विकल्प उठता है तो गले से ही अमृत झर जाता है, जबान जूठी नव भी नहीं होती। इसीप्रकार घ्राण, चक्षु, कर्ण इन्द्रियों के विषयों का भी प्रभाव-मा ही पाया जाता है। उन्हें जिनेन्द्र पंचकल्याणक को देखने, दिव्यध्वनि सुनने तक का भाव नहीं आता।
षटकाय के जीवों की हिंसा का भी प्रसंग वहाँ नहीं है। कषाय भी सदा मंद, मंदतर, और मंदतम रहती है - क्योंकि उनके शुक्ल लेश्या होती है। पाँचों पापों की प्रवृत्ति भी नहीं देखी जाती। यह सब बातें जिनवाणी में यत्र-तत्र-सर्वत्र देखी जा सकती हैं । कुछ कमबढ़ इसीप्रकार की स्थिति नवग्रैवेयक के मिथ्यादप्टि अहमिन्द्रों के भी पाई जाती है।
जहाँ एक ओर अहमिन्द्रों के बाह्यरूप से षट्काय के जीवों की हिसा, पंचेन्द्रिय के विषयों, कषायों और पाँचों पापों की प्रवृत्ति नहीं होने पर या कम से कम होने पर भी शास्त्रकार लिखते हैं कि उनके संयम नहीं है, वे असंयमी है। वहीं दूसरी ओर अणुव्रती मनुष्य श्रावक को देशसंयमी ही सही, पर संयमी कहा गया है - जबकि उसके अहमिन्द्रों की अपेक्षा हिंसा, पंचेन्द्रिय के विषयों, कषायों एवं पापों में प्रवृत्ति अधिक देखी जाती है।
यद्यपि अणुव्रती के त्रमहिमा का त्याग होता है; तथापि उद्योगी, प्रारंभी एवं विरोधी त्रसहिंसा से भी वह नहीं बच पाता है। प्रयोजनभूत स्थावहिमा तो होती ही है।
__ पंचेन्द्रियों के विषयों की दृष्टि से विचार करें तो स्पर्शन इन्द्रिय के सन्दर्भ में यद्यपि वह परस्त्रीसेवन का सर्वथा त्यागी होता है तथापि स्वस्त्रीसेवन तो उसके पाया ही जाता है। जबकि अहमिन्द्रों के स्त्रीसेवन का मन में भी विकल्प नहीं उठता। इसीप्रकार रसनेन्द्रिय के विषय में विचार करें तो न सही अभक्ष्य भक्षरण एवं खाने-पीने की लोलुपता; पर खाता-पीता तो है ही। भले ही शुद्ध खान-पान ही सही; पर स्वाद तो लेता ही होगा। अहमिन्द्रों के तो हजारों वर्ष तक भोजन ही नहीं, स्वाद की तो बात ही दूर है। घ्राण, चक्षु और कर्ण के विषय में भी यही स्थिति है। फिर भी अणुवती मनुष्य को संयमी कहा है। ___ यदि विषयों को वाह्य प्रवृत्ति के त्याग का नाम ही संयम होता तो फिर वह देवों में अवश्य होना चाहिए था और मनुष्य एवं तियंचों