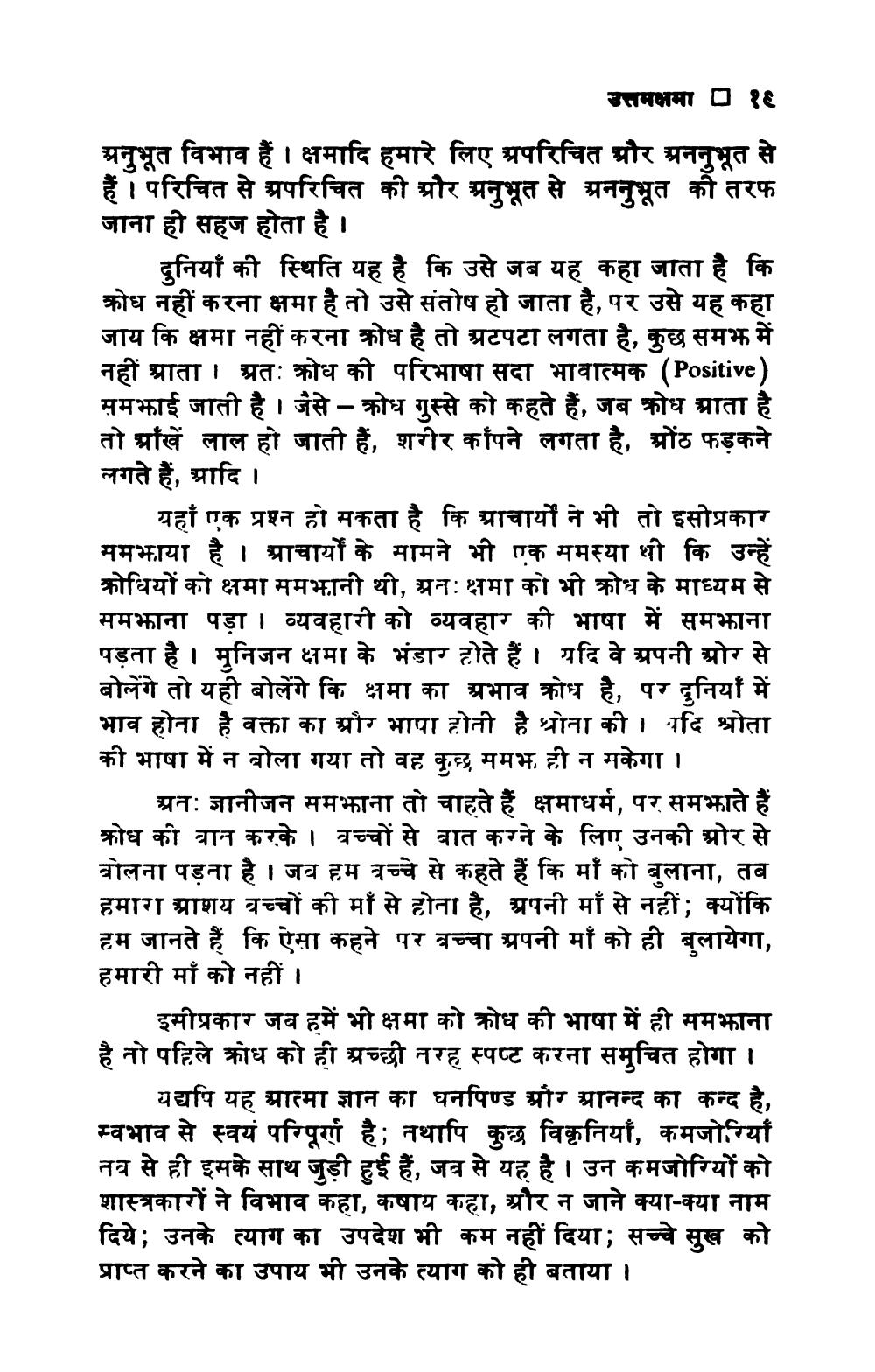________________
उत्तमक्षमा १६
से
अनुभूत विभाव हैं । क्षमादि हमारे लिए अपरिचित और अननुभूत हैं । परिचित से अपरिचित की और अनुभूत से अननुभूत की तरफ जाना ही सहज होता है ।
दुनियाँ की स्थिति यह है कि उसे जब यह कहा जाता है कि क्रोध नहीं करना क्षमा है तो उसे संतोष हो जाता है, पर उसे यह कहा जाय कि क्षमा नहीं करना क्रोध है तो अटपटा लगता है, कुछ समझ में नहीं आता । अतः क्रोध की परिभाषा सदा भावात्मक (Positive ) समझाई जाती है । जैसे - क्रोध गुस्से को कहते हैं, जब क्रोध आता है तो आँखें लाल हो जाती हैं, शरीर काँपने लगता है, मोंठ फड़कने लगते हैं, आदि ।
यहाँ एक प्रश्न हो सकता है कि प्राचार्यों ने भी तो इसीप्रकार समझाया है । प्राचार्यों के सामने भी एक समस्या थी कि उन्हें क्रोधियों को क्षमा ममभानी थी, अतः क्षमा को भी क्रोध के माध्यम से समझाना पड़ा । व्यवहारी को व्यवहार की भाषा में समझाना पड़ता है । मुनिजन क्षमा के भंडार होते हैं । यदि वे अपनी ओर से बोलेंगे तो यही बोलेंगे कि क्षमा का प्रभाव क्रोध है, पर दुनियाँ में भाव होता है वक्ता का और भाषा होती है श्रोता की । यदि श्रोता की भाषा में न बोला गया तो वह कुछ समझ ही न सकेगा ।
अतः ज्ञानीजन समझाना तो चाहते हैं क्षमाधर्म, पर समझाते हैं क्रोध की बात करके । बच्चों से बात करने के लिए उनकी ओर से बोलना पड़ता है । जब हम बच्चे से कहते हैं कि माँ को बुलाना, तब हमारा आशय बच्चों की माँ से होता है, अपनी माँ से नहीं; क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसा कहने पर बच्चा अपनी माँ को ही बुलायेगा, हमारी माँ को नहीं ।
इसीप्रकार जब हमें भी क्षमा को क्रोध की भाषा में ही समझाना है तो पहिले क्रोध को ही अच्छी तरह स्पष्ट करना समुचित होगा ।
यद्यपि यह आत्मा ज्ञान का घनपिण्ड और आनन्द का कन्द है, स्वभाव से स्वयं परिपूर्ण है; तथापि कुछ विकृतियाँ, कमजोरियाँ तब से ही इसके साथ जुड़ी हुई हैं, जब से यह है । उन कमजोरियों को शास्त्रकारों ने विभाव कहा, कषाय कहा, और न जाने क्या-क्या नाम दिये; उनके त्याग का उपदेश भी कम नहीं दिया; सच्चे सुख को प्राप्त करने का उपाय भी उनके त्याग को ही बताया ।