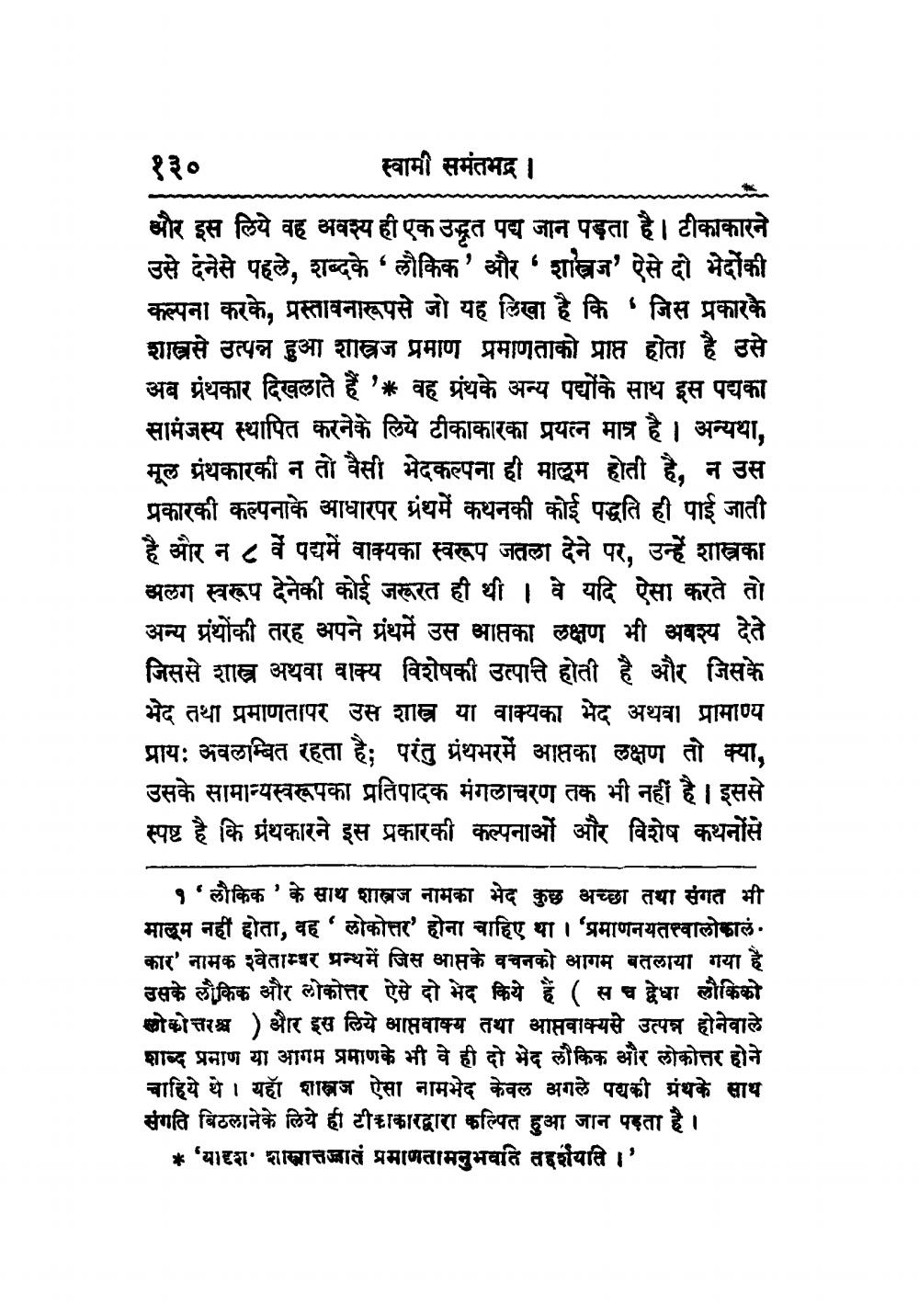________________
१३०
स्वामी समंतभद्र।
और इस लिये वह अवश्य ही एक उद्धृत पद्य जान पड़ता है। टीकाकारने उसे देनेसे पहले, शब्दके 'लौकिक' और 'शास्त्रज' ऐसे दो भेदोंकी कल्पना करके, प्रस्तावनारूपसे जो यह लिखा है कि जिस प्रकारके शास्त्रसे उत्पन्न हुआ शास्त्रज प्रमाण प्रमाणताको प्राप्त होता है उसे अब ग्रंथकार दिखलाते हैं '* वह ग्रंथके अन्य पद्योंके साथ इस पद्यका सामंजस्य स्थापित करनेके लिये टीकाकारका प्रयत्न मात्र है। अन्यथा, मूल ग्रंथकारकी न तो वैसी भेदकल्पना ही मालूम होती है, न उस प्रकारकी कल्पनाके आधारपर ग्रंथमें कथनकी कोई पद्धति ही पाई जाती है और न ८ वें पद्यमें वाक्यका स्वरूप जतला देने पर, उन्हें शास्त्रका अलग स्वरूप देनेकी कोई जरूरत ही थी । वे यदि ऐसा करते तो अन्य ग्रंथोंकी तरह अपने ग्रंथमें उस आप्तका लक्षण भी अवश्य देते जिससे शास्त्र अथवा वाक्य विशेषकी उत्पत्ति होती है और जिसके भेद तथा प्रमाणतापर उस शास्त्र या वाक्यका भेद अथवा प्रामाण्य प्रायः अवलम्बित रहता है; परंतु ग्रंथभरमें आप्तका लक्षण तो क्या, उसके सामान्यस्वरूपका प्रतिपादक मंगलाचरण तक भी नहीं है। इससे स्पष्ट है कि ग्रंथकारने इस प्रकारकी कल्पनाओं और विशेष कथनोंसे
'लौकिक ' के साथ शास्त्रज नामका भेद कुछ अच्छा तथा संगत भी मालूम नहीं होता, वह 'लोकोत्तर' होना चाहिए था। 'प्रमाणनयतत्त्वालोकालं. कार' नामक श्वेताम्बर प्रन्थमें जिस आप्तके वचनको आगम बतलाया गया है उसके लौकिक और लोकोत्तर ऐसे दो भेद किये हैं ( स च द्वेधा लौकिको लोकोत्तरश्च ) और इस लिये आप्तवाक्य तथा आप्तवाक्यसे उत्पन्न होनेवाले शान्द प्रमाण या आगम प्रमाणके भी वे ही दो भेद लौकिक और लोकोत्तर होने चाहिये थे। यहाँ शास्त्रज ऐसा नामभेद केवल अगले पथकी ग्रंथके साथ संगति बिठलानेके लिये ही टीकाकारद्वारा कल्पित हुआ जान पड़ता है। * 'यादृशः शास्त्रात्तज्जातं प्रमाणतामनुभवति तदर्शयति ।'