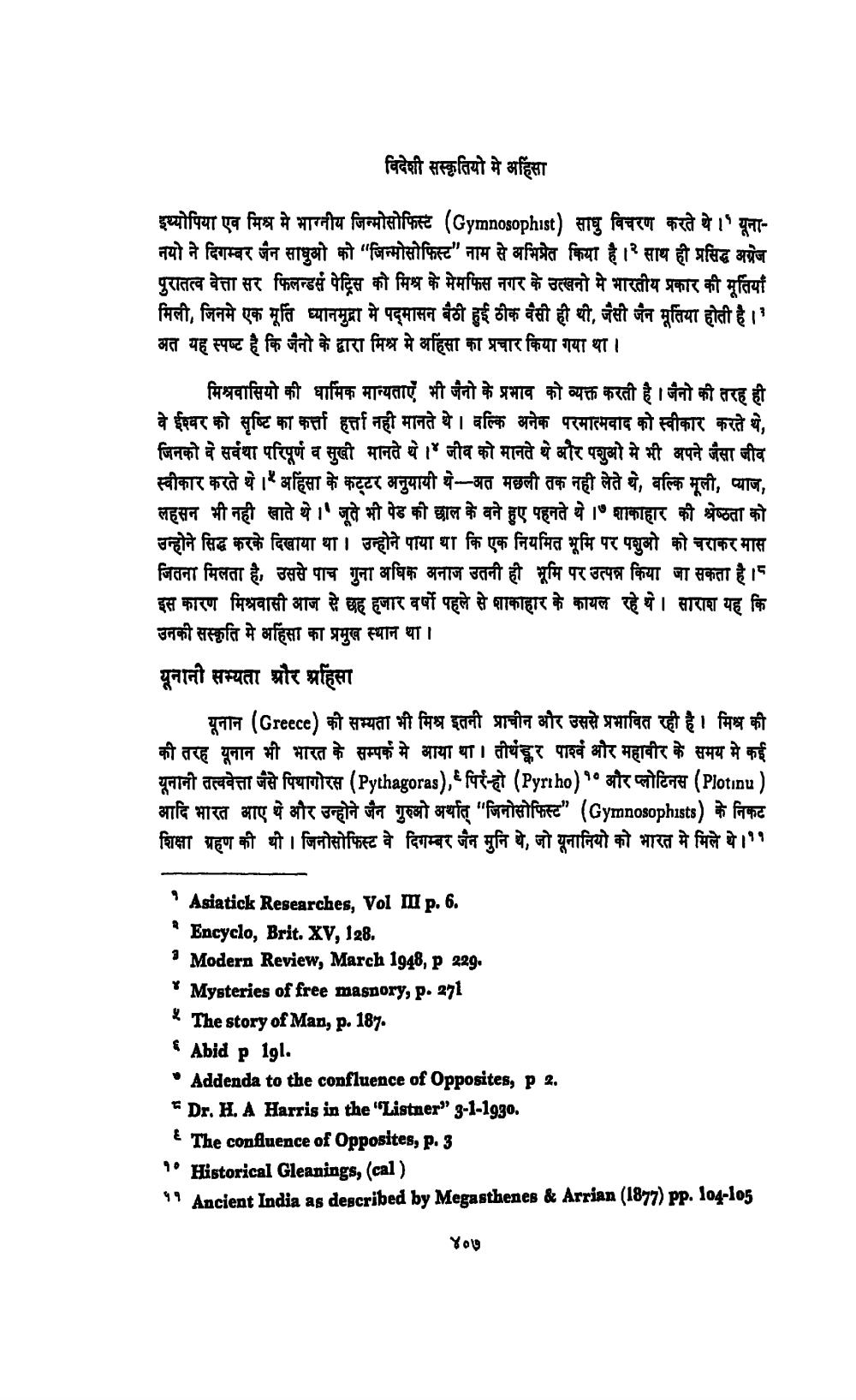________________
विदेशी संस्कृतियो मे अहिंसा
इथ्योपिया एव मिश्र मे भाग्नीय जिन्मोसोफिस्ट (Gymnosophist) साधु विचरण करते थे।' यूनानयो ने दिगम्बर जैन साधुओ को "जिन्मोसोफिस्ट" नाम से अभिप्रेत किया है। साथ ही प्रसिद्ध अग्रेज पुरातत्व वेत्ता सर फिलन्डर्स पेट्रिस को मिश्र के मेमफिस नगर के उत्खनो मे भारतीय प्रकार की मूर्तियां मिली, जिनमे एक मूर्ति ध्यानमुद्रा में पद्मासन बैठी हुई ठीक वैसी ही थी, जैसी जैन मूर्तिया होती है।' अत यह स्पष्ट है कि जैनो के द्वारा मिश्र मे अहिंसा का प्रचार किया गया था।
मिश्रवासियो की धार्मिक मान्यताएँ भी जैनो के प्रभाव को व्यक्त करती है । जैनो की तरह ही वे ईश्वर को सृष्टि का कर्ता हर्ता नहीं मानते थे । बल्कि अनेक परमात्मवाद को स्वीकार करते थे, जिनको वे सर्वथा परिपूर्ण व सुखी मानते थे। जीव को मानते थे और पशुओ मे भी अपने जैसा जीव स्वीकार करते थे । अहिंसा के कट्टर अनुयायी थे--अत मछली तक नहीं लेते थे, बल्कि मूली, प्याज, लहसन भी नहीं खाते थे। जूते भी पेड की छाल के बने हुए पहनते थे । शाकाहार की श्रेष्ठता को उन्होने सिद्ध करके दिखाया था। उन्होने पाया था कि एक नियमित भूमि पर पशुओ को चराकर मास जितना मिलता है, उससे पाच गुना अधिक अनाज उतनी ही भूमि पर उत्पन्न किया जा सकता है। इस कारण मिश्रवासी आज से छह हजार वर्षों पहले से शाकाहार के कायल रहे थे। साराश यह कि उनकी सस्कृति मे अहिंसा का प्रमुख स्थान था। यूनानी सभ्यता और अहिंसा
यूनान (Greece) की सभ्यता भी मिश्र इतनी प्राचीन और उससे प्रभावित रही है। मिश्र की की तरह यूनान भी भारत के सम्पर्क मे आया था। तीर्थकर पावं और महावीर के समय मे कई यूनानी तत्त्ववेत्ता जैसे पिथागोरस (Pythagoras), पिरं-हो (Pyrrho) १० और प्लोटिनस (Plotinu ) आदि भारत आए थे और उन्होने जैन गुरुओ अर्थात् "जिनोसोफिस्ट" (Gymnosophists) के निकट शिक्षा ग्रहण की थी। जिनोसोफिस्ट वे दिगम्बर जैन मुनि थे, जो यूनानियो को भारत मे मिले थे।"
' Asiatick Researches, Vol mp.6.
Encyclo, Brit. XV, 128. . Modern Review, March 1948, p 229.
Mysteries of free masnory, p. 271 " The story of Man, p. 187.
Abid p 19l. •Addenda to the confluence of Opposites, P2. 5 Dr. H. A Harris in the "Listner?" 3-1-1990.
The confluence of Opposites, p. 3 no Historical Gleanings, (cal) 19 Ancient India as described by Megasthenes & Arrian (1877) pp. 104-105
४०७