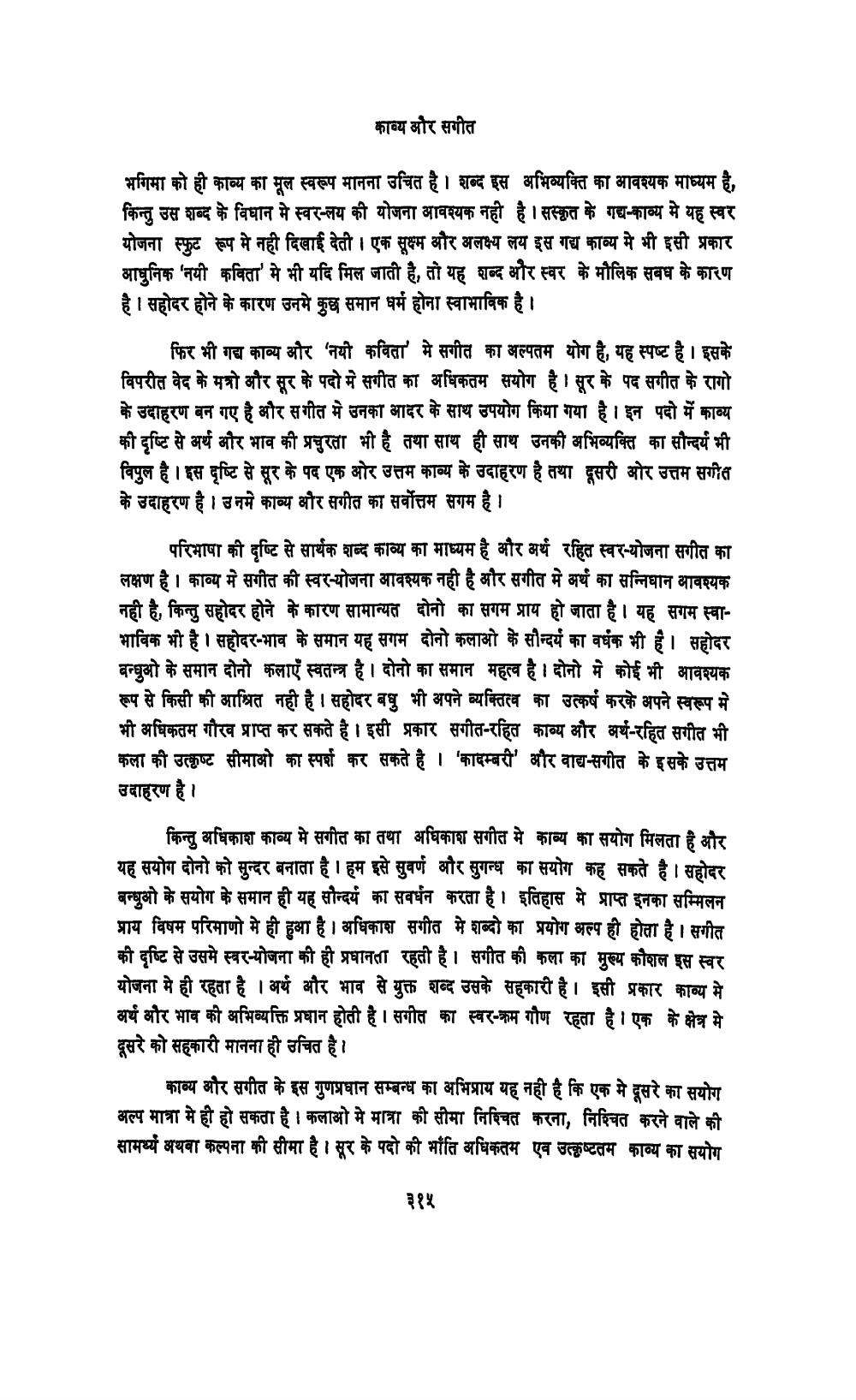________________
काव्य और संगीत
भगिमा को ही काव्य का मूल स्वरूप मानना उचित है। शब्द इस अभिव्यक्ति का आवश्यक माध्यम है, किन्तु उस शब्द के विधान मे स्वर-लय की योजना आवश्यक नहीं है । संस्कृत के गद्य-काव्य मे यह स्वर योजना स्फुट रूप मे नही दिखाई देती । एक सूक्ष्म और अलक्ष्य लय इस गद्य काव्य मे भी इसी प्रकार आधुनिक 'नयी कविता' मे भी यदि मिल जाती है, तो यह शब्द और स्वर के मौलिक सबध के कारण है । सहोदर होने के कारण उनमे कुछ समान धर्म होना स्वाभाविक है।
फिर भी गद्य काव्य और 'नयी कविता' मे सगीत का अल्पतम योग है, यह स्पष्ट है । इसके विपरीत वेद के मत्रो और सूर के पदो मे सगीत का अधिकतम सयोग है । सूर के पद सगीत के रागो के उदाहरण बन गए है और संगीत में उनका आदर के साथ उपयोग किया गया है। इन पदो में काव्य की दृष्टि से अर्थ और भाव की प्रचुरता भी है तथा साथ ही साथ उनकी अभिव्यक्ति का सौन्दर्य भी विपुल है । इस दृष्टि से सूर के पद एक ओर उत्तम काव्य के उदाहरण है तथा दूसरी ओर उत्तम समेत के उदाहरण है। उनमे काव्य और संगीत का सर्वोत्तम सगम है।
परिभाषा की दृष्टि से सार्थक शब्द काव्य का माध्यम है और अर्थ रहित स्वर-योजना सगीत का लक्षण है । काव्य मे सगीत की स्वर-योजना आवश्यक नहीं है और संगीत में अर्थ का सन्निधान आवश्यक नहीं है, किन्तु सहोदर होने के कारण सामान्यत दोनो का सगम प्राय हो जाता है। यह सगम स्वाभाविक भी है । सहोदर-भाव के समान यह सगम दोनो कलाओ के सौन्दर्य का वर्धक भी है। सहोदर बन्धुओ के समान दोनो कलाएं स्वतन्त्र है। दोनो का समान महत्व है। दोनो मे कोई भी आवश्यक रूप से किसी की आश्रित नही है । सहोदर बधु भी अपने व्यक्तित्व का उत्कर्ष करके अपने स्वरूप में भी अधिकतम गौरव प्राप्त कर सकते है। इसी प्रकार सगीत-रहित काव्य और अर्थ-रहित सगीत भी कला की उत्कृष्ट सीमाओ का स्पर्श कर सकते है । 'कादम्बरी' और वाद्य-सगीत के इसके उत्तम उदाहरण है।
किन्तु अधिकाश काव्य मे सगीत का तथा अधिकाश सगीत मे काव्य का सयोग मिलता है और यह सयोग दोनो को सुन्दर बनाता है । हम इसे सुवर्ण और सुगन्ध का सयोग कह सकते है । सहोदर बन्धुओ के सयोग के समान ही यह सौन्दर्य का सवर्धन करता है। इतिहास में प्राप्त इनका सम्मिलन प्राय विषम परिमाणो मे ही हुआ है । अधिकाश सगीत मे शब्दो का प्रयोग अल्प ही होता है । सगीत की दृष्टि से उसमे स्वर-योजना की ही प्रधानता रहती है। सगीत की कला का मुख्य कौशल इस स्वर योजना मे ही रहता है । अर्थ और भाव से युक्त शब्द उसके सहकारी है। इसी प्रकार काव्य मे अर्थ और भाव को अभिव्यक्ति प्रधान होती है । सगीत का स्वर-क्रम गौण रहता है । एक के क्षेत्र मे दूसरे को सहकारी मानना ही उचित है।
काव्य और संगीत के इस गुणप्रधान सम्बन्ध का अभिप्राय यह नहीं है कि एक मे दूसरे का सयोग अल्प मात्रा मे ही हो सकता है । कलाओ मे मात्रा की सीमा निश्चित करना, निश्चित करने वाले की सामर्थ्य अथवा कल्पना की सीमा है । सूर के पदो की भांति अधिकतम एव उत्कृष्टतम काव्य का सयोग
३१५