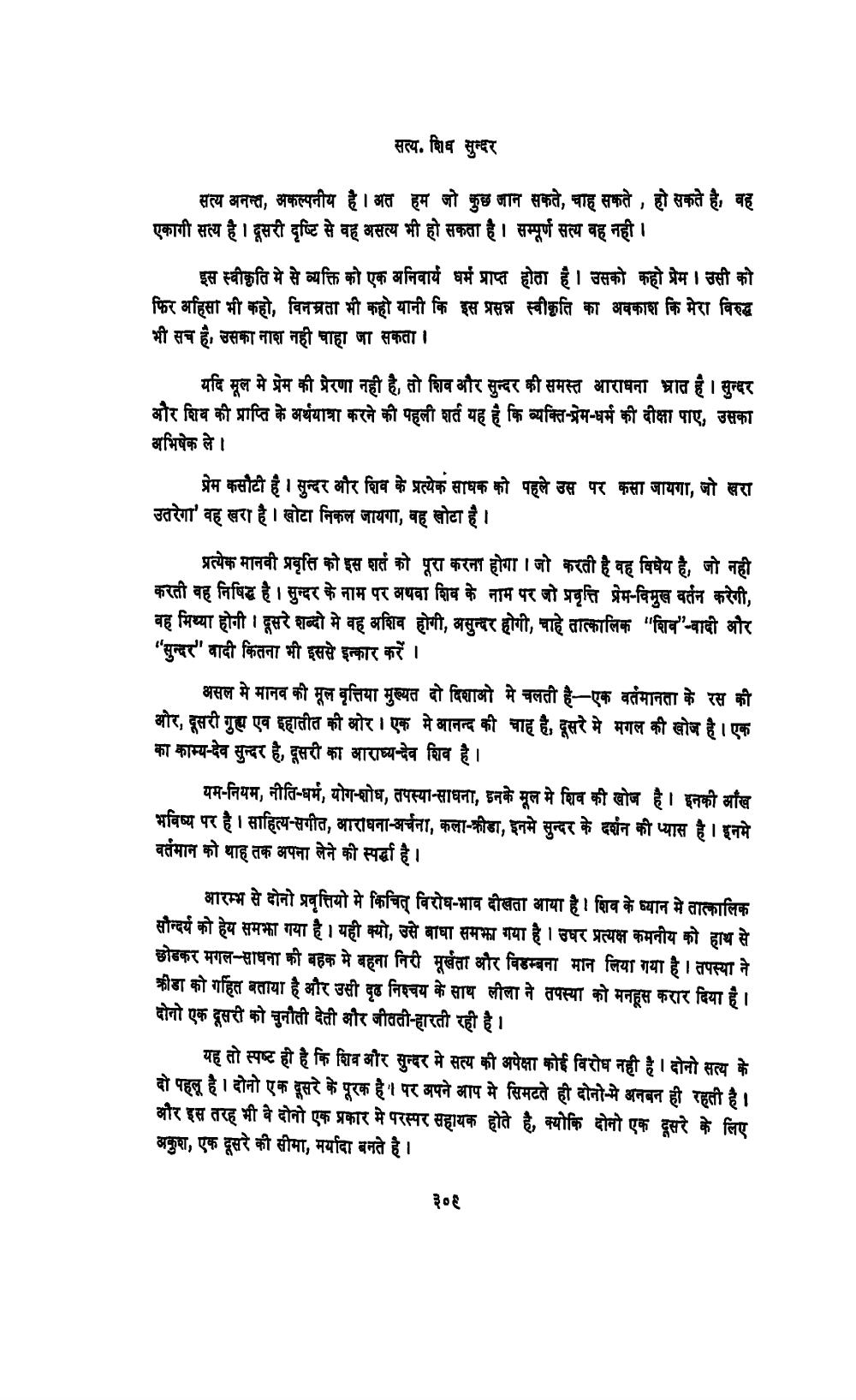________________
सत्य. शिष सुन्दर
सत्य अनन्त, अकल्पनीय है । अत हम जो कुछ जान सकते, चाह सकते , हो सकते है, वह एकागी सत्य है । दूसरी दृष्टि से वह असत्य भी हो सकता है। सम्पूर्ण सत्य वह नहीं । ___इस स्वीकृति मे से व्यक्ति को एक अनिवार्य धर्म प्राप्त होता है । उसको कहो प्रेम । उसी को फिर अहिसा भी कहो, विनम्रता भी कहो यानी कि इस प्रसन्न स्वीकृति का अवकाश कि मेरा विरुद्ध भी सच है। उसका नाश नहीं चाहा जा सकता।
यदि मूल मे प्रेम की प्रेरणा नहीं है, तो शिव और सुन्दर की समस्त आराधना भ्रात है । सुन्दर और शिव की प्राप्ति के अर्थयात्रा करने की पहली शर्त यह है कि व्यक्ति-प्रेम-धर्म की दीक्षा पाए, उसका अभिषेक ले।
प्रेम कसौटी है । सुन्दर और शिव के प्रत्येक साधक को पहले उस पर कसा जायगा, जो खरा उतरेगा' वह खरा है । खोटा निकल जायगा, वह खोटा है।
प्रत्येक मानवी प्रवृत्ति को इस शर्त को पूरा करना होगा । जो करती है वह विधेय है, जो नही करती वह निषिद्ध है । सुन्दर के नाम पर अथवा शिव के नाम पर जो प्रवृत्ति प्रेम-विमुख वर्तन करेगी, वह मिथ्या होगी । दूसरे शब्दो मे वह अशिव होगी, असुन्दर होगी, चाहे तात्कालिक "शिव"-वादी और "सुन्दर" वादी कितना भी इससे इन्कार करें।
असल मे मानव की मूल वृत्तिया मुख्यत दो दिशाओ मे चलती है-एक वर्तमानता के रस की ओर, दूसरी गुह्य एव इहातीत की ओर । एक मे आनन्द की चाह है, दूसरे मे मगल की खोज है । एक का काम्य-देव सुन्दर है, दूसरी का आराध्य देव शिव है।
यम-नियम, नीति-धर्म, योग-शोध, तपस्या-साधना, इनके मूल मे शिव की खोज है। इनकी आँख भविष्य पर है । साहित्य-सगीत, आराधना-अर्चना, कला-क्रीडा, इनमे सुन्दर के दर्शन की प्यास है। इनमे वर्तमान को थाह तक अपना लेने की स्पर्धा है।
आरम्भ से दोनो प्रवृत्तियो मे किचित् विरोध-भाव दीखता आया है। शिव के ध्यान मे तात्कालिक सौन्दर्य को हेय समझा गया है। यही क्यो, उसे बाघा समझा गया है । उधर प्रत्यक्ष कमनीय को हाथ से छोडकर मगल-साधना की बहक मे बहना निरी मूर्खता और विडम्बना मान लिया गया है । तपस्या ने क्रीडा को गहित बताया है और उसी दृढ निश्चय के साथ लीला ने तपस्या को मनहूस करार दिया है। दोनो एक दूसरी को चुनौती देती और जीतती-हारती रही है।
यह तो स्पष्ट ही है कि शिव और सुन्दर मे सत्य की अपेक्षा कोई विरोध नही है । दोनो सत्य के दो पहलू है । दोनो एक दूसरे के पूरक है । पर अपने आप मे सिमटते ही दोनो-मे अनबन ही रहती है। और इस तरह भी वे दोनो एक प्रकार मे परस्पर सहायक होते है, क्योकि दोनो एक दूसरे के लिए अकुश, एक दूसरे की सीमा, मर्यादा बनते है।
३०९