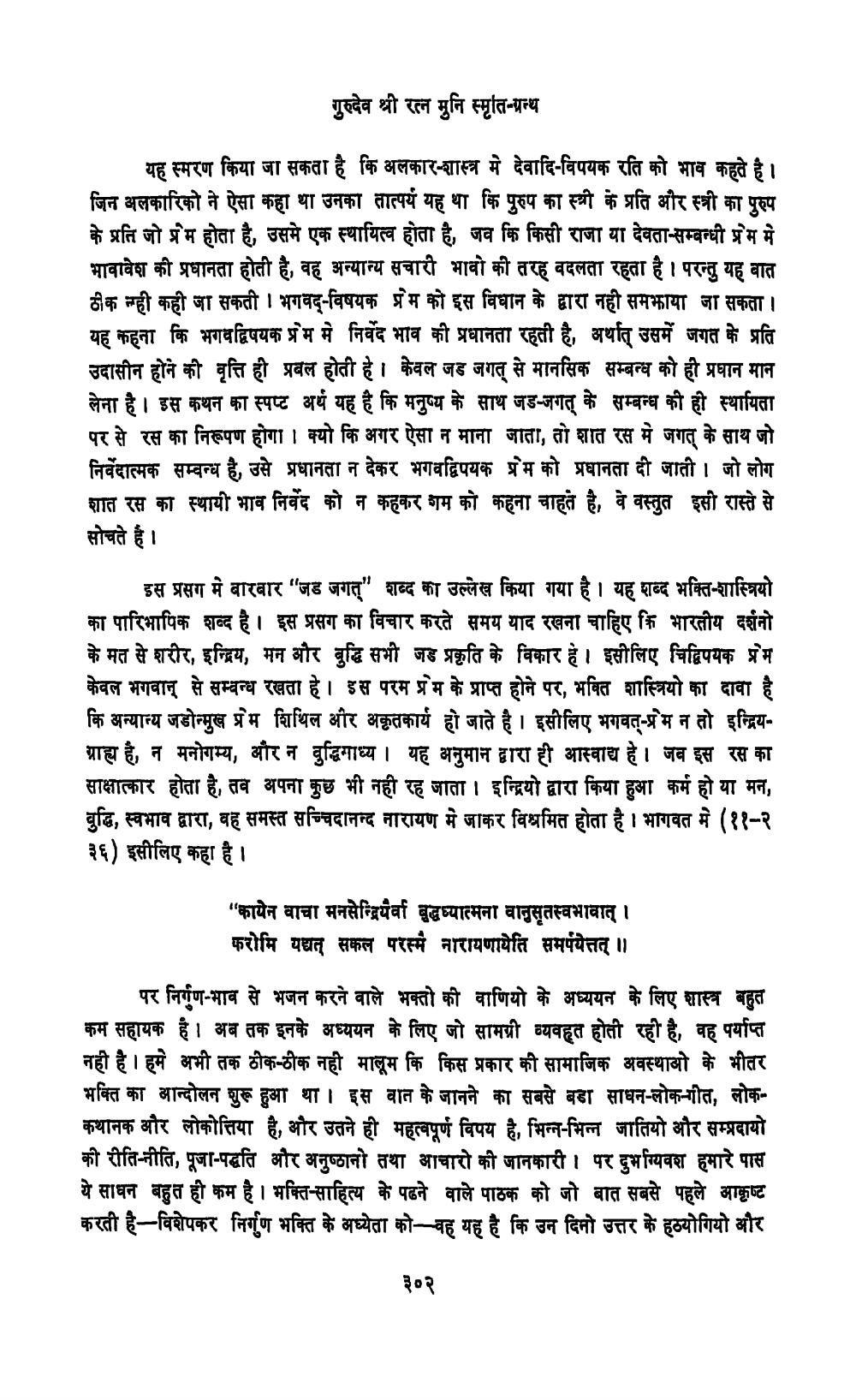________________
गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्थ
यह स्मरण किया जा सकता है कि अलकार-शास्त्र में देवादि-विपयक रति को भाव कहते है। जिन अलकारिको ने ऐसा कहा था उनका तात्पर्य यह था कि पुरुप का स्त्री के प्रति और स्त्री का पुरुप के प्रति जो प्रेम होता है, उसमे एक स्थायित्व होता है, जव कि किसी राजा या देवता-सम्बन्धी प्रेम में भावावेश की प्रधानता होती है, वह अन्यान्य सचारी भावो की तरह बदलता रहता है । परन्तु यह बात ठीक नही कही जा सकती । भगवद्-विषयक प्रेम को इस विधान के द्वारा नही समझाया जा सकता। यह कहना कि भगवद्विषयक प्रेम मे निर्वेद भाव की प्रधानता रहती है, अर्थात् उसमें जगत के प्रति उदासीन होने की वृत्ति ही प्रबल होती है। केवल जड जगत् से मानसिक सम्बन्ध को ही प्रधान मान लेना है। इस कथन का स्पप्ट अर्थ यह है कि मनुष्य के साथ जड-जगत् के सम्बन्ध की ही स्थायिता पर से रस का निरूपण होगा। क्यो कि अगर ऐसा न माना जाता, तो शात रस में जगत् के साथ जो निर्वेदात्मक सम्बन्ध है, उसे प्रधानता न देकर भगवद्विपयक प्रेम को प्रधानता दी जाती। जो लोग शात रस का स्थायी भाव निर्वेद को न कहकर गम को कहना चाहते है, वे वस्तुत इसी रास्ते से सोचते है।
इस प्रसग में बारवार "जड जगत्" शब्द का उल्लेख किया गया है। यह शब्द भक्ति-शास्त्रियो का पारिभाषिक शब्द है। इस प्रसग का विचार करते समय याद रखना चाहिए कि भारतीय दर्शनो के मत से शरीर, इन्द्रिय, मन और बुद्धि सभी जड प्रकृति के विकार है। इसीलिए चिद्विपयक प्रेम केवल भगवान् से सम्बन्ध रखता है। इस परम प्रेम के प्राप्त होने पर, भक्ति शास्त्रियो का दावा है कि अन्यान्य जडोन्मुख प्रेम शिथिल और अकृतकार्य हो जाते है। इसीलिए भगवत्-प्रम न तो इन्द्रियग्राह्य है, न मनोगम्य, और न बुद्धिगाध्य । यह अनुमान द्वारा ही आस्वाद्य हे। जव इस रस का साक्षात्कार होता है, तब अपना कुछ भी नहीं रह जाता। इन्द्रियो द्वारा किया हुआ कर्म हो या मन, बुद्धि, स्वभाव द्वारा, वह समस्त सच्चिदानन्द नारायण में जाकर विश्रमित होता है । भागवत में (११-२ ३६) इसीलिए कहा है।
"कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्धध्यात्मना वानुसृतस्वभावात् ।
फरोमि यद्यत् सफल परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्तत् । पर निर्गुण-भाव से भजन करने वाले भक्तो की वाणियो के अध्ययन के लिए शास्त्र बहुत कम सहायक है। अब तक इनके अध्ययन के लिए जो सामग्री व्यवहृत होती रही है, वह पर्याप्त नही है । हमे अभी तक ठीक-ठीक नहीं मालूम कि किस प्रकार की सामाजिक अवस्थाओ के भीतर भक्ति का आन्दोलन शुरू हुआ था। इस बात के जानने का सबसे बड़ा साधन-लोक-गीत, लोककथानक और लोकोत्तिया है, और उतने ही महत्वपूर्ण विषय है, भिन्न-भिन्न जातियो और सम्प्रदायो की रीति-नीति, पूजा-पद्धति और अनुष्ठानो तथा आचारो की जानकारी। पर दुर्भाग्यवश हमारे पास ये साधन बहुत ही कम है । भक्ति-साहित्य के पढने वाले पाठक को जो बात सबसे पहले आकृष्ट करती है-विशेषकर निर्गुण भक्ति के अध्येता को-वह यह है कि उन दिनो उत्तर के हठयोगियो और
३०२