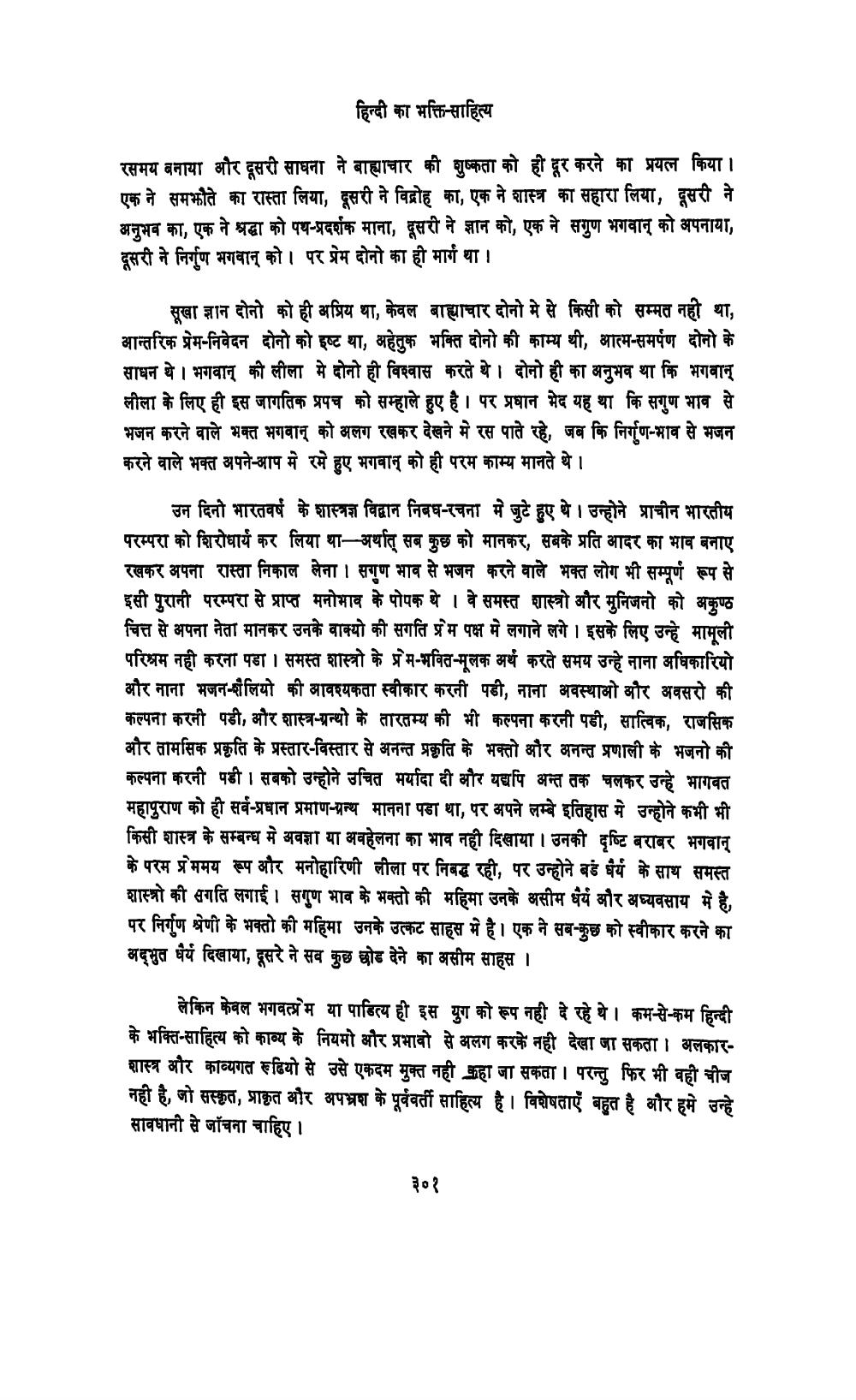________________
हिन्दी का भक्ति-साहित्य
रसमय बनाया और दूसरी साधना ने बाह्याचार की शुष्कता को ही दूर करने का प्रयल किया। एक ने समझौते का रास्ता लिया, दूसरी ने विद्रोह का, एक ने शास्त्र का सहारा लिया, दूसरी ने अनुभव का, एक ने श्रद्धा को पथ-प्रदर्शक माना, दूसरी ने ज्ञान को, एक ने सगुण भगवान् को अपनाया, दूसरी ने निर्गुण भगवान् को। पर प्रेम दोनो का ही मार्ग था।
सूखा ज्ञान दोनो को ही अप्रिय था, केवल बाह्याचार दोनो मे से किसी को सम्मत नही था, आन्तरिक प्रेम-निवेदन दोनो को इष्ट था, अहेतुक भक्ति दोनो की काम्य थी, आत्म-समर्पण दोनो के साधन थे। भगवान् की लीला मे दोनो ही विश्वास करते थे। दोनो ही का अनुभव था कि भगवान् लीला के लिए ही इस जागतिक प्रपच को सम्हाले हुए है । पर प्रधान भेद यह था कि सगुण भाव से भजन करने वाले भक्त भगवान् को अलग रखकर देखने मे रस पाते रहे, जब कि निर्गुण-भाव से भजन करने वाले भक्त अपने-आप मे रमे हुए भगवान् को ही परम काम्य मानते थे।
उन दिनो भारतवर्ष के शास्त्रज्ञ विद्वान निबध-रचना में जुटे हुए थे। उन्होने प्राचीन भारतीय परम्परा को शिरोधार्य कर लिया था—अर्थात् सब कुछ को मानकर, सबके प्रति आदर का भाव बनाए रखकर अपना रास्ता निकाल लेना । सगुण भाव से भजन करने वाले भक्त लोग भी सम्पूर्ण रूप से इसी पुरानी परम्परा से प्राप्त मनोभाव के पोपक थे । वे समस्त शास्त्रो और मुनिजनो को अकुण्ठ चित्त से अपना नेता मानकर उनके वाक्यो की सगति प्रेम पक्ष मे लगाने लगे । इसके लिए उन्हें मामूली परिश्रम नही करना पड़ा । समस्त शास्त्रो के प्रेम-भवित-मूलक अर्थ करते समय उन्हे नाना अधिकारियो और नाना भजन-शैलियो की आवश्यकता स्वीकार करनी पडी, नाना अवस्थाओ और अवसरो की कल्पना करनी पड़ी, और शास्त्र-ग्रन्थो के तारतम्य की भी कल्पना करनी पड़ी, सात्विक, राजसिक और तामसिक प्रकृति के प्रस्तार-विस्तार से अनन्त प्रकृति के भक्तो और अनन्त प्रणाली के भजनो की कल्पना करनी पड़ी। सबको उन्होने उचित मर्यादा दी और यद्यपि अन्त तक चलकर उन्हे भागवत महापुराण को ही सर्व-प्रधान प्रमाण-ग्रन्थ मानना पडा था, पर अपने लम्बे इतिहास में उन्होने कभी भी किसी शास्त्र के सम्बन्ध मे अवज्ञा या अवहेलना का भाव नहीं दिखाया। उनकी दृष्टि बराबर भगवान् के परम प्रेममय रूप और मनोहारिणी लीला पर निबद्ध रही, पर उन्होने बडं धैर्य के साथ समस्त शास्त्रो की संगति लगाई। सगुण भाव के भक्तो की महिमा उनके असीम धैर्य और अध्यवसाय मे है, पर निर्गुण श्रेणी के भक्तो की महिमा उनके उत्कट साहस मे है। एक ने सब-कुछ को स्वीकार करने का अद्भुत धैर्य दिखाया, दूसरे ने सब कुछ छोड देने का असीम साहस ।
लेकिन केवल भगवत्प्रेम या पाडित्य ही इस युग को रूप नही दे रहे थे। कम-से-कम हिन्दी के भक्ति-साहित्य को काव्य के नियमो और प्रभावो से अलग करके नही देखा जा सकता। अलकारशास्त्र और काव्यगत रूढियो से उसे एकदम मुक्त नही कहा जा सकता। परन्तु फिर भी वही चीज नही है, जो सस्कृत, प्राकृत और अपभ्रश के पूर्ववर्ती साहित्य है। विशेषताएँ बहुत है और हमे उन्हे सावधानी से जॉचना चाहिए।
३०१