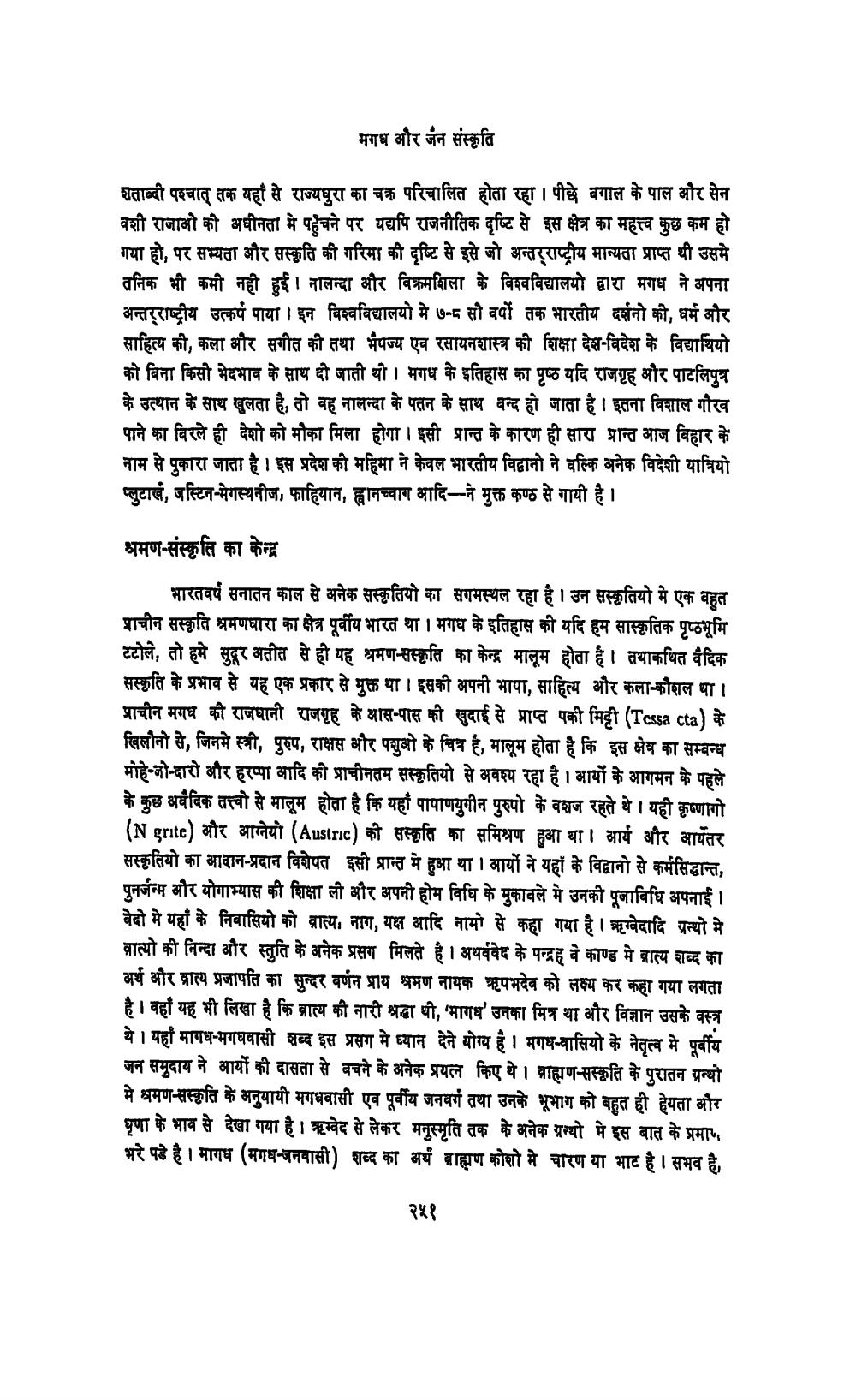________________
मगध और जन संस्कृति
शताब्दी पश्चात् तक यहां से राज्यधुरा का चक्र परिचालित होता रहा । पीछे बगाल के पाल और सेन वशी राजाओ की अधीनता में पहुंचने पर यद्यपि राजनीतिक दृष्टि से इस क्षेत्र का महत्त्व कुछ कम हो गया हो, पर सभ्यता और संस्कृति की गरिमा की दृष्टि से इसे जो अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त थी उसमे तनिक भी कमी नहीं हुई। नालन्दा और विक्रमशिला के विश्वविद्यालयो द्वारा मगध ने अपना अन्तर्राष्ट्रीय उत्कर्ष पाया। इन विश्वविद्यालयो मे ७-८ सौ वर्षों तक भारतीय दर्शनो की, धर्म और साहित्य की, कला और संगीत की तथा भैपज्य एव रसायनशास्त्र की शिक्षा देश-विदेश के विद्याथियो को बिना किसी भेदभाव के साथ दी जाती थी। मगध के इतिहास का पृष्ठ यदि राजगृह और पाटलिपुत्र के उत्थान के साथ खुलता है, तो वह नालन्दा के पतन के साथ बन्द हो जाता है। इतना विशाल गौरव पाने का बिरले ही देशो को मौका मिला होगा। इसी प्रान्त के कारण ही सारा प्रान्त आज बिहार के नाम से पुकारा जाता है । इस प्रदेश की महिमा ने केवल भारतीय विद्वानो ने वल्कि अनेक विदेशी यात्रियो प्लुटार्ख, जस्टिन-मेगस्थनीज, फाहियान, ह्वानच्वाग आदि-ने मुक्त कण्ठ से गायी है।
श्रमण-संस्कृति का केन्द्र
भारतवर्ष सनातन काल से अनेक सस्कृतियो का सगमस्थल रहा है। उन सस्कृतियो मे एक बहुत प्राचीन संस्कृति श्रमणधारा का क्षेत्र पूर्वीय भारत था । मगध के इतिहास की यदि हम सास्कृतिक पृष्ठभूमि टटोले, तो हमे सुदूर अतीत से ही यह श्रमण-सस्कृति का केन्द्र मालूम होता है। तथाकथित वैदिक सस्कृति के प्रभाव से यह एक प्रकार से मुक्त था। इसकी अपनी भापा, साहित्य और कला-कौशल था। प्राचीन मगध की राजधानी राजगृह के आस-पास की खुदाई से प्राप्त पकी मिट्टी (Tessa cta) के खिलौनो से, जिनमे स्त्री, पुरुष, राक्षस और पशुओ के चित्र है, मालूम होता है कि इस क्षेत्र का सम्बन्ध मोहे-जो-दारो और हरप्पा आदि की प्राचीनतम संस्कृतियो से अवश्य रहा है । आर्यों के आगमन के पहले के कुछ अवैदिक तत्त्वो से मालूम होता है कि यहाँ पापाणयुगीन पुरुषो के वशज रहते थे। यही कृष्णागो (N grate) और आग्नेयो (Austric) को सस्कृति का समिश्रण हुआ था। आर्य और आर्यतर सस्कृतियो का आदान-प्रदान विशेपत इसी प्रान्त में हुआ था। आर्यों ने यहाँ के विद्वानो से कर्मसिद्धान्त, पुनर्जन्म और योगाभ्यास की शिक्षा ली और अपनी होम विधि के मुकाबले मे उनकी पूजाविधि अपनाई। वेदो मे यहां के निवासियो को व्रात्य, नाग, यक्ष आदि नामो से कहा गया है । ऋग्वेदादि ग्रन्थो में वात्यो की निन्दा और स्तुति के अनेक प्रसग मिलते है । अथर्ववेद के पन्द्रह वे काण्ड मे वात्य शब्द का अर्थ और वात्य प्रजापति का सुन्दर वर्णन प्राय श्रमण नायक ऋपभदेव को लक्ष्य कर कहा गया लगता है। वहाँ यह भी लिखा है कि व्रात्य की नारी श्रद्धा थी, 'मागध' उनका मित्र था और विज्ञान उसके वस्त्र थे । यहाँ मागध-मगधवासी शब्द इस प्रसग मे ध्यान देने योग्य है । मगध-वासियो के नेतृत्व में पूर्वीय जन समुदाय ने आर्यों की दासता से बचने के अनेक प्रयत्न किए थे। ब्राह्मण-सस्कृति के पुरातन ग्रन्थो मे श्रमण-सस्कृति के अनुयायी मगधवासी एव पूर्वीय जनवर्ग तथा उनके भूभाग को बहुत ही हेयता और घृणा के भाव से देखा गया है । ऋग्वेद से लेकर मनुस्मृति तक के अनेक ग्रन्थो मे इस बात के प्रमा, भरे पडे है । मागध (मगध-जनवासी) शब्द का अर्थ ब्राह्मण कोशो मे चारण या भाट है । सभव है,
२५१