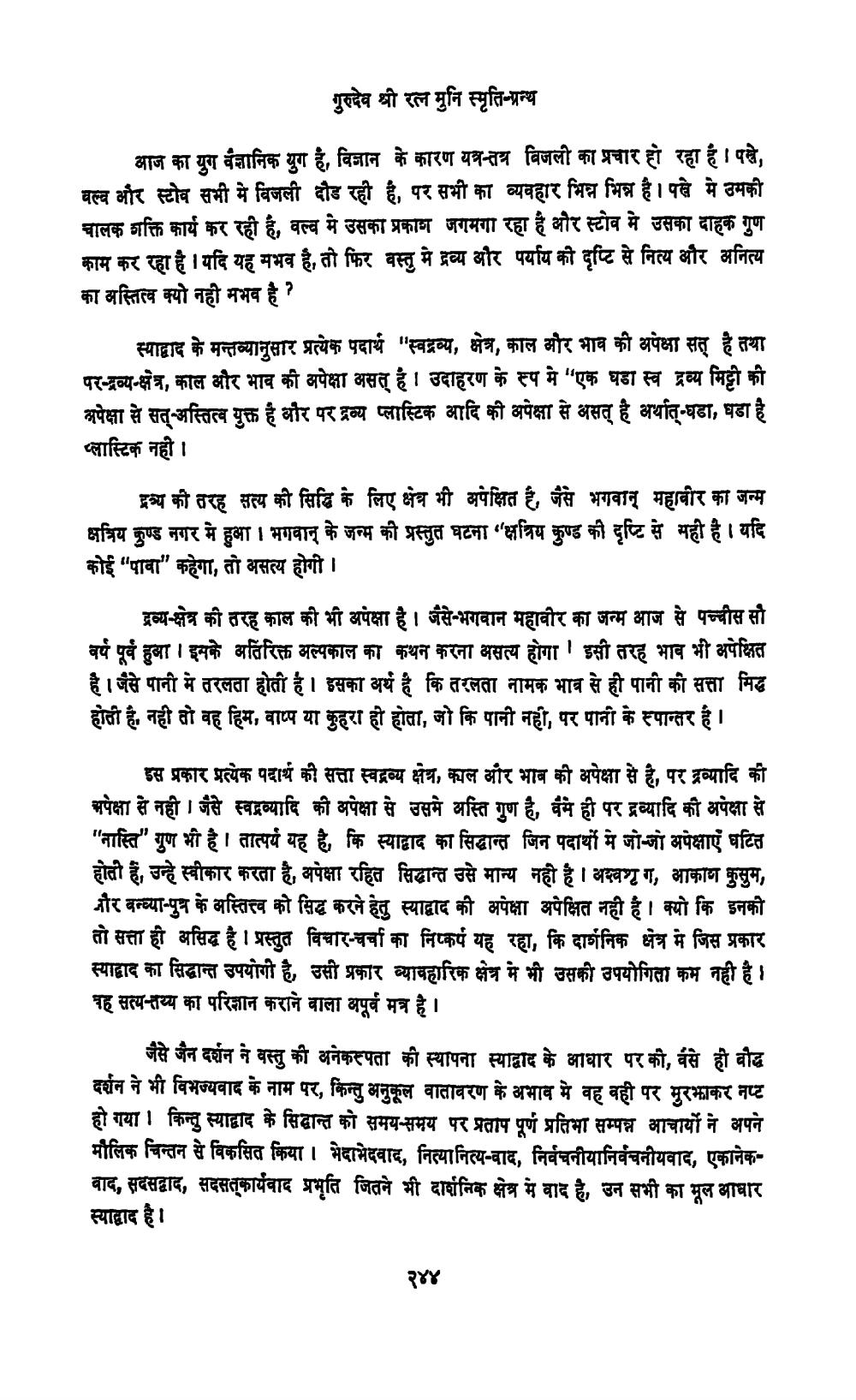________________
गुरुदेव श्री रल मुनि स्मृति-प्रन्थ
आज का युग वैज्ञानिक युग है, विनान के कारण यत्र-तत्र विजली का प्रचार हो रहा है । पखे, वल्व और स्टोव सभी मे विजली दौड रही है, पर सभी का व्यवहार भिन्न भिन्न है। पखे मे उसकी चालक शक्ति कार्य कर रही है, वल्व में उसका प्रकाश जगमगा रहा है और स्टोव में उसका दाहक गुण काम कर रहा है । यदि यह मभव है, तो फिर वस्तु मे द्रव्य और पर्याय की दृष्टि से नित्य और अनित्य का अस्तित्व क्यो नही मभव है?
स्याद्वाद के मन्तव्यानुसार प्रत्येक पदार्थ "स्वद्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा सत् है तथा पर-द्रव्य-क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा असत् है। उदाहरण के रूप में "एक घडा स्व द्रव्य मिट्टी की अपेक्षा से सत्-अस्तित्व युक्त है और पर द्रव्य प्लास्टिक आदि की अपेक्षा से असत् है अर्थात्-घडा, घडा है प्लास्टिक नही।
द्रव्य की तरह सत्य की सिद्धि के लिए क्षेत्र भी अपेक्षित है, जैसे भगवान् महावीर का जन्म भत्रिय कुण्ड नगर मे हुआ । भगवान् के जन्म की प्रस्तुत घटना "क्षत्रिय कुण्ड की दृष्टि से मही है । यदि कोई "पावा" कहेगा, तो असत्य होगी।
द्रव्य-क्षेत्र की तरह काल की भी अपेक्षा है। जैसे-भगवान महावीर का जन्म आज से पच्चीस सौ वर्ष पूर्व हुआ । इसके अतिरिक्त अल्पकाल का कथन करना असत्य होगा। इसी तरह भाव भी अपेक्षित है । जैसे पानी में तरलता होती है। इसका अर्थ है कि तरलता नामक भाव से ही पानी की सत्ता मिद्ध होती है, नहीं तो वह हिम, वाष्प या कुहरा ही होता, जो कि पानी नहीं, पर पानी के स्पान्तर है।
इस प्रकार प्रत्येक पदार्थ की सत्ता स्वद्रव्य क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा से है, पर द्रव्यादि की अपेक्षा से नही । जैसे स्वद्रव्यादि की अपेक्षा से उसमे अस्ति गुण है, वम ही पर द्रव्यादि की अपेक्षा से "नास्ति" गुण भी है । तात्पर्य यह है, कि स्याद्वाद का सिद्धान्त जिन पदार्थों में जो-जो अपेक्षाएं घटित होती हैं, उन्हे स्वीकार करता है, अपेक्षा रहित सिद्धान्त उसे मान्य नहीं है । अश्वशृग, आकाण कुसुम, और बन्च्या-पुत्र के अस्तित्त्व को सिद्ध करने हेतु स्याद्वाद की अपेक्षा अपेक्षित नहीं है। क्यो कि इनको तो सत्ता ही असिद्ध है । प्रस्तुत विचार-चर्चा का निष्कर्ष यह रहा, कि दार्शनिक क्षेत्र में जिस प्रकार स्याद्वाद का सिद्धान्त उपयोगी है, उसी प्रकार व्यावहारिक क्षेत्र में भी उसकी उपयोगिता कम नहीं है। वह सत्य-तथ्य का परिज्ञान कराने वाला अपूर्व मत्र है।
जैसे जैन दर्शन ने वस्तु की अनेकरूपता की स्थापना स्याद्वाद के आधार पर को, वैसे ही बौद्ध दर्शन ने भी विभज्यवाद के नाम पर, किन्तु अनुकूल वातावरण के अभाव मे वह वही पर मुरझाकर नष्ट हो गया। किन्तु स्याद्वाद के सिद्धान्त को समय-समय पर प्रताप पूर्ण प्रतिभा सम्पन्न आचार्यों ने अपने मौलिक चिन्तन से विकसित किया । भेदाभेदवाद, नित्यानित्य-वाद, निर्वचनीयानिर्वचनीयवाद, एकानेकवाद, सदसद्वाद, सदसत्कार्यवाद प्रभृति जितने भी दार्शनिक क्षेत्र में वाद है, उन सभी का मूल आधार स्याद्वाद है।