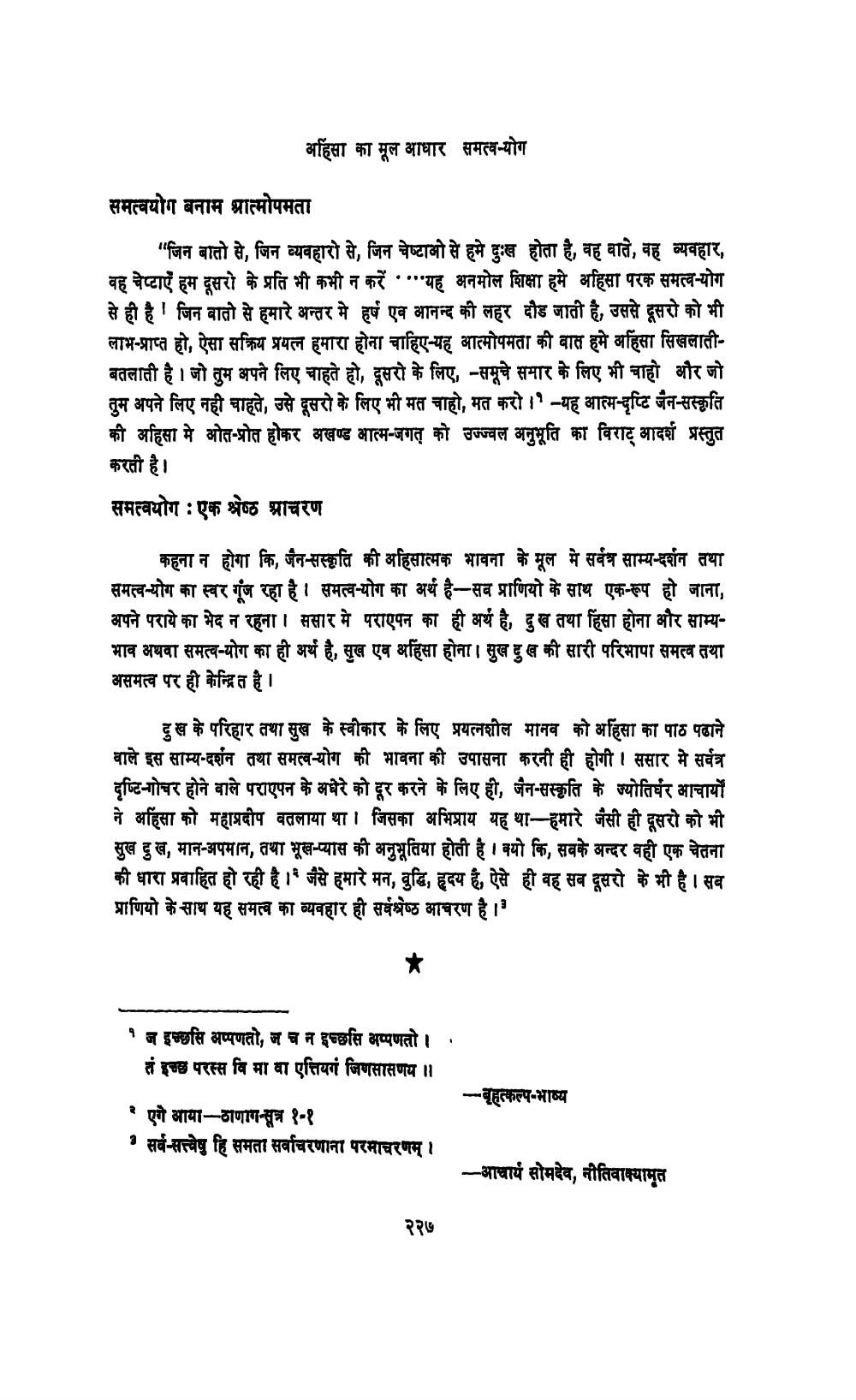________________
अहिंसा का मूल आधार समत्व-योग
समत्वयोग बनाम प्रात्मोपमता
"जिन बातो से, जिन व्यवहारो से, जिन चेष्टाओ से हमे दुःख होता है, वह बाते, वह व्यवहार, वह चेप्टाएँ हम दूसरो के प्रति भी कभी न करें ..""यह अनमोल शिक्षा हमे अहिसा परक समत्व-योग से ही है । जिन बातो से हमारे अन्तर मे हर्ष एव आनन्द की लहर दौड जाती है, उससे दूसरो को भी लाभ-प्राप्त हो, ऐसा सक्रिय प्रयत्ल हमारा होना चाहिए-यह आत्मोपमता की बात हमे अहिंसा सिखलातीबतलाती है । जो तुम अपने लिए चाहते हो, दूसरो के लिए, -समूचे समार के लिए भी चाहो और जो तुम अपने लिए नहीं चाहते, उसे दूसरो के लिए भी मत चाहो, मत करो।' -यह आत्म-दृष्टि जन-संस्कृति की अहिंसा मे ओत-प्रोत होकर अखण्ड आत्म-जगत् को उज्ज्वल अनुभूति का विराट् आदर्श प्रस्तुत करती है। समत्वयोग : एक श्रेष्ठ प्राचरण
कहना न होगा कि, जैन-सस्कृति की अहिसात्मक भावना के मूल मे सर्वत्र साम्य-दर्शन तथा समत्व-योग का स्वर गूंज रहा है। समत्व-योग का अर्थ है-सब प्राणियो के साथ एक-रूप हो जाना, अपने पराये का भेद न रहना। ससार मे पराएपन का ही अर्थ है, दुख तथा हिंसा होना और साम्यभाव अथवा समत्व-योग का ही अर्थ है, सुख एव अहिंसा होना। सुख दुख की सारी परिभाषा समत्व तथा असमत्व पर ही केन्द्रित है।
दुख के परिहार तथा सुख के स्वीकार के लिए प्रयत्नशील मानव को अहिंसा का पाठ पढाने वाले इस साम्य-दर्शन तथा समत्व-योग की भावना की उपासना करनी ही होगी। ससार मे सर्वत्र दृष्टि-गोचर होने वाले पराएपन के अधेरे को दूर करने के लिए ही, जैन-सस्कृति के ज्योतिर्धर आचार्यों ने अहिंसा को महाप्रदीप बतलाया था। जिसका अभिप्राय यह था-हमारे जैसी ही दूसरो को भी सुख दुःख, मान-अपमान, तथा भूख-प्यास की अनुभूतिया होती है । क्यो कि, सबके अन्दर वही एक चेतना की धारा प्रवाहित हो रही है । जैसे हमारे मन, बुद्धि, हृदय है, ऐसे ही वह सब दूसरो के भी है । सब प्राणियो के साथ यह समत्व का व्यवहार ही सर्वश्रेष्ठ आचरण है।'
'न इच्छसि अप्पणतो, न च न इच्छसि अप्पणतो।। तं इच्छ परस्स वि मा वा एत्तियगं जिगसासणय ॥
-बृहत्कल्प-भाष्य • एगे आया-आणाग-सूत्र १-१ ३ सर्व-सत्त्वेषु हि समता सर्वाचरणाना परमाचरणम् ।
-आचार्य सोमदेव, नीतिवाक्यामृत
૨૭