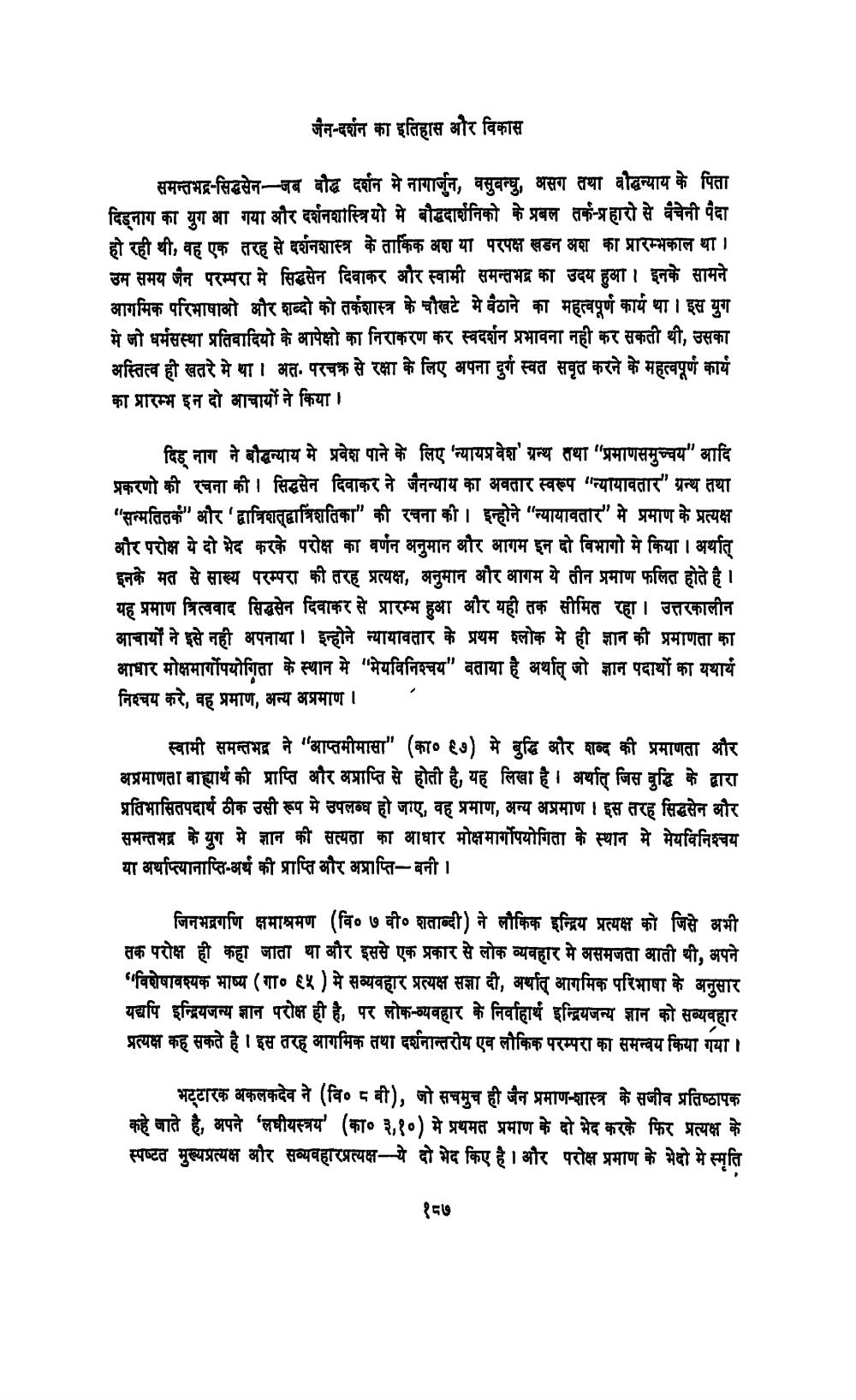________________
जैन-दर्शन का इतिहास और विकास
समन्तभद्र-सिद्धसेन जब बौद्ध दर्शन मे नागार्जुन, वसुबन्धु, असग तथा बौद्धन्याय के पिता दिड्नाग का युग आ गया और दर्शनशास्त्रियो मे बौद्धदार्शनिको के प्रबल तर्क-प्रहारो से बैचेनी पैदा हो रही थी, वह एक तरह से दर्शनशास्त्र के तार्किक अश या परपक्ष खडन अश का प्रारम्भकाल था। उम समय जैन परम्परा मे सिद्धसेन दिवाकर और स्वामी समन्तभद्र का उदय हुआ। इनके सामने आगमिक परिभाषाओ और शब्दो को तर्कशास्त्र के चौखटे मे बैठाने का महत्वपूर्ण कार्य था। इस युग मे जो धर्मसस्था प्रतिवादियो के आपेक्षो का निराकरण कर स्वदर्शन प्रभावना नहीं कर सकती थी, उसका अस्तित्व ही खतरे मे था। अत. परचक्र से रक्षा के लिए अपना दुर्ग स्वत सवृत करने के महत्वपूर्ण कार्य का प्रारम्भ इन दो आचार्यों ने किया।
दिड नाग ने बौद्धन्याय मे प्रवेश पाने के लिए 'न्यायप्रवेश' ग्रन्थ तथा "प्रमाणसमुच्चय" आदि प्रकरणो की रचना की। सिद्धसेन दिवाकर ने जैनन्याय का अवतार स्वरूप "न्यायावतार" ग्रन्थ तथा "सन्मतितर्क" और 'द्वाविशत्वात्रिंशतिका" की रचना की। इन्होने "न्यायावतार" मे प्रमाण के प्रत्यक्ष और परोक्ष ये दो भेद करके परोक्ष का वर्णन अनुमान और आगम इन दो विभागो मे किया । अर्थात् इनके मत से साख्य परम्परा की तरह प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम ये तीन प्रमाण फलित होते है । यह प्रमाण त्रित्ववाद सिद्धसेन दिवाकर से प्रारम्भ हुआ और यही तक सीमित रहा । उत्तरकालीन आचायों ने इसे नहीं अपनाया। इन्होने न्यायावतार के प्रथम श्लोक मे ही ज्ञान की प्रमाणता का आधार मोक्षमार्गोपयोगिता के स्थान मे "मेयविनिश्चय" बताया है अर्थात् जो ज्ञान पदार्थों का यथार्य निश्चय करे, वह प्रमाण, अन्य अप्रमाण ।
स्वामी समन्तभद्र ने "आप्तमीमासा" (का० ६७) मे बुद्धि और शब्द की प्रमाणता और अप्रमाणता बाह्यार्थ की प्राप्ति और अप्राप्ति से होती है, यह लिखा है। अर्थात् जिस बुद्धि के द्वारा प्रतिभासितपदार्थ ठीक उसी रूप में उपलब्ध हो जाए, वह प्रमाण, अन्य अप्रमाण । इस तरह सिद्धसेन और समन्तभद्र के युग मे ज्ञान की सत्यता का आधार मोक्षमार्गोपयोगिता के स्थान में मेयविनिश्चय या अप्त्यिानाप्ति-अर्थ की प्राप्ति और अप्राप्ति-बनी ।
जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण (वि० ७ वी० शताब्दी) ने लौकिक इन्द्रिय प्रत्यक्ष को जिसे अभी तक परोक्ष ही कहा जाता था और इससे एक प्रकार से लोक व्यवहार मे असमजता आती थी, अपने "विशेषावश्यक भाष्य (गा० ६५ ) मे सव्यवहार प्रत्यक्ष सज्ञा दी, अर्थात् आगमिक परिभाषा के अनुसार यद्यपि इन्द्रियजन्य ज्ञान परोक्ष ही है, पर लोक-व्यवहार के निर्वाहार्थ इन्द्रियजन्य ज्ञान को सव्यवहार प्रत्यक्ष कह सकते है । इस तरह आगमिक तथा दर्शनान्तरोय एव लौकिक परम्परा का समन्वय किया गया।
भट्टारक अकलकदेव ने (वि० ८ वी), जो सचमुच ही जैन प्रमाण-शास्त्र के सजीव प्रतिष्ठापक कहे जाते है, अपने 'लघीयस्त्रय' (का० ३,१०) मे प्रथमत प्रमाण के दो भेद करके फिर प्रत्यक्ष के स्पष्टत मुख्यप्रत्यक्ष और सव्यवहारप्रत्यक्ष-ये दो भेद किए है । और परोक्ष प्रमाण के भेदो मे स्मृति
१८७