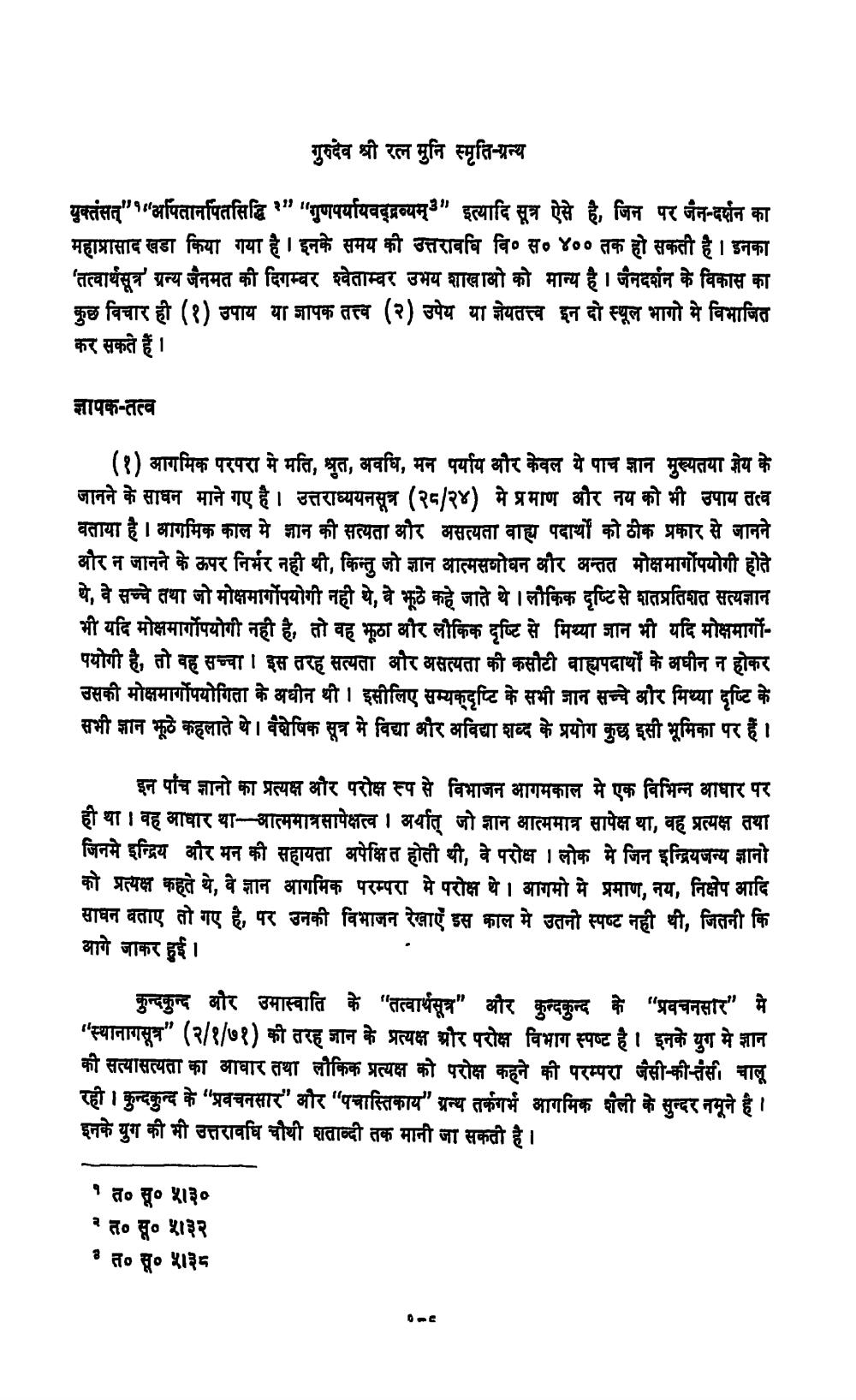________________
गुरुदेव श्री रल मुनि स्मृति-ग्रन्थ
युक्तंसत्" "अपितानपितसिद्धि " "गुणपर्यायवद्रव्यम्" इत्यादि सूत्र ऐसे है, जिन पर जैन-दर्शन का महाप्रासाद खडा किया गया है । इनके समय की उत्तरावधि वि० स० ४०० तक हो सकती है । इनका 'तत्वार्थसूत्र' ग्रन्य जैनमत की दिगम्बर श्वेताम्बर उभय शाखाओ को मान्य है । जैनदर्शन के विकास का कुछ विचार ही (१) उपाय या जापक तत्त्व (२) उपेय या ज्ञेयतत्त्व इन दो स्थूल भागो मे विभाजित कर सकते हैं।
ज्ञापक-तत्व
(१) आगमिक परपरा मे मति, श्रुत, अवधि, मन पर्याय और केवल ये पाच ज्ञान मुख्यतया ज्ञेय के जानने के साधन माने गए है। उत्तराध्ययनसूत्र (२०/२४) मे प्रमाण और नय को भी उपाय तत्व बताया है । आगमिक काल मे ज्ञान की सत्यता और असत्यता वाह्य पदार्थों को ठीक प्रकार से जानने और न जानने के ऊपर निर्भर नही थी, किन्तु जो ज्ञान आत्मसगोधन और अन्तत मोक्षमार्गोपयोगी होते थे, वे सच्चे तथा जो मोक्षमार्गोपयोगी नही थे, वे झूठे कहे जाते थे । लौकिक दृष्टि से शतप्रतिशत सत्यज्ञान भी यदि मोक्षमार्गोपयोगी नही है, तो वह झूठा और लौकिक दृष्टि से मिथ्या ज्ञान भी यदि मोक्षमार्गोपयोगी है, तो वह सच्चा । इस तरह सत्यता और असत्यता की कसौटी वाह्यपदार्थों के अधीन न होकर उसकी मोक्षमार्गोपयोगिता के अधीन थी । इसीलिए सम्यक्दृष्टि के सभी जान सच्चे और मिथ्या दृष्टि के सभी ज्ञान झूठे कहलाते थे। वैशेषिक सूत्र में विद्या और अविद्या शब्द के प्रयोग कुछ इसी भूमिका पर हैं।
इन पांच ज्ञानो का प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से विभाजन आगमकाल मे एक विभिन्न आधार पर ही था । वह आधार था आत्ममात्रसापेक्षत्व । अर्थात् जो ज्ञान आत्ममात्र सापेक्ष था, वह प्रत्यक्ष तथा जिनमे इन्द्रिय और मन की सहायता अपेक्षित होती थी, वे परोक्ष । लोक मे जिन इन्द्रियजन्य ज्ञानो को प्रत्यक्ष कहते थे, वे ज्ञान आगमिक परम्परा मे परोक्ष थे। आगमो मे प्रमाण, नय, निक्षेप आदि साधन बताए तो गए है, पर उनकी विभाजन रेखाएं इस काल मे उतनी स्पष्ट नही थी, जितनी कि आगे जाकर हुई।
कुन्दकुन्द और उमास्वाति के "तत्वार्थसूत्र" और कुन्दकुन्द के "प्रवचनसार" मे "स्थानागसूत्र" (२/१/७१) की तरह जान के प्रत्यक्ष और परोक्ष विभाग स्पष्ट है । इनके युग मे ज्ञान की सत्यासत्यता का आधार तथा लौकिक प्रत्यक्ष को परोक्ष कहने की परम्परा जैसी-की-सी चालू रही । कुन्दकुन्द के "प्रवचनसार" और "पचास्तिकाय" ग्रन्थ तर्कगर्भ आगमिक शैली के सुन्दर नमूने है । इनके युग की भी उत्तरावधि चौथी शताब्दी तक मानी जा सकती है।
'त० सू० ५।३०
त० सू० ॥३२ त० सू० ५।३८