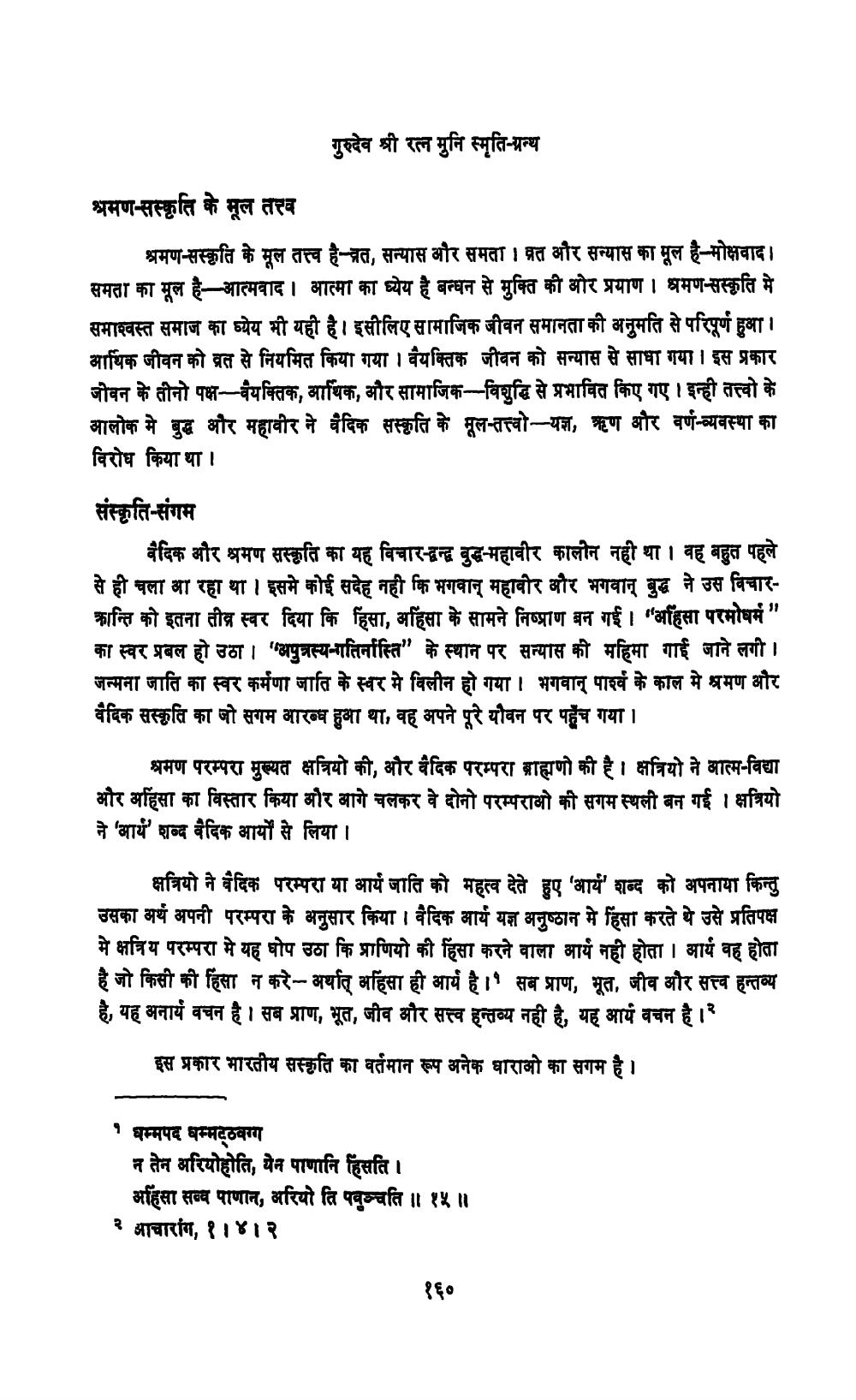________________
गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्थ
श्रमण-सस्कृति के मूल तत्त्व
श्रमण-सस्कृति के मूल तत्त्व है-व्रत, सन्यास और समता । व्रत और सन्यास का मूल है-मोक्षवाद। समता का मूल है-आत्मवाद । आत्मा का ध्येय है बन्धन से मुक्ति की ओर प्रयाण । श्रमण-सस्कृति में समाश्वस्त समाज का ध्येय भी यही है। इसीलिए सामाजिक जीवन समानता की अनुमति से परिपूर्ण हुआ। आर्थिक जीवन को व्रत से नियमित किया गया । वैयक्तिक जीवन को सन्यास से साधा गया। इस प्रकार जीवन के तीनो पक्ष-वैयक्तिक, आर्थिक, और सामाजिक-विशुद्धि से प्रभावित किए गए। इन्ही तत्वो के आलोक मे बुद्ध और महावीर ने वैदिक संस्कृति के मूल-तत्त्वो-यज्ञ, ऋण और वर्ण-व्यवस्था का विरोध किया था। संस्कृति-संगम
वैदिक और श्रमण संस्कृति का यह विचार-द्वन्द्व बुद्ध-महावीर कालीन नही था । वह बहुत पहले से ही चला आ रहा था। इसमे कोई सदेह नही कि भगवान् महावीर और भगवान् बुद्ध ने उस विचारक्रान्ति को इतना तीव्र स्वर दिया कि हिंसा, अहिंसा के सामने निष्प्राण बन गई । "अहिंसा परमोधर्म" का स्वर प्रबल हो उठा। "अपुत्रस्य-गति स्ति" के स्थान पर सन्यास की महिमा गाई जाने लगी। जन्मना जाति का स्वर कर्मणा जाति के स्वर में विलीन हो गया। भगवान् पार्श्व के काल मे श्रमण और वैदिक संस्कृति का जो सगम आरब्ध हुआ था, वह अपने पूरे यौवन पर पहुंच गया।
श्रमण परम्परा मुख्यत क्षत्रियो की, और वैदिक परम्परा ब्राह्मणो की है। क्षत्रियो ने आत्म-विद्या और अहिंसा का विस्तार किया और आगे चलकर वे दोनो परम्पराओ की सगम स्थली बन गई । क्षत्रियो ने 'आर्य' शब्द वैदिक आर्यों से लिया।
क्षत्रियो ने वैदिक परम्परा या आर्य जाति को महत्व देते हुए 'आर्य' शब्द को अपनाया किन्तु उसका अर्थ अपनी परम्परा के अनुसार किया। वैदिक आर्य यज्ञ अनुष्ठान मे हिंसा करते थे उसे प्रतिपक्ष मे क्षत्रिय परम्परा मे यह घोप उठा कि प्राणियो की हिंसा करने वाला आर्य नही होता । आर्य वह होता है जो किसी की हिंसा न करे-- अर्थात् अहिंसा ही आर्य है। सब प्राण, भूत, जीव और सत्त्व हन्तव्य है, यह अनार्य वचन है । सब प्राण, भूत, जीव और सत्त्व हन्तव्य नहीं है, यह आर्य वचन है ।'
इस प्रकार भारतीय संस्कृति का वर्तमान रूप अनेक धाराओ का सगम है।
'धम्मपद धम्मट्ठवग्ग न तेन अरियोहोति, येन पाणानि हिंसति ।
अहिंसा सब्व पाणान, अरियो ति पञ्चति ॥ १५ ॥ २ आचारांग, १।४।२
१६०