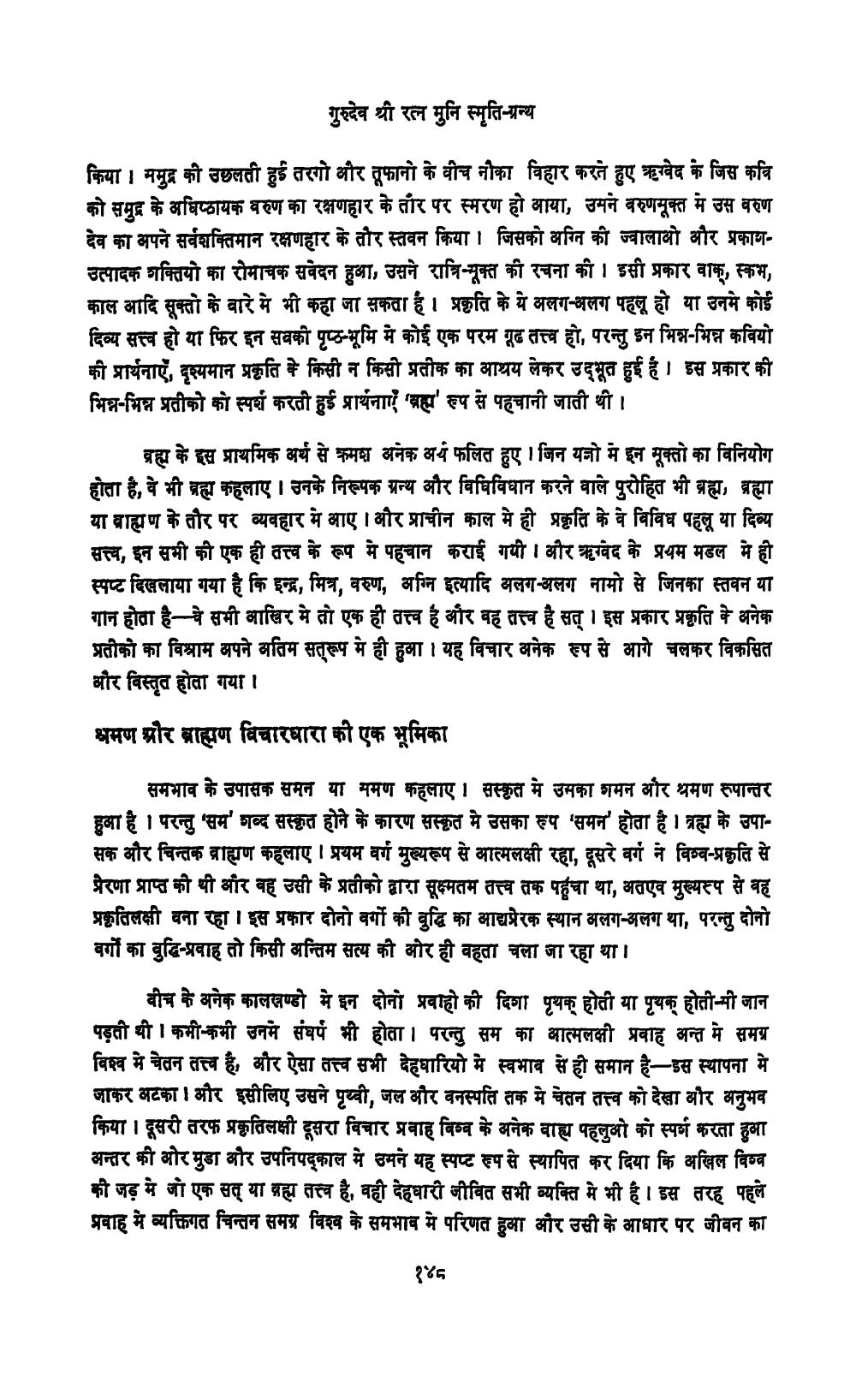________________
गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्थ
किया। ममुद्र की उछलती हुई तरगो और तूफानो के बीच नौका विहार करते हुए ऋग्वेद के जिस कवि को समुद्र के अधिष्ठायक वरुण का रक्षणहार के तौर पर स्मरण हो आया, उसने वरुणमूक्त में उस वरुण देव का अपने सर्वशक्तिमान रक्षणहार के तौर स्तवन किया। जिसको अग्नि की ज्वालाओ और प्रकाणउत्पादक शक्तियो का रोमाचक सवेदन हुआ, उसने रात्रि-यूक्त की रचना की । इसी प्रकार वाक्, स्कम, काल आदि सूक्तों के बारे में भी कहा जा सकता है। प्रकृति के ये अलग-अलग पहलू हो या उनमे कोई दिव्य सत्त्व हो या फिर इन सवकी पृष्ठभूमि में कोई एक परम गूढ तत्त्व हो, परन्तु इन भिन्न-भिन्न कवियो की प्रार्थनाएं, दृश्यमान प्रकृति के किसी न किसी प्रतीक का आश्रय लेकर उद्भूत हुई है। इस प्रकार की भिन्न-भिन्न प्रतीको को स्पर्श करती हुई प्रार्थनाएं 'ब्रह्म' रूप से पहचानी जाती थी।
ब्रह्म के इस प्राथमिक अर्थ से क्रमश अनेक अयं फलित हुए । जिन यनो में इन मूक्तो का विनियोग होता है, वे भी ब्रह्म कहलाए । उनके निरूपक ग्रन्थ और विधिविधान करने वाले पुरोहित भी ब्रह्म, ब्रह्मा या ब्राह्मण के तौर पर व्यवहार में माए । और प्राचीन काल मे ही प्रकृति के वे विविध पहलू या दिव्य सत्त्व, इन सभी को एक ही तत्त्व के रूप में पहचान कराई गयी । और ऋग्वेद के प्रथम मडल मे ही सप्ट दिखलाया गया है कि इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि इत्यादि अलग-अलग नामो से जिनका स्तवन या गान होता है-वे सभी आखिर मे तो एक ही तत्त्व है और वह तत्त्व है सत् । इस प्रकार प्रकृति के अनेक प्रतीको का विश्राम अपने अतिम सत्रूप में ही हुआ । यह विचार अनेक रूप से आगे चलकर विकसित और विस्तृत होता गया। श्रमण और ब्राह्मण विचारधारा को एक भूमिका
समभाव के उपासक समन या ममण कहलाए । संस्कृत में उसका गमन और श्रमण रुपान्तर हुआ है । परन्तु 'सम' शब्द संस्कृत होने के कारण सस्कृत मै उसका रूप 'समन' होता है । ब्रह्म के उपासक और चिन्तक ब्राह्मण कहलाए । प्रथम वर्ग मुख्यरूप से आत्मलक्षी रहा, दूसरे वर्ग ने विश्व-प्रकृति से प्रेरणा प्राप्त की थी और वह उसी के प्रतीको द्वारा सूक्ष्मतम तत्त्व तक पहुंचा था, अतएव मुख्यस्प से वह प्रकृतिलक्षी बना रहा । इस प्रकार दोनो वर्गों की बुद्धि का आद्यप्रेरक स्थान अलग-अलग था, परन्तु दोनो वर्गों का बुद्धि-प्रवाह तो किसी अन्तिम सत्य की ओर ही वहता चला जा रहा था।
वीच के अनेक कालखण्डो में इन दोनों प्रवाहो की दिशा पृथक् होती या पृथक् होती-मी जान पड़ती थी। कभी-कभी उनमे संघर्प भी होता। परन्तु सम का आत्मलक्षी प्रवाह अन्त मे समग्र विश्व में चेतन तत्त्व है, और ऐसा तत्त्व सभी देहधारियो मे स्वभाव से ही समान है-इस स्थापना मे जाकर अटका । और इसीलिए उसने पृथ्वी, जल और वनस्पति तक मै चेतन तत्त्व को देखा और अनुभव किया । दूसरी तरफ प्रकृतिलक्षी दूसरा विचार प्रवाह विश्व के अनेक वाह्य पहलुओ को स्पर्श करता हुआ अन्तर की ओर मुडा और उपनिपकाल में उसने यह स्पष्ट रूप से स्थापित कर दिया कि अखिल विश्व की जड़ मे जो एक सत् या ब्रह्म तत्त्व है, वही देहधारी जीवित सभी व्यक्ति में भी है। इस तरह पहले प्रवाह में व्यक्तिगत चिन्तन समग्र विश्व के समभाव में परिणत हुआ और उसी के आधार पर जीवन का
१४०