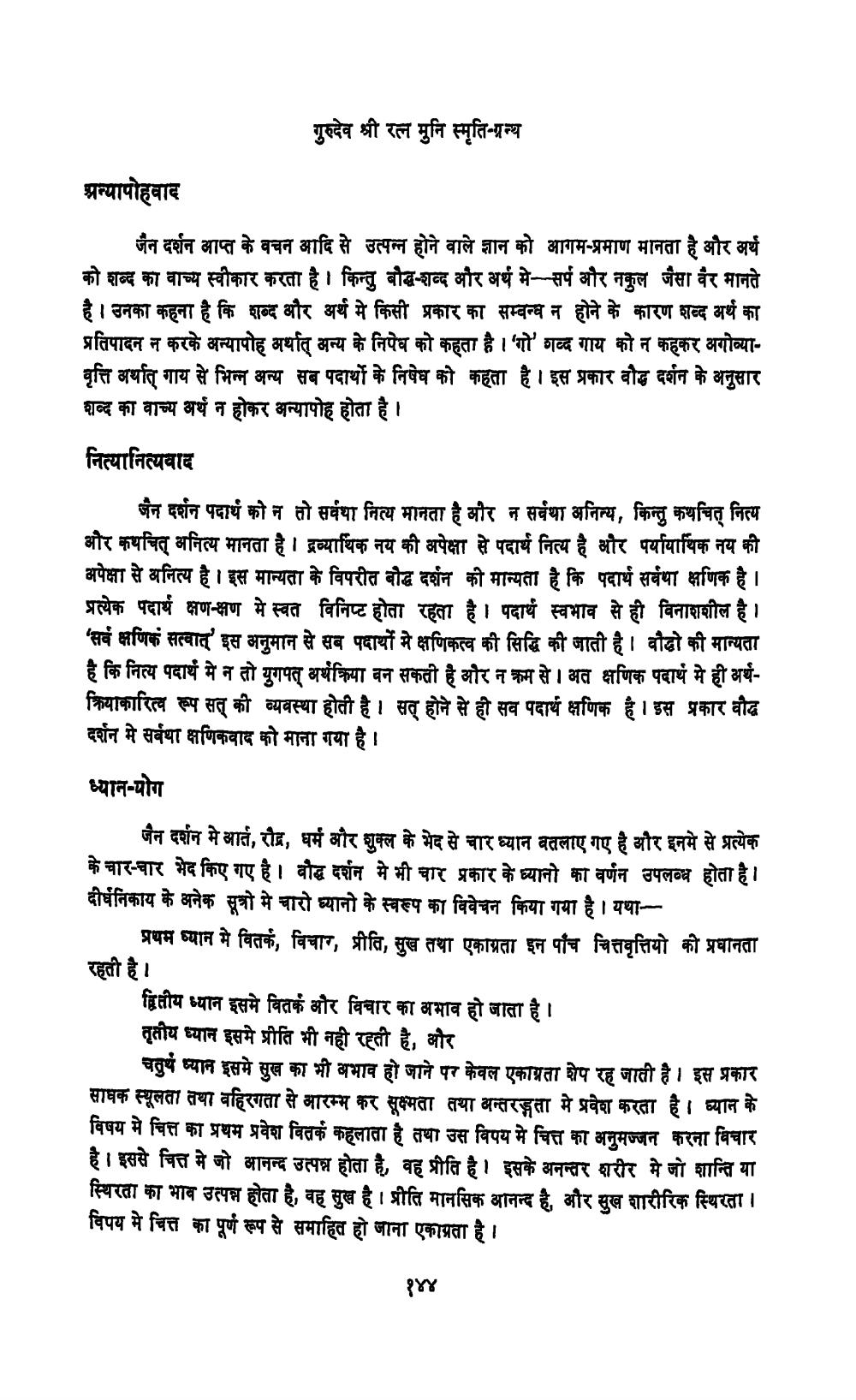________________
गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्थ
अन्यापोहवाद
जैन दर्शन आप्त के वचन आदि से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को आगम-प्रमाण मानता है और अर्थ को शब्द का वाच्य स्वीकार करता है। किन्तु बौद्ध-शब्द और अर्थ मे-सर्प और नकुल जैसा वर मानते है। उनका कहना है कि शब्द और अर्थ मे किसी प्रकार का सम्बन्ध न होने के कारण शब्द अर्थ का प्रतिपादन न करके अन्यापोह अर्थात् अन्य के निपेध को कहता है । 'गो' गब्द गाय को न कहकर अगोव्यावृत्ति अर्थात् गाय से भिन्न अन्य सब पदार्थों के निषेध को कहता है । इस प्रकार वौद्ध दर्शन के अनुसार शब्द का वाच्य अर्थ न होकर अन्यापोह होता है ।
नित्यानित्यवाद
जैन दर्शन पदार्थ को न तो सर्वथा नित्य मानता है और न सर्वथा अनिन्य, किन्तु कथचित् नित्य और कथचित् अनित्य मानता है । द्रव्याथिक नय की अपेक्षा से पदार्थ नित्य है और पर्यायाथिक नय की अपेक्षा से अनित्य है। इस मान्यता के विपरीत बौद्ध दर्शन को मान्यता है कि पदार्थ सर्वथा क्षणिक है । प्रत्येक पदार्थ क्षण-क्षण मे स्वत विनिप्ट होता रहता है। पदार्थ स्वभाव से ही विनाशशील है। 'सर्व क्षणिक सत्वात् इस अनुमान से सब पदार्थों मे क्षणिकत्व की सिद्धि की जाती है। बौद्धो की मान्यता है कि नित्य पदार्थ मे न तो युगपत् अर्थक्रिया बन सकती है और न क्रम से । अत क्षणिक पदार्थ मे ही अर्थक्रियाकारित्व रूप सत् की व्यवस्था होती है। सत् होने से ही सब पदार्थ क्षणिक है । इस प्रकार वौद्ध दर्शन मे सर्वथा क्षणिकवाद को माना गया है। ध्यान-योग
जैन दर्शन मे आर्त, रौद्र, धर्म और शुक्ल के भेद से चार ध्यान बतलाए गए है और इनमे से प्रत्येक के चार-चार भेद किए गए है। बौद्ध दर्शन मे भी चार प्रकार के ध्यानो का वर्णन उपलब्ध होता है। दीर्घनिकाय के अनेक सूत्रो मे चारो ध्यानो के स्वरूप का विवेचन किया गया है । यथा
प्रथम ध्यान मे वितर्क, विचार, प्रीति, सुख तथा एकाग्रता इन पांच चित्तवृत्तियो को प्रधानता
रहती है।
द्वितीय ध्यान इसमे वितर्क और विचार का अभाव हो जाता है। तृतीय ध्यान इसमे प्रीति भी नही रहती है, और
चतुर्थ ध्यान इसमे सुख का भी अभाव हो जाने पर केवल एकाग्रता शेप रह जाती है। इस प्रकार साधक स्थूलता तथा वहिरगता से आरम्भ कर सूक्ष्मता तथा अन्तरङ्गता मे प्रवेश करता है। ध्यान के विषय मे चित्त का प्रथम प्रवेश वितर्क कहलाता है तथा उस विषय मे चित्त का अनुमज्जन करना विचार है। इससे चित्त मे जो आनन्द उत्पन्न होता है, वह प्रीति है। इसके अनन्तर शरीर मे जो शान्ति या स्थिरता का भाव उत्पन्न होता है, वह सुख है । प्रीति मानसिक आनन्द है, और सुख शारीरिक स्थिरता । विषय मे चित्त का पूर्ण रूप से समाहित हो जाना एकाग्रता है।
१४४