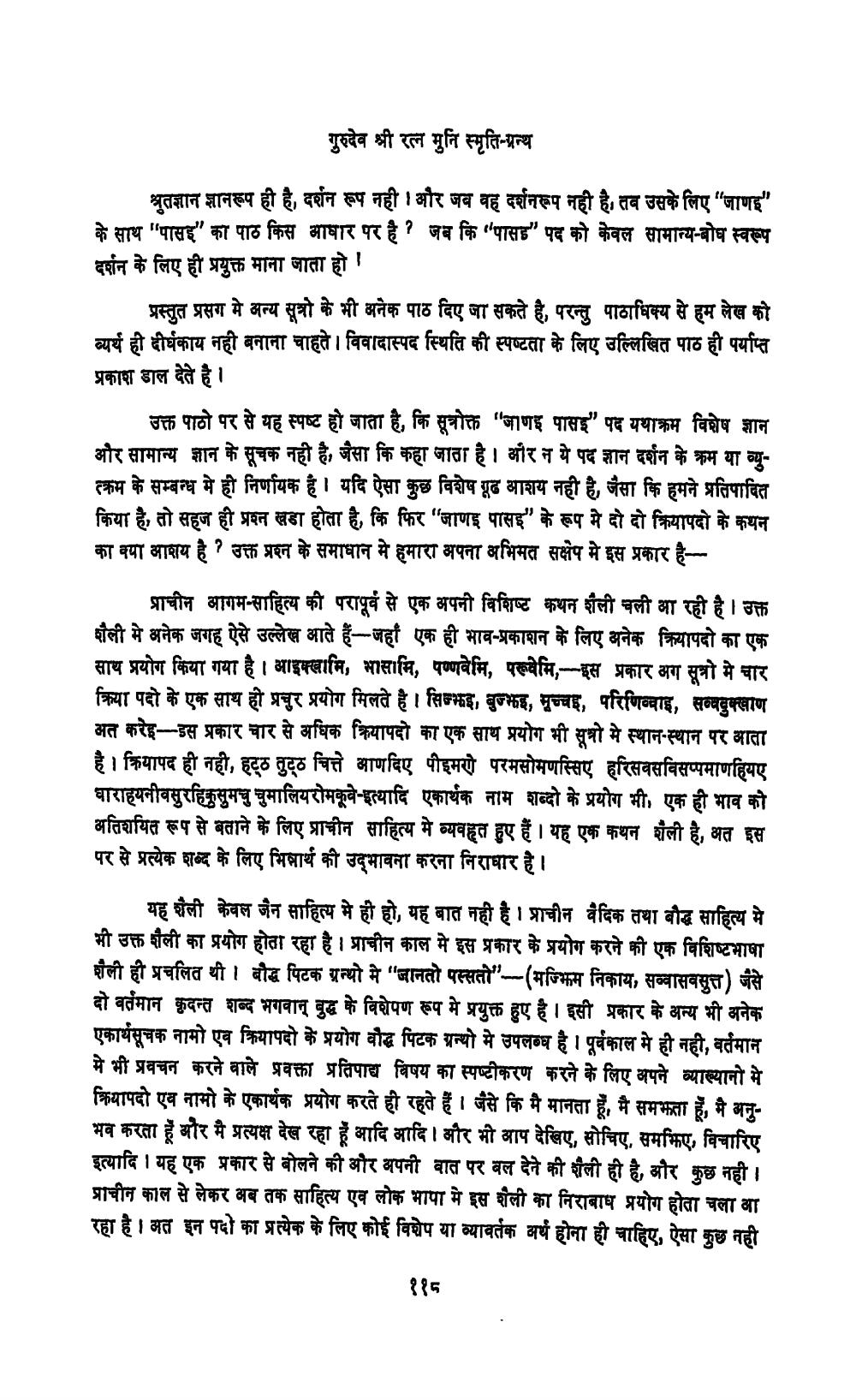________________
गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्थ
श्रुतज्ञान ज्ञानरूप ही है, दर्शन रूप नही । और जब वह दर्शनरूप नही है, तब उसके लिए "जाणइ" के साथ "पासई" का पाठ किस आधार पर है ? जब कि "पासह" पद को केवल सामान्य-बोध स्वरूप दर्शन के लिए ही प्रयुक्त माना जाता हो ।
प्रस्तुत प्रसग मे अन्य सूत्रो के भी अनेक पाठ दिए जा सकते है, परन्तु पाठाधिक्य से हम लेख को व्यर्थ ही दीर्घकाय नही बनाना चाहते । विवादास्पद स्थिति की स्पष्टता के लिए उल्लिखित पाठ ही पर्याप्त प्रकाश डाल देते है।
उक्त पाठो पर से यह स्पष्ट हो जाता है, कि सूत्रोक्त "जाणइ पासई" पद यथाक्रम विशेष ज्ञान और सामान्य ज्ञान के सूचक नही है, जैसा कि कहा जाता है। और न ये पद ज्ञान दर्शन के क्रम या व्यूक्रम के सम्बन्ध मे ही निर्णायक है। यदि ऐसा कुछ विशेष गूढ आशय नहीं है, जैसा कि हमने प्रतिपादित किया है, तो सहज ही प्रश्न खडा होता है, कि फिर "जाणइ पासई" के रूप मे दो दो क्रियापदो के कथन का क्या आशय है ? उक्त प्रश्न के समाधान मे हमारा अपना अभिमत सक्षेप मे इस प्रकार है
प्राचीन आगम-साहित्य की परापूर्व से एक अपनी विशिष्ट कथन शैली चली आ रही है । उक्त शैली मे अनेक जगह ऐसे उल्लेख आते हैं-जहाँ एक ही भाव-प्रकाशन के लिए अनेक क्रियापदो का एक साथ प्रयोग किया गया है । आइक्खामि, भासामि, पण्णवेमि, परूवेमि, इस प्रकार अग सूत्रो मे चार क्रिया पदो के एक साथ ही प्रचुर प्रयोग मिलते है । सिम्झइ, बुझइ, मच्चाइ, परिणिव्वाइ, सन्धदुक्खाण अत करेइ-इस प्रकार चार से अधिक क्रियापदो का एक साथ प्रयोग भी सूत्रो मे स्थान-स्थान पर आता है। क्रियापद ही नही, हट्ठ तुट्ठ चित्ते आणदिए पीइमणे परमसोमणस्सिए हरिसवसविसप्पमाणहियए धाराहयनीवसुरहिकुसुमचु चुमालियरोमकूवे-इत्यादि एकार्थक नाम शब्दो के प्रयोग भी, एक ही भाव को अतिशयित रूप से बताने के लिए प्राचीन साहित्य मे व्यवहृत हुए हैं । यह एक कथन शैली है, अत इस पर से प्रत्येक शब्द के लिए भिन्नार्थ की उद्भावना करना निराधार है।
यह शैली केवल जैन साहित्य मे ही हो, यह बात नहीं है । प्राचीन वैदिक तथा बौद्ध साहित्य मे भी उक्त शैली का प्रयोग होता रहा है । प्राचीन काल में इस प्रकार के प्रयोग करने की एक विशिष्टभाषा शैली ही प्रचलित थी। बौद्ध पिटक ग्रन्थो मे "जानतो पस्सतो"-(मज्झिम निकाय, सव्वासवसुत्त) जैसे दो वर्तमान कृदन्त शब्द भगवान् बुद्ध के विशेषण रूप में प्रयुक्त हुए है । इसी प्रकार के अन्य भी अनेक एकार्थसूचक नामो एव क्रियापदो के प्रयोग वौद्ध पिटक ग्रन्थो मे उपलब्ध है । पूर्वकाल मे ही नहीं, वर्तमान मे भी प्रवचन करने वाले प्रवक्ता प्रतिपाद्य विषय का स्पष्टीकरण करने के लिए अपने व्याख्यानो मे क्रियापदो एव नामो के एकार्थक प्रयोग करते ही रहते हैं । जैसे कि मै मानता हूँ, मै समझता हूँ, मै अनुभव करता हूँ और मै प्रत्यक्ष देख रहा हूँ आदि आदि । और भी आप देखिए, सोचिए, समझिए, विचारिए इत्यादि । यह एक प्रकार से बोलने की और अपनी बात पर बल देने की शैली ही है, और कुछ नही । प्राचीन काल से लेकर अब तक साहित्य एव लोक भाषा मे इस शैली का निराबाध प्रयोग होता चला आ रहा है । अत इन पदो का प्रत्येक के लिए कोई विशेप या व्यावर्तक अर्थ होना ही चाहिए, ऐसा कुछ नही
११८