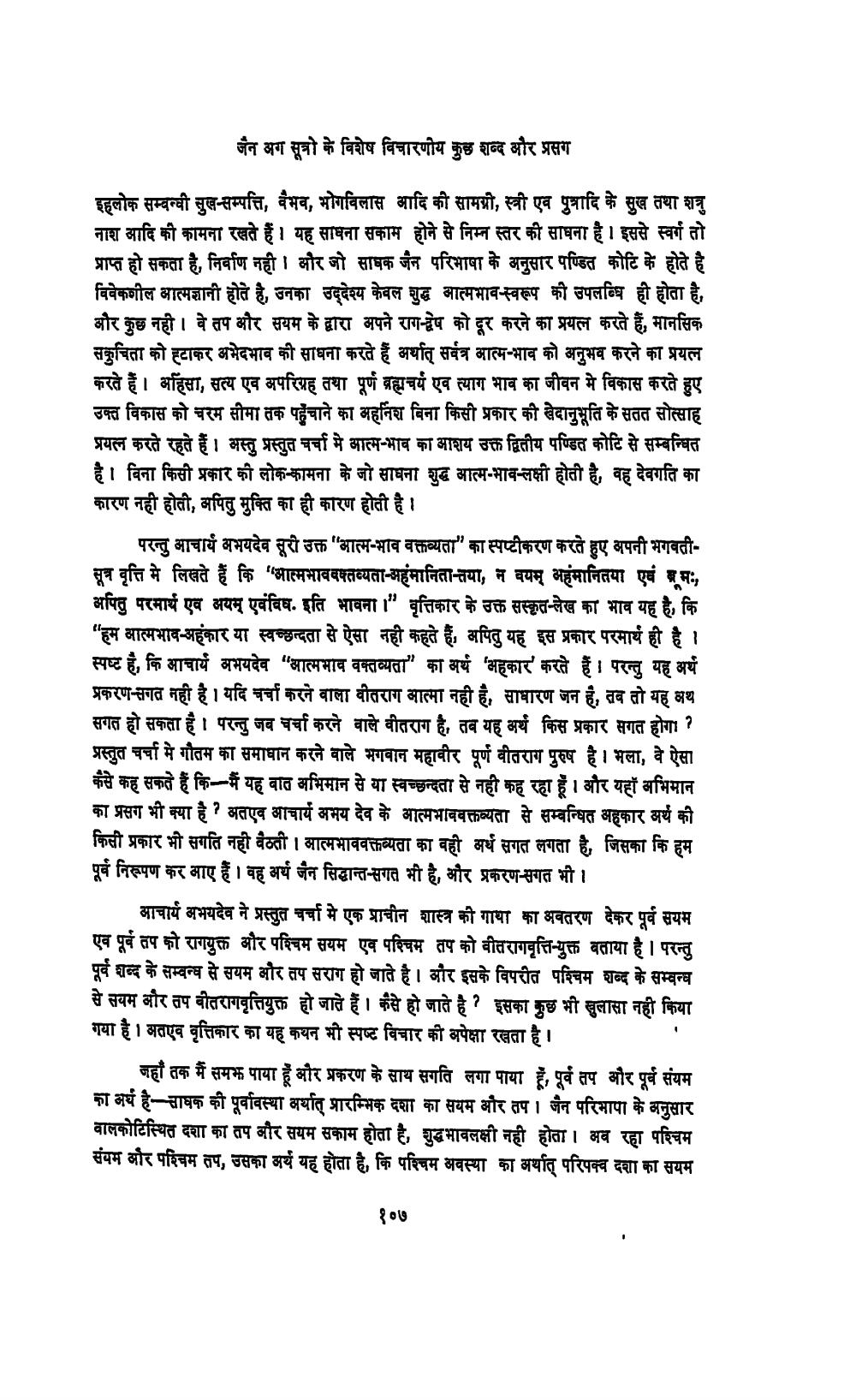________________
जैन अग सूत्रो के विशेष विचारणीय कुछ शब्द और प्रसग
इहलोक सम्बन्धी सुख-सम्पत्ति, वैभव, भोगविलास आदि की सामग्री, स्त्री एव पुत्रादि के सुख तथा शत्रु नाश आदि की कामना रखते हैं। यह साधना सकाम होने से निम्न स्तर की साधना है । इससे स्वर्ग तो प्राप्त हो सकता है, निर्वाण नही । और जो साधक जैन परिभाषा के अनुसार पण्डित कोटि के होते है विवेकगील आत्मज्ञानी होते है, उनका उद्देश्य केवल शुद्ध आत्मभाव-स्वरूप की उपलब्धि ही होता है,
और कुछ नही । वे तप और सयम के द्वारा अपने राग-द्वेष को दूर करने का प्रयल करते हैं, मानसिक सकुचिता को हटाकर अभेदभाव की साधना करते हैं अर्थात् सर्वत्र आत्म-भाव को अनुभव करने का प्रयल करते हैं। अहिंसा, सत्य एव अपरिग्रह तथा पूर्ण ब्रह्मचर्य एव त्याग भाव का जीवन मे विकास करते हुए उक्त विकास को चरम सीमा तक पहुंचाने का अहर्निश बिना किसी प्रकार की खेदानुभूति के सतत सोत्साह प्रयत्न करते रहते हैं। अस्तु प्रस्तुत चर्चा में आत्म-भाव का आशय उक्त द्वितीय पण्डित कोटि से सम्बन्धित है। बिना किसी प्रकार की लोक-कामना के जो साधना शुद्ध आत्म-भाव-लक्षी होती है, वह देवगति का कारण नही होती, अपितु मुक्ति का ही कारण होती है ।
परन्तु आचार्य अभयदेव सूरी उक्त "आत्म-भाव वक्तव्यता" का स्पष्टीकरण करते हुए अपनी भगवतीसूत्र वृत्ति मे लिखते हैं कि "आत्मभाववक्तव्यता-अहंमानिता-तया, न वयम् महंमानितया एवं नमः, अपितु परमार्थ एव अयम् एवं विष. इति भावना।" वृत्तिकार के उक्त संस्कृत-लेख का भाव यह है कि "हम आत्मभाव-अहंकार या स्वच्छन्दता से ऐसा नही कहते हैं, अपितु यह इस प्रकार परमार्थ ही है । स्पष्ट है, कि आचार्य अभयदेव "आत्मभाव वक्तव्यता" का अर्थ 'महकार करते हैं। परन्तु यह अर्थ प्रकरण-सगत नहीं है । यदि चर्चा करने वाला वीतराग आत्मा नही है, साधारण जन है, तब तो यह अथ सगत हो सकता है। परन्तु जब चर्चा करने वाले वीतराग है, तब यह अर्थ किस प्रकार सगत होगा? प्रस्तुत चर्चा मे गौतम का समाधान करने वाले भगवान महावीर पूर्ण वीतराग पुरुष है । भला, वे ऐसा कैसे कह सकते हैं कि मैं यह वात अभिमान से या स्वच्छन्दता से नहीं कह रहा हूँ। और यहाँ अभिमान का प्रसग भी क्या है ? अतएव आचार्य अभय देव के आत्मभाववक्तव्यता से सम्बन्धित अहकार अर्थ की किसी प्रकार भी सगति नहीं बैठती । आत्मभाववक्तव्यता का वही अर्थ सगत लगता है, जिसका कि हम पूर्व निरूपण कर आए हैं । वह अर्थ जैन सिद्धान्त-सगत भी है, और प्रकरण-सगत भी।
आचार्य अभयदेव ने प्रस्तुत चर्चा मे एक प्राचीन शास्त्र की गाथा का अवतरण देकर पूर्व सयम एव पूर्व तप को रागयुक्त और पश्चिम सयम एव पश्चिम तप को वीतरागवृत्ति-युक्त बताया है । परन्तु पूर्व शब्द के सम्बन्ध से सयम और तप सराग हो जाते है। और इसके विपरीत पश्चिम शब्द के सम्बन्ध से सयम और तप वीतरागवृत्तियुक्त हो जाते हैं । कैसे हो जाते है ? इसका कुछ भी खुलासा नहीं किया गया है । अतएव वृत्तिकार का यह कथन भी स्पष्ट विचार की अपेक्षा रखता है।
जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ और प्रकरण के साथ सगति लगा पाया है, पूर्व तप और पूर्व संयम का अर्थ है-साधक की पूर्वावस्था अर्थात् प्रारम्भिक दशा का सयम और तप । जैन परिभापा के अनुसार वालकोटिस्थित दशा का तप और सयम सकाम होता है, शुद्धभावलक्षी नही होता। अव रहा पश्चिम संयम और पश्चिम तप, उसका अर्थ यह होता है, कि पश्चिम अवस्था का अर्थात् परिपक्व दशा का सयम
१०७