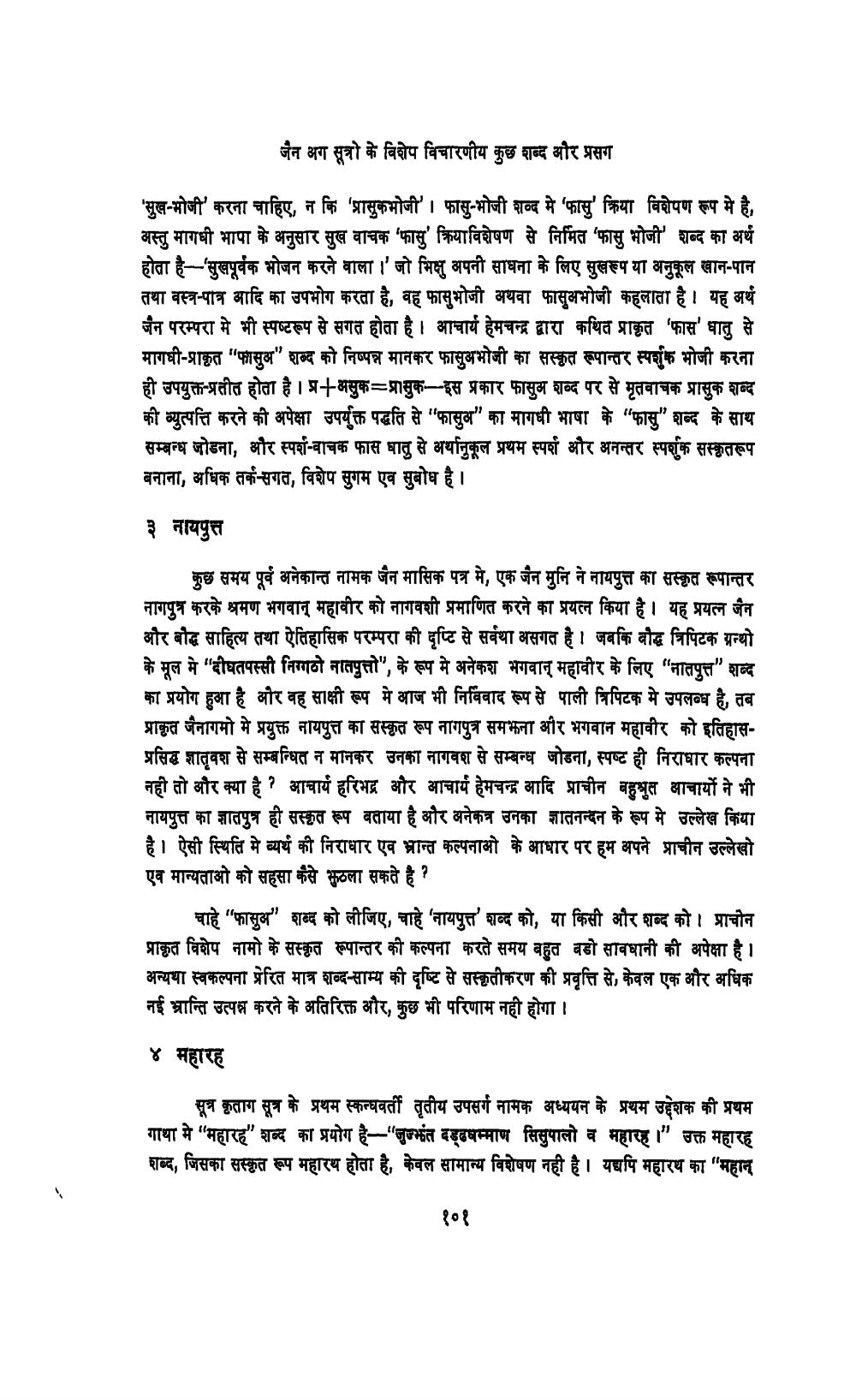________________
जैन अग सूत्रो के विशेप विचारणीय कुछ शब्द और प्रसग
'सुख-भोजी' करना चाहिए, न कि 'प्रासुकभोजी' । फासु-भोजी शब्द मे 'फासु' क्रिया विशेषण रूप में है, अस्तु मागधी भापा के अनुसार सुख वाचक 'फासु' क्रियाविशेषण से निर्मित 'फासु भोजी' शब्द का अर्थ होता है-'सुखपूर्वक भोजन करने वाला ।' जो भिक्षु अपनी साधना के लिए सुखरूप या अनुकूल खान-पान तथा वस्त्र-पात्र आदि का उपभोग करता है, वह फासुभोजी अथवा फासुअभोजी कहलाता है। यह अर्थ जैन परम्परा मे भी स्पष्टरूप से सगत होता है। आचार्य हेमचन्द्र द्वारा कथित प्राकृत 'फास' धातु से मागधी-प्राकृत "फासुअ" शब्द को निष्पन्न मानकर फासुअभोजी का सस्कृत रूपान्तर स्पर्शक भोजी करना ही उपयुक्त प्रतीत होता है । प्र+असुक=प्रासुक-इस प्रकार फासुअ शब्द पर से मृतवाचक प्रासुक शब्द की व्युत्पत्ति करने की अपेक्षा उपर्युक्त पद्धति से "फासुम" का मागधी भाषा के "फासु" शब्द के साथ सम्बन्ध जोडना, और स्पर्श-वाचक फास धातु से अर्थानुकूल प्रथम स्पर्श और अनन्तर स्पर्शक सस्कृतरूप बनाना, अधिक तर्क-सगत, विशेप सुगम एव सुबोध है।
३ नायपुत्त
कुछ समय पूर्व अनेकान्त नामक जैन मासिक पत्र मे, एक जैन मुनि ने नायपुत्त का सस्कृत रूपान्तर नागपुत्र करके श्रमण भगवान् महावीर को नागवशी प्रमाणित करने का प्रयत्ल किया है। यह प्रयत्न जैन
और बौद्ध साहित्य तथा ऐतिहासिक परम्परा की दृष्टि से सर्वथा असगत है। जबकि बौद्ध त्रिपिटक ग्रन्थो के मूल मे "दोघतपस्सी निग्गगे नातपुत्तो", के रूप मे अनेकश भगवान् महावीर के लिए "नातपुत्त" शब्द का प्रयोग हुआ है और वह साक्षी रूप मे आज भी निर्विवाद रूप से पाली त्रिपिटक मे उपलब्ध है, तब प्राकृत जैनागमो मे प्रयुक्त नायपुत्त का सस्कृत रूप नागपुत्र समझना और भगवान महावीर को इतिहासप्रसिद्ध ज्ञातृवश से सम्बन्धित न मानकर उनका नागवश से सम्बन्ध जोडना, स्पष्ट ही निराधार कल्पना नहीं तो और क्या है ? आचार्य हरिभद्र और आचार्य हेमचन्द्र आदि प्राचीन बहुश्रुत आचार्यों ने भी नायपुत्त का ज्ञातपुत्र ही सस्कृत रूप बताया है और अनेकत्र उनका ज्ञातनन्दन के रूप मे उल्लेख किया है। ऐसी स्थिति मे व्यर्थ की निराधार एव भ्रान्त कल्पनाओ के आधार पर हम अपने प्राचीन उल्लेखो एव मान्यताओ को सहसा कैसे झुठला सकते है ?
चाहे "फासुअ" शब्द को लीजिए, चाहे 'नायपुत्त' शब्द को, या किसी और शब्द को। प्राचीन प्राकृत विशेप नामो के सस्कृत रूपान्तर की कल्पना करते समय बहुत बडो सावधानी की अपेक्षा है। अन्यथा स्वकल्पना प्रेरित मात्र शब्द-साम्य की दृष्टि से सस्कृतीकरण की प्रवृत्ति से, केवल एक और अधिक नई भ्रान्ति उत्पन्न करने के अतिरिक्त और, कुछ भी परिणाम नही होगा।
४ महारह
सूत्र कृताग सूत्र के प्रथम स्कन्धवर्ती तृतीय उपसर्ग नामक अध्ययन के प्रथम उद्देशक की प्रथम गाथा मे "महारह" शब्द का प्रयोग है-"जुम्भंत दड्डधम्माण सिसुपालो व महारह ।” उक्त महारह शब्द, जिसका सस्कृत रूप महारथ होता है, केवल सामान्य विशेषण नहीं है। यद्यपि महारथ का "महान
१०१