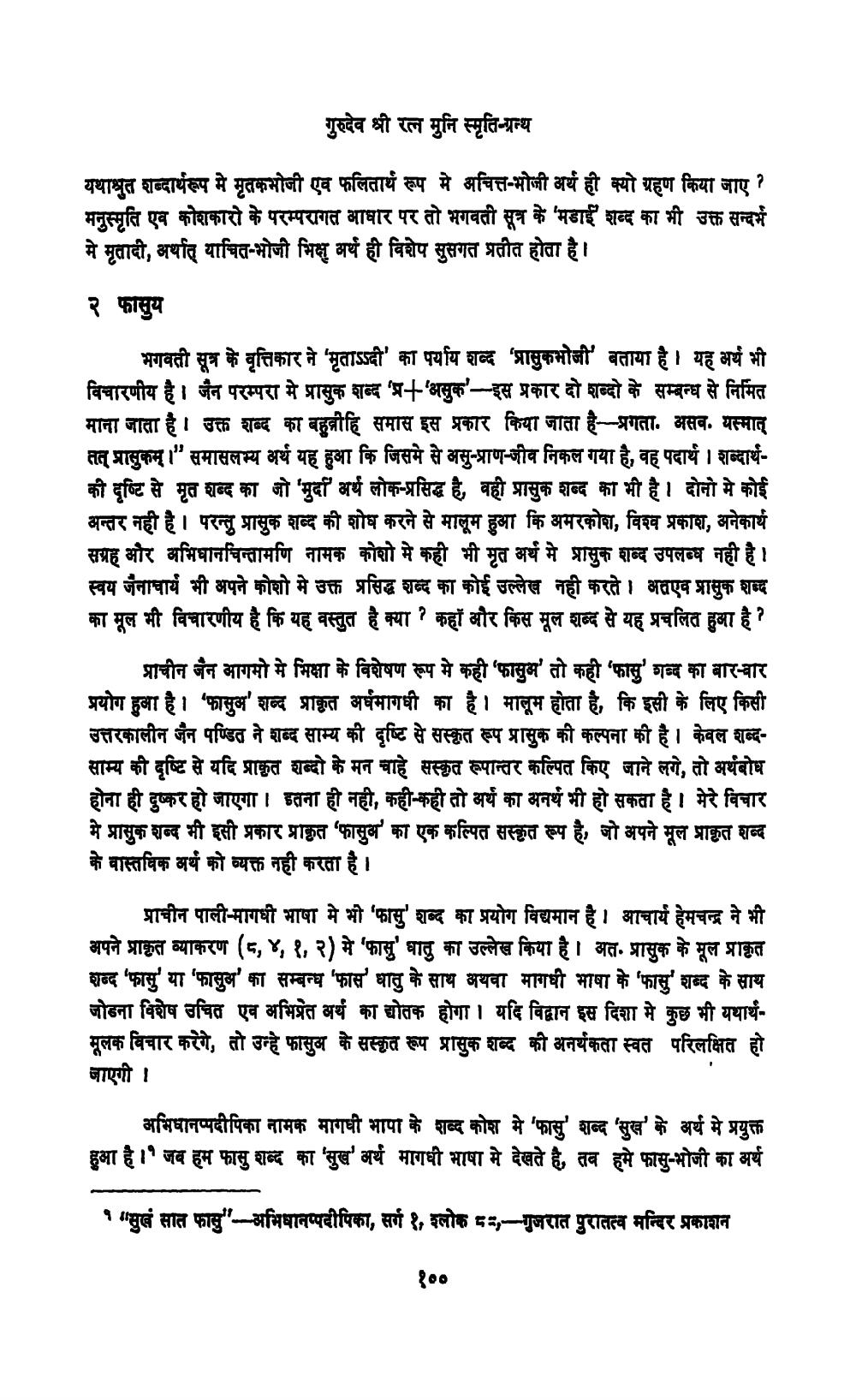________________
गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति-ग्रन्थ यथाश्रुत शब्दार्थरूप मे मृतकभोजी एव फलितार्थ रूप मे अचित्त-भोजी अर्थ ही क्यो ग्रहण किया जाए। मनुस्मृति एव कोशकारो के परम्परागत आधार पर तो भगवती सूत्र के 'मडाई शब्द का भी उक्त सन्दर्भ मे मृतादी, अर्थात् याचित-भोजी भिक्षु अर्थ ही विशेप सुसगत प्रतीत होता है।
२ फासुय
भगवती सूत्र के वृत्तिकार ने 'मृताऽऽदी' का पर्याय शब्द 'प्रासुकभोजी' बताया है। यह अर्थ भी विचारणीय है। जैन परम्परा मे प्रासुक शब्द '+'असुक'-इस प्रकार दो शब्दो के सम्बन्ध से निर्मित माना जाता है। उक्त शब्द का बहुव्रीहि समास इस प्रकार किया जाता है-प्रगता. असव. यस्मात् तत् प्रासुकम्।" समासलभ्य अर्थ यह हुआ कि जिसमे से असु-प्राण-जीव निकल गया है, वह पदार्थ । शब्दार्थकी दृष्टि से मृत शब्द का जो 'मुर्दा अर्थ लोक-प्रसिद्ध है, वही प्रासुक शब्द का भी है। दोनो मे कोई अन्तर नहीं है। परन्तु प्रासुक शब्द की शोध करने से मालूम हुआ कि अमरकोश, विश्व प्रकाश, अनेकार्थ सग्रह और अभिधानचिन्तामणि नामक कोशो मे कही भी मृत अर्थ मे प्रासुक शब्द उपलब्ध नहीं है। स्वय जैनाचार्य भी अपने कोशो मे उक्त प्रसिद्ध शब्द का कोई उल्लेख नहीं करते। अतएव प्रासुक शब्द का मूल भी विचारणीय है कि यह वस्तुत है क्या ? कहाँ और किस मूल शब्द से यह प्रचलित हुआ है ?
प्राचीन जैन आगमो मे भिक्षा के विशेषण रूप मे कही 'फासुम' तो कही 'फासु' गब्द का बार-बार प्रयोग हुआ है। 'फासुअ' शब्द प्राकृत अर्धमागधी का है। मालूम होता है, कि इसी के लिए किसी उत्तरकालीन जैन पण्डित ने शब्द साम्य की दृष्टि से सस्कृत रूप प्रासुक की कल्पना की है। केवल शब्दसाम्य की दृष्टि से यदि प्राकृत शब्दो के मन चाहे संस्कृत रूपान्तर कल्पित किए जाने लगे, तो अर्थबोध होना ही दुष्कर हो जाएगा। इतना ही नही, कही-कही तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। मेरे विचार मे प्रासुक शब्द भी इसी प्रकार प्राकृत 'फासुम' का एक कल्पित सस्कृत रूप है, जो अपने मूल प्राकृत शब्द के वास्तविक अर्थ को व्यक्त नहीं करता है।
प्राचीन पाली-मागधी भाषा मे भी 'फासु' शब्द का प्रयोग विद्यमान है। आचार्य हेमचन्द्र ने भी अपने प्राकृत व्याकरण (८, ४, १, २) मे 'फासु' धातु का उल्लेख किया है। अत. प्रासुक के मूल प्राकृत शब्द 'फासु' या 'फासुअ' का सम्बन्ध 'फास' धातु के साथ अथवा मागधी भाषा के 'फासु' शब्द के साथ जोडना विशेष उचित एव अभिप्रेत अर्थ का द्योतक होगा। यदि विद्वान इस दिशा मे कुछ भी यथार्थमूलक विचार करेंगे, तो उन्हे फासुम के सस्कृत रूप प्रासुक शब्द की अनर्थकता स्वत परिलक्षित हो जाएगी।
अभिधानप्पदीपिका नामक मागधी भापा के शब्द कोश मे 'फासु' शब्द 'सुख' के अर्थ मे प्रयुक्त हुआ है। जब हम फासु शब्द का 'सुख' अर्थ मागधी भाषा मे देखते है, तब हमे फासु-भोजी का अर्थ
"सुखं सात फासु"-अभिधानप्पदीपिका, सर्ग १, श्लोक
-गुजरात पुरातत्व मन्दिर प्रकाशन