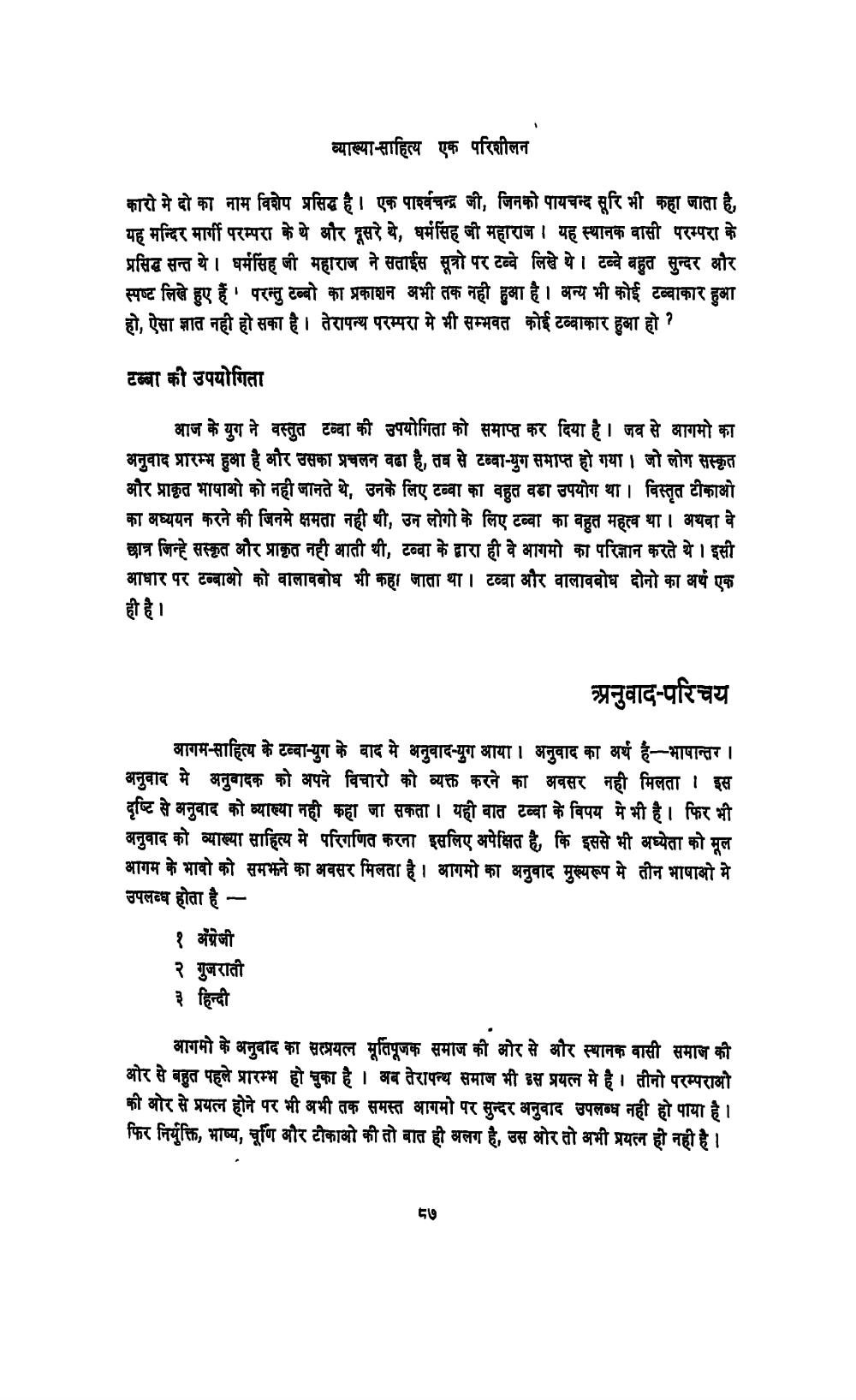________________
व्याख्या-साहित्य एक परिशीलन
कारो मे दो का नाम विशेप प्रसिद्ध है। एक पार्श्वचन्द्र जी, जिनको पायचन्द सूरि भी कहा जाता है, यह मन्दिर मार्गी परम्परा के थे और दूसरे थे, धर्मसिंह जी महाराज । यह स्थानक वासी परम्परा के प्रसिद्ध सन्त थे। धर्मसिंह जी महाराज ने सताईस सूत्रो पर टब्बे लिखे थे। टब्बे बहुत सुन्दर और स्पष्ट लिखे हुए हैं। परन्तु टब्बो का प्रकाशन अभी तक नही हुआ है। अन्य भी कोई टब्बाकार हुआ हो, ऐसा ज्ञात नही हो सका है। तेरापन्थ परम्परा मे भी सम्भवत कोई टव्वाकार हुआ हो ?
टब्बा की उपयोगिता
आज के युग ने वस्तुत टव्वा की उपयोगिता को समाप्त कर दिया है। जब से आगमो का अनुवाद प्रारम्भ हुआ है और उसका प्रचलन बढा है, तब से टब्वा-युग समाप्त हो गया। जो लोग सस्कृत और प्राकृत भाषाओ को नही जानते थे, उनके लिए टब्वा का बहुत वडा उपयोग था। विस्तृत टीकाओ का अध्ययन करने की जिनमे क्षमता नहीं थी, उन लोगो के लिए टब्बा का बहुत महत्व था । अथवा वे छात्र जिन्हे सस्कृत और प्राकृत नहीं आती थी, टव्वा के द्वारा ही वे आगमो का परिज्ञान करते थे। इसी आधार पर टब्बाओ को वालावबोध भी कहा जाता था। टव्वा और वालावबोध दोनो का अर्थ एक
ही है।
अनुवाद-परिचय
आगम-साहित्य के टब्बा-युग के बाद मे अनुवाद-युग आया। अनुवाद का अर्थ है-भाषान्तर । अनुवाद मे अनुवादक को अपने विचारो को व्यक्त करने का अवसर नही मिलता । इस दृष्टि से अनुवाद को व्याख्या नहीं कहा जा सकता । यही बात टब्वा के विषय में भी है। फिर भी अनुवाद को व्याख्या साहित्य मे परिगणित करना इसलिए अपेक्षित है, कि इससे भी अध्येता को मूल आगम के भावो को समझने का अवसर मिलता है। आगमो का अनुवाद मुख्यरूप मे तीन भाषाओ मे उपलब्ध होता है -
१ अंग्रेजी २ गुजराती ३ हिन्दी
आगमो के अनुवाद का सत्प्रयत्न मूर्तिपूजक समाज की ओर से और स्थानक वासी समाज की ओर से बहुत पहले प्रारम्भ हो चुका है । अब तेरापन्थ समाज भी इस प्रयत्न मे है। तीनो परम्पराओ की ओर से प्रयत्न होने पर भी अभी तक समस्त आगमो पर सुन्दर अनुवाद उपलब्ध नहीं हो पाया है। फिर नियुक्ति, भाष्य, चूणि और टीकाओ की तो बात ही अलग है, उस ओर तो अभी प्रयत्न ही नहीं है।