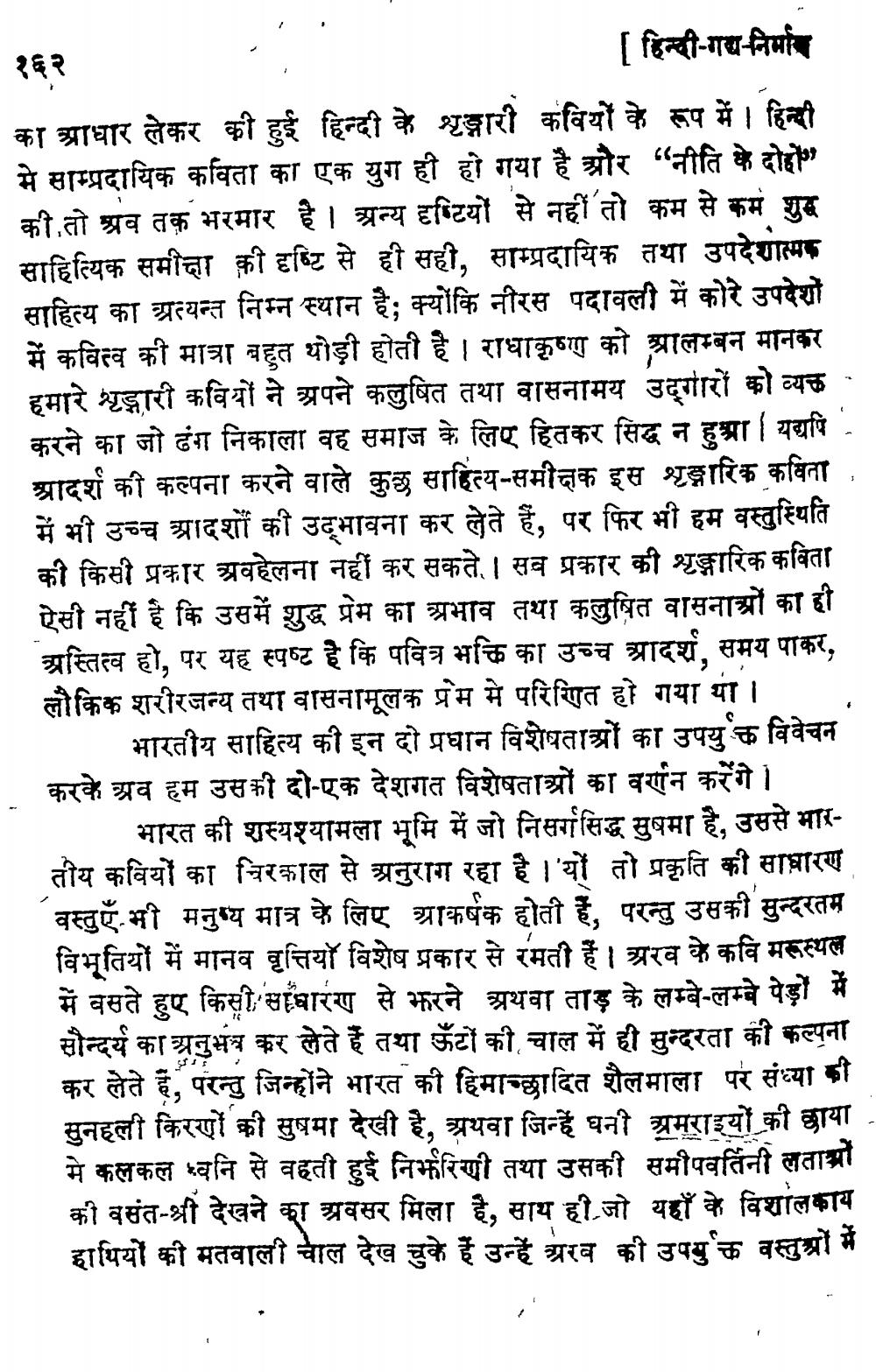________________
२६२
[हिन्दी-गद्य-निर्माब का आधार लेकर की हुई हिन्दी के शृङ्गारी कवियों के रूप में । हिन्दी मे साम्प्रदायिक कविता का एक युग ही हो गया है और "नीति के दोहो" की,तो अव तक भरमार है। अन्य दृष्टियों से नहीं तो कम से कम शुद्ध साहित्यिक समीक्षा की दृष्टि से ही सही, साम्प्रदायिक तथा उपदेशात्मक साहित्य का अत्यन्त निम्न स्थान है; क्योंकि नीरस पदावली में कोरे उपदेशों में कवित्व की मात्रा बहुत थोड़ी होती है । राधाकृष्ण को पालम्बन मानकर हमारे शृङ्गारी कवियों ने अपने कलुषित तथा वासनामय उद्गारों को व्यक्त । करने का जो ढंग निकाला वह समाज के लिए हितकर सिद्ध न हुआ । यद्यपि . श्रादर्श की कल्पना करने वाले कुछ साहित्य-समीक्षक इस शृङ्गारिक कविता में भी उच्च आदर्शों की उद्भावना कर लेते हैं, पर फिर भी हम वस्तुस्थिति की किसी प्रकार अवहेलना नहीं कर सकते । सब प्रकार की शृङ्गारिक कविता ऐसी नहीं है कि उसमें शुद्ध प्रेम का अभाव तथा कलुषित वासनाओं का ही अस्तित्व हो, पर यह स्पष्ट है कि पवित्र भक्ति का उच्च आदर्श, समय पाकर, लौकिक शरीरजन्य तथा वासनामूलक प्रेम मे परिणित हो गया था।
भारतीय साहित्य की इन दो प्रधान विशेषताओं का उपयुक्त विवेचन करके अव हम उसकी दो-एक देशगत विशेषताओं का वर्णन करेंगे।
भारत की शस्यश्यामला भूमि में जो निसर्गसिद्ध सुषमा है, उससे मारतीय कवियों का चिरकाल से अनुराग रहा है । यों तो प्रकृति की साधारण वस्तुएँ भी मनुष्य मात्र के लिए अाकर्षक होती हैं, परन्तु उसकी सुन्दरतम विभूतियों में मानव वृत्तियों विशेष प्रकार से रमती हैं । अरव के कवि मरूस्थल में वसते हुए किसी साधारण से झरने अथवा ताड़ के लम्बे-लम्बे पेड़ों में सौन्दर्य का अनुभव कर लेते हैं तथा ऊँटों की चाल में ही सुन्दरता की कल्पना कर लेते हैं, परन्तु जिन्होंने भारत की हिमाच्छादित शैलमाला पर संध्या की सुनहली किरणों की सुषमा देखी है, अथवा जिन्हें घनी अमराइयों की छाया . मे कलकल ध्वनि से वहती हुई निरिणी तथा उसकी समीपवर्तिनी लताओ की वसंत-श्री देखने का अवसर मिला है, साथ ही,जो यहाँ के विशालकाय हाथियों की मतवाली चाल देख चुके हैं उन्हें अरव की उपयुक्त वस्तुओं में