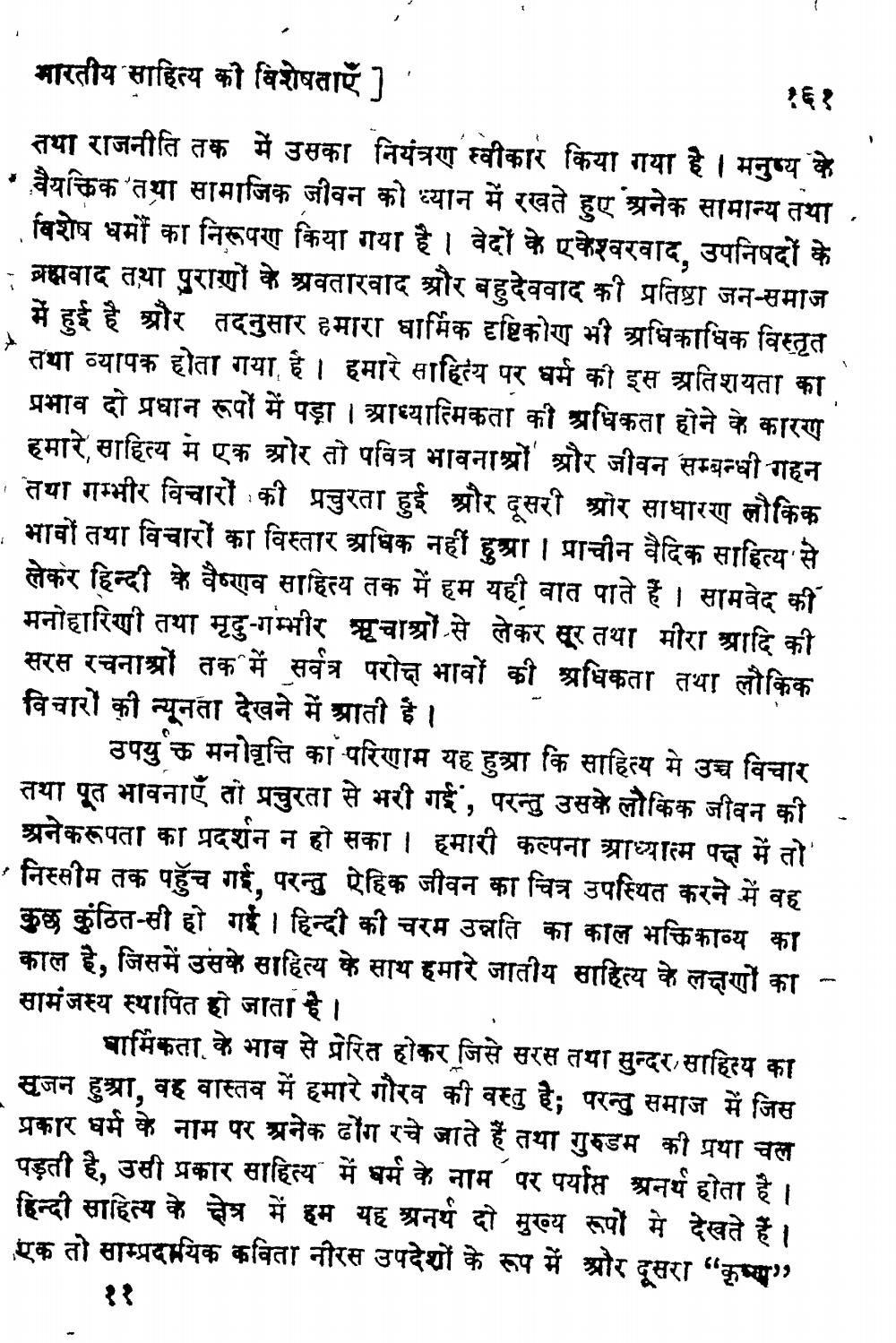________________
भारतीय साहित्य को विशेषताएँ] .
तथा राजनीति तक में उसका नियंत्रण स्वीकार किया गया है । मनुष्य के - वैयक्तिक तथा सामाजिक जीवन को ध्यान में रखते हुए अनेक सामान्य तथा ,
विशेष धर्मों का निरूपण किया गया है। वेदों के एकेश्वरवाद, उपनिषदों के - ब्रह्मवाद तथा पुराणों के अवतारवाद और बहुदेववाद की प्रतिष्ठा जन-समाज में हुई है और तदनुसार हमारा धार्मिक दृष्टिकोण भी अधिकाधिक विस्तृत तथा व्यापक होता गया है। हमारे साहित्य पर धर्म की इस अतिशयता का प्रभाव दो प्रधान रूपों में पड़ा । आध्यात्मिकता की अधिकता होने के कारण हमारे, साहित्य में एक ओर तो पवित्र भावनाओं और जीवन सम्बन्धी गहन तथा गम्भीर विचारों की प्रचुरता हुई और दूसरी श्रोर साधारण लौकिक भावों तथा विचारों का विस्तार अधिक नहीं हुआ। प्राचीन वैदिक साहित्य से लेकर हिन्दी के वैष्णव साहित्य तक में हम यही बात पाते हैं । सामवेद की मनोहारिणी तथा मृदु-गम्भीर ऋचायों से लेकर सूर तथा मीरा आदि की सरस रचनाओं तक में सर्वत्र परोक्ष भावों की अधिकता तथा लौकिक विचारों की न्यूनता देखने में आती है।
उपयुक्त मनोवृत्ति का परिणाम यह हुआ कि साहित्य मे उच्च विचार तथा पूत भावनाएँ तो प्रचुरता से भरी गई, परन्तु उसके लौकिक जीवन की .
अनेकरूपता का प्रदर्शन न हो सका। हमारी कल्पना प्राध्यात्म पक्ष में तो , निस्सीम तक पहुंच गई, परन्तु ऐहिक जीवन का चित्र उपस्थित करने में वह कुछ कुंठित-सी हो गई । हिन्दी की चरम उन्नति का काल भक्तिकाव्य का काल है, जिसमें उसके साहित्य के साथ हमारे जातीय साहित्य के लक्षणों का - सामंजस्य स्थापित हो जाता है।
धार्मिकता के भाव से प्रेरित होकर जिसे सरस तथा सुन्दर साहित्य का सुजन हुश्रा, वह वास्तव में हमारे गौरव की वस्तु है; परन्तु समाज में जिस प्रकार धर्म के नाम पर अनेक ढोंग रचे जाते हैं तथा गुरुडम की प्रथा चल पड़ती है, उसी प्रकार साहित्य में धर्म के नाम पर पर्याप्त अनर्थ होता है। हिन्दी साहित्य के क्षेत्र में हम यह अनर्थ दो मुख्य रूपों में देखते हैं। एक तो साम्प्रदायिक कविता नीरस उपदेशों के रूप में और दूसरा "कृ"