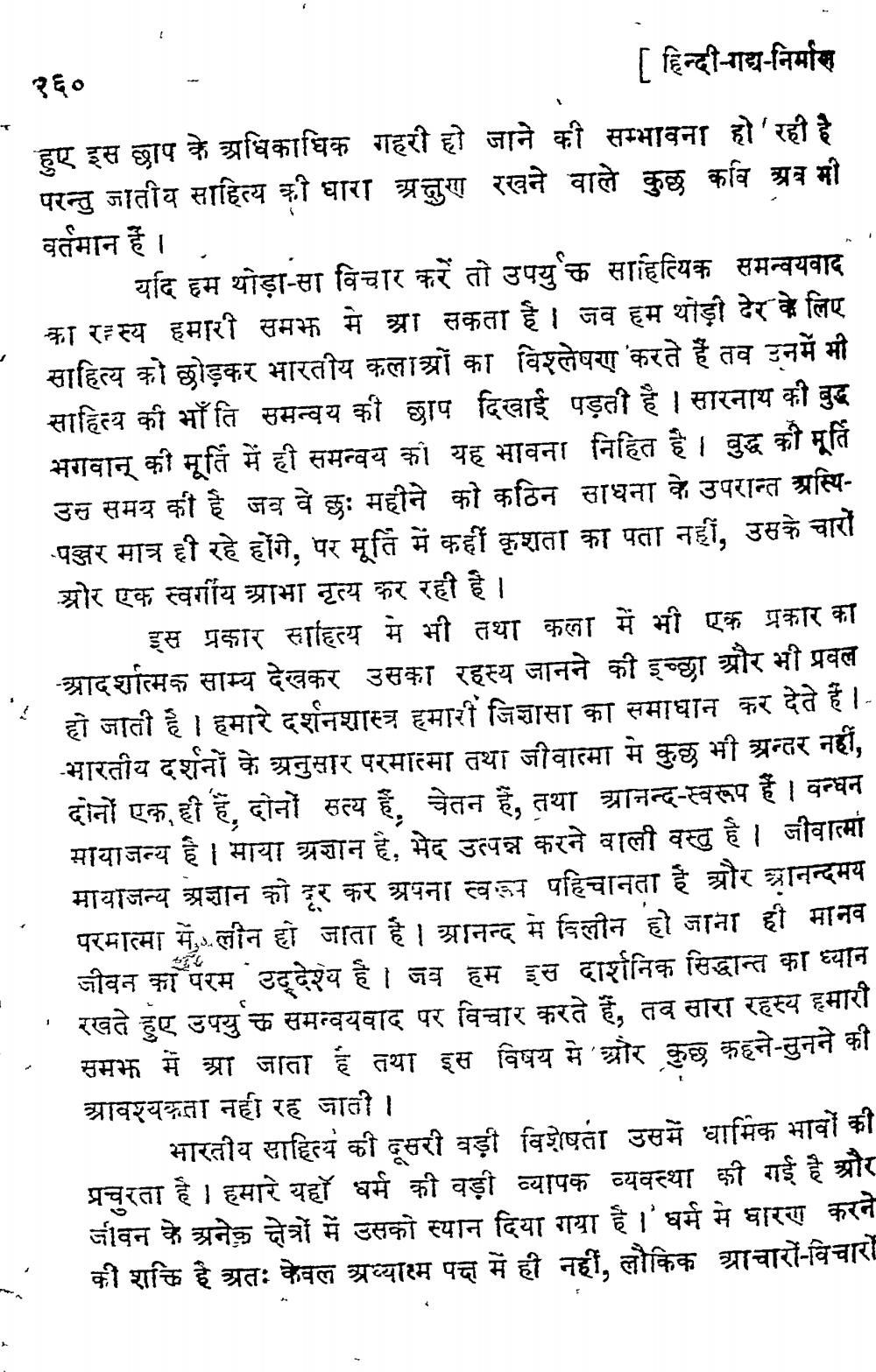________________
२६०
[हिन्दी-गद्य-निर्मास हुए इस छाप के अधिकाधिक गहरी हो जाने की सम्भावना हो रही है परन्तु जातीय साहित्य की धारा अक्षुण रखने वाले कुछ कवि अब मी वर्तमान हैं। .
यदि हम थोड़ा-सा विचार करें तो उपर्युक्त साहित्यिक समन्वयवाद का रहस्य हमारी समझ में आ सकता है। जब हम थोड़ी देर के लिए साहित्य को छोड़कर भारतीय कलाओं का विश्लेषण करते हैं तव उनमें भी साहित्य की भाँति समन्वय की छाप दिखाई पड़ती है । सारनाथ की बुद्ध भगवान् की मूर्ति में ही समन्वय की यह भावना निहित है । बुद्ध की मूर्ति उस समय की है जब वे छः महीने को कठिन साधना के उपरान्त अस्थिपञ्जर मात्र ही रहे होंगे, पर मूर्ति में कहीं कृशता का पता नहीं, उसके चारों ओर एक स्वर्गीय आभा नृत्य कर रही है।
इस प्रकार साहित्य में भी तथा कला में भी एक प्रकार का आदर्शात्मक साम्य देखकर उसका रहस्य जानने की इच्छा और भी प्रबल हो जाती है। हमारे दर्शनशास्त्र हमारी जिज्ञासा का समाधान कर देते हैं । - -भारतीय दर्शनों के अनुसार परमात्मा तथा जीवात्मा मे कुछ भी अन्तर नहीं, दोनों एक ही हैं, दोनों सत्य हैं, चेतन है, तथा आनन्द-स्वरूप हैं । वन्धन मायाजन्य है । माया अज्ञान है, भेद उत्पन्न करने वाली वस्तु है । जीवात्मा मायाजन्य अज्ञान को दूर कर अपना त्वा पहिचानता है और अानन्दमय परमात्मा में लीन हो जाता है । अानन्द में विलीन हो जाना ही मानव जीवन का परम उद्देश्य है । जब हम इस दार्शनिक सिद्धान्त का ध्यान रखते हुए उपयुक्त समन्वयवाद पर विचार करते हैं, तब सारा रहस्य हमारी समझ में आ जाता है तथा इस विषय मे और कुछ कहने-सुनने को आवश्यकता नहीं रह जाती।
___ भारतीय साहित्य की दूसरी बड़ी विशेषता उसमें धार्मिक भावों की प्रचुरता है । हमारे यहाँ धर्म की बड़ी व्यापक व्यवस्था की गई है और जीवन के अनेक क्षेत्रों में उसको स्यान दिया गया है। धर्म मे धारण करने की शक्ति है अतः केवल अध्यात्म पक्ष में ही नहीं, लौकिक प्राचारों-विचारों