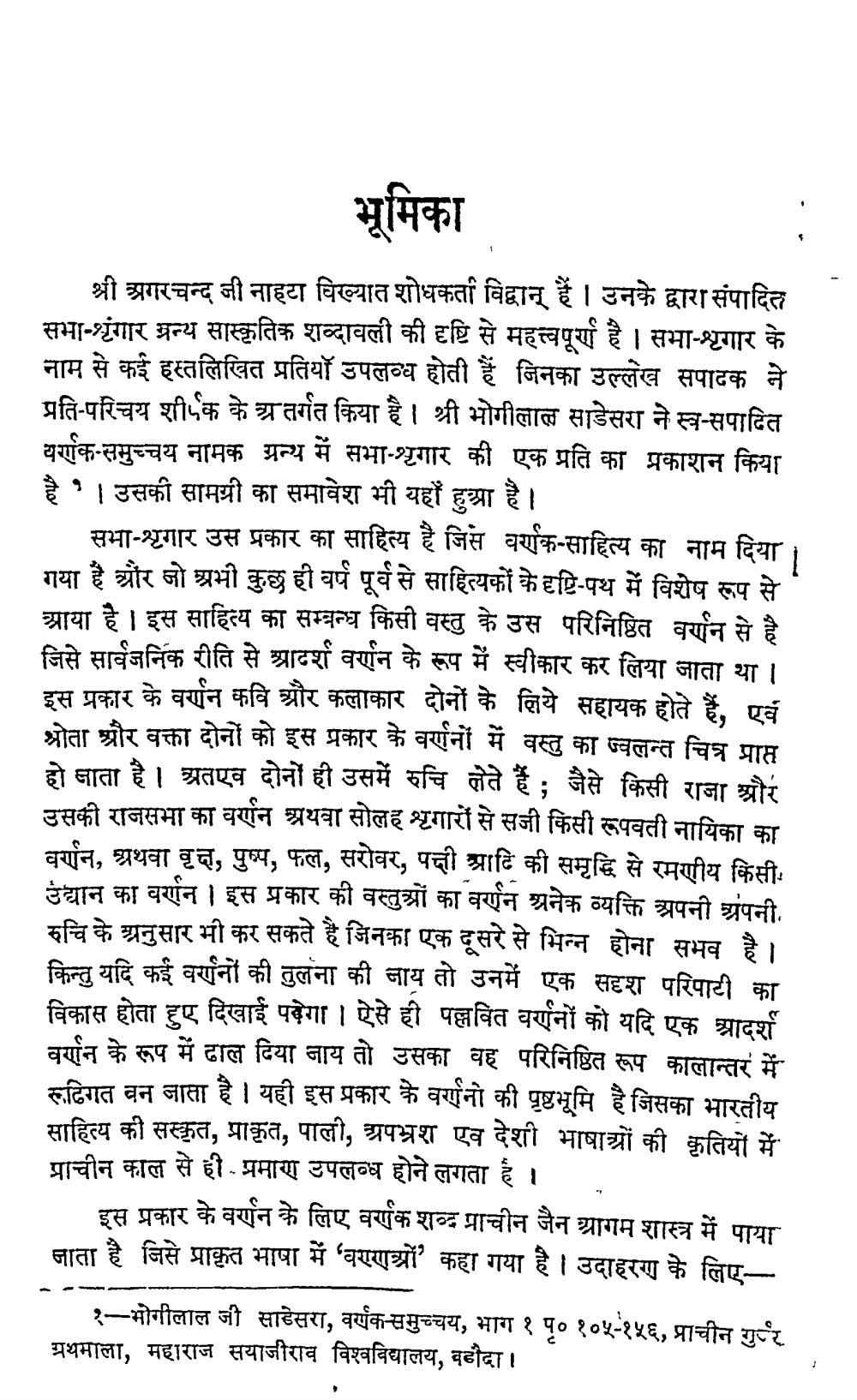________________
भूमिका
श्री अगरचन्द जी नाहटा विख्यात शोधकर्ता विद्वान् हैं । उनके द्वारा संपादित सभा-शृंगार ग्रन्थ सास्कृतिक शब्दावली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। सभा शृंगार के नाम से कई हस्तलिखित प्रतियाँ उपलब्ध होती हैं जिनका उल्लेख सपादक ने प्रति-परिचय शीर्षक के तर्गत किया है। श्री भोगीलाल साडेसरा ने स्व-सपादित थर्णक-समुच्चय नामक ग्रन्थ में सभा-शृगार की एक प्रति का प्रकाशन किया है ' । उसकी सामग्री का समावेश भी यहाँ हुआ है ।
।
सभा-शृंगार उस प्रकार का साहित्य है जिसे वर्णक - साहित्य का नाम दिया गया है और जो अभी कुछ ही वर्ष पूर्व से साहित्यकों के दृष्टि पथ में विशेष रूप से आया है । इस साहित्य का सम्बन्ध किसी वस्तु के उस परिनिष्ठित वर्णन से है जिसे सार्वजनिक रीति से आदर्श वर्णन के रूप में स्वीकार कर लिया जाता था । इस प्रकार के वर्णन कवि और कलाकार दोनों के लिये सहायक होते हैं, एवं श्रोता और वक्ता दोनों को इस प्रकार के वर्णनों में वस्तु का ज्वलन्त चित्र प्राप्त हो जाता है । अतएव दोनों ही उसमें रुचि लेते हैं; जैसे किसी राजा और उसकी राजसभा का वर्णन अथवा सोलह शृंगारों से सजी किसी रूपवती नायिका का वर्णन, अथवा वृक्ष, पुष्प, फल, सरोवर, पक्षी श्रादि की समृद्धि से रमणीय किसी उद्यान का वर्णन | इस प्रकार की वस्तुओं का वर्णन अनेक व्यक्ति अपनी श्रंपनी. रुचि के अनुसार भी कर सकते है जिनका एक दूसरे से भिन्न होना सभव है । किन्तु यदि कई वर्णनों की तुलना की नाय तो उनमें एक सदृश परिपाटी का विकास होता हुए दिखाई पड़ेगा । ऐसे ही पल्लवित वर्णनों को यदि एक आदर्श वर्णन के रूप में ढाल दिया जाय तो उसका वह परिनिष्ठित रूप कालान्तर में रूढिगत बन जाता है | यही इस प्रकार के वर्णनो की पृष्ठभूमि है जिसका भारतीय साहित्य की संस्कृत, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश एव देशी भाषात्रों की कृतियों में प्राचीन काल से ही प्रमाण उपलब्ध होने लगता है ।
इस प्रकार के वर्णन के लिए वर्णक शब्द प्राचीन जैन श्रागम शास्त्र में पाया जाता है जिसे प्राकृत भाषा में 'वरात्र' कहा गया है । उदाहरण के लिए
1
१ – भोगीलाल जी साडेसरा, वर्णक समुच्चय, भाग १ पृ० १०५ - १५६, प्राचीन गुर ग्रंथमाला, महाराज सयाजीराव विश्वविद्यालय, बडौदा ।